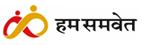भारत चीन संबंधों के पेच (भाग-4) : तनावपूर्ण अतीत और अनिश्चित भविष्य
India China relationship: संबंधों की जटिलताएं नज़ाकत के साथ नियंत्रित रखने की चुनौती

अगर देश में चीन संबंधी चर्चा नेहरू विरोध के भाव से मुक्त होकर वस्तुगत ढंग से चली होती, तो शायद आज चीन के बारे में हमारी समझ कहीं बेहतर होती। तब हम चीन के प्रति कहीं बेहतर रणनीति बनाने की स्थिति में होते। तब वैसी दुविधाओं का शिकार नहीं होते जैसा आज हम हैं। तब हम चीन के विकास से मोहित होते तो उस विकास की बुनियाद और उसके पीछे की प्रेरणाओं को भी बेहतर समझ सकते। और तब हम चीन की महत्त्वाकांक्षाओं और उसके कथित विस्तारवादी रुख को भी बेहतर ढंग से विश्लेषित कर सकते थे।
आज भी हम ऐसी शुरुआत बिना उन दुविधाओं को समझे नहीं कर सकते जिनकी जड़ें 1950- 60 के दशकों में चली चर्चाओं में छिपी हैं। इनमें एक बड़ी दुविधा तिब्बत को लेकर है। ये दुविधा कैसी रही, इसकी एक झलक राम मनोहर लोहिया की सोच में पा सकते हैं। मसलन, डॉ. लोहिया की यह टिप्पणी पर गौर करें- “अपनी निजी पसंद या नापंसद से अलग लामा-व्यवस्था की धार्मिक सत्ता को मैं स्वीकार करता हूं। कुछ लोग यह चाह सकते हैं कि सभी संगठित धर्मों की तरह लामा व्यवस्था भी खत्म हो जाए। (लेकिन) इस बारे में फैसला तिब्बती लोगों को करना है। तिब्बत में लामाओं के पास बड़ी मात्रा में जमीन और राजनीतिक सत्ता भी थी। (इसलिए यहां) तिब्बत से सहानुभूति का मतलब अनिवार्य रूप से दलाई लामा के प्रति सहानुभूति नहीं है और दलाई लामा से सहानुभूति का मतलब हर उस बात को स्वीकार कर लेना नहीं है, जिसे वो कहते हैं। (लेकिन) इसमें कोई संदेह नहीं है कि दलाई लामा आज स्वतंत्रता के लिए तिब्बत के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसके जीवट का प्रतीक बन गए हैं।” (इंडिया-चाइना एंड नॉदर्न फ्रंटियर्स, पेज 145)। डॉ. लोहिया ने इस क्रम में कहा था- “यह बात अवश्य साफ-साफ समझ ली जानी चाहिए कि एक सकारात्मक विदेश नीति सिर्फ तभी बन सकती है, जब हमारे दोस्त और पड़ोसी मजबूत हों। यह बिल्कुल साफ है कि लामाओं की राजनीतिक सत्ता और आर्थिक विशेषाधिकारों के तले गल रहे 40 लाख तिब्बती कभी एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकते।”
तो लामाओं के बारे में डॉ. लोहिया की यह समझ थी। मगर क्या यही समझ उनके राजनीतिक वारिसों में भी नजर आई? गुजरते वक्त के साथ तिब्बत की मजबूती की शर्त उनके विमर्श से गायब हो गई और उनकी शब्दावली में दलाई लामा “परम पावन” हो गए। धीरे-धीरे तिब्बत का सामाजिक संदर्भ गायब होता गया और इसका भू-राजनीतिक पहलू इस राजनीतिक धारा की सोच पर हावी होता चला गया। यह फर्क करना मुश्किल होता चला गया कि तिब्बत और चीन के सवालों पर दक्षिणपंथी ताकतों से इस खेमे की राय किस रूप में अलग है? नेहरू के प्रति साझा द्रोह का परदा उनकी वैचारिक भिन्नताओं को निरंतर ढंकता रहा। यह आजाद भारत के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है।
बहरहाल इस क्रम में स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा अपनाई गई चीन नीति को समझना जरूरी हो जाता है। प्रकारांतर में यह नेहरू की चीन नीति ही है। जवाहर लाल नेहरू पर आरोप है कि उन्होंने अपने वैचारिक आग्रहों की वजह से कम्युनिस्ट चीन को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिष्ठा दिलाई और तिब्बत में उसके दखल को नजरअंदाज करते रहे। उपलब्ध जानकारियों से जाहिर होता है कि यह आरोप 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध में एक मुहिम की शक्ल लेने लगा था। परिणाम यह हुआ कि गुजरते वक्त के साथ और भड़कते राजनीतिक माहौल के बीच पंडित नेहरू इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा अपनाने को मजबूर होने लगे। 1959 में नेहरू सरकार ने न सिर्फ दलाई लामा को भारत आने औऱ यहां से निर्वासित सरकार चलाने की इजाजत दी, बल्कि खुद पंडित नेहरू ने भी दलाई लामा से भेंटकर उन्हें एक तरह की वैधता प्रदान की। इन सारे घटनाक्रमों की भारत-चीन संबंधों की दिशा तय करने में बेहद अहम भूमिका रही। बिगड़ते भारत चीन संबंधों की अंतिम परिणति 1962 के युद्ध के रूप में हुई।
यह बात ध्यान में रखने की है कि वह दौर ढहते उपनिवेशवाद और नई बनी अस्थिर परिस्थितियों का था। उपनिवेशवाद के बाद के दौर का भूगोल इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। चीन में कम्युनिस्ट क्रांति की सफलता के साथ उस देश का नया चेहरा और नई भूमिका दुनिया के सामने आई थी। उसमें निसंदेह आक्रामकता और असहिष्णुता थी। चीनी कम्युनिस्ट नेता भले अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पंचशील की बात करते थे लेकिन व्यवहार में उन पर साम्यवाद को पूरी दुनिया में फैलाने का जुनून छाया हुआ था। यह बहुत मुमकिन है कि उनकी शब्दावली में दोस्त और दुश्मन के बीच कुछ और न होता हो। ऐसे में जब ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ से बात बिगड़ी, तो फिर उसका युद्ध तक पहुंच जाना शायद उसकी स्वाभाविक परिणति थी। चीन आज भी उस मानसिकता या राजनीतिक संस्कृति से पूरी तरह उबर गया है, यह नहीं कहा जा सकता।
मगर बीते दशकों में कुछ मौकों पर भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान ने चीनी सत्ता तंत्र के चरित्र की कहीं बेहतर समझ दिखाई- यह जरूर कहा जा सकता है। मसलन, यूपीए के शासनकाल में तत्कालीन विदेश सचिव निरुपमा राव ने एक महत्त्वपूर्ण भाषण में दोनों देशों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा की स्थितियों का वर्णन करते हुए यह याद दिलाया था कि यह रिश्ता जटिलताओं से भरा हुआ है। जटिलताएं किन्हीं दो देशों के संबंधों में होती हैं। लेकिन अगर वे देश पड़ोसी हों और उनके बीच सीमा जैसा विवाद हो, तो वे कुछ ज्यादा गंभीर रूप ले लेती हैं। और अगर उन दोनों देशों की सरकारें अलग-अलग विचारधाराओं और विश्व-दृष्टि के साथ चल रही हों, तो जटिलताएं गंभीरता के साथ-साथ नाजुक रूप भी लिए रहती हैं। भारत और चीन के संबंधों को इसी गंभीरता और नजाकत के साथ समझा जा सकता है। मगर राजनीतिक पार्टियों और विचारधाराओं के सामने चुनौती अपना चुनावी समर्थन आधार बढ़ाने की होती भी है और अक्सर उन्हें लगता है कि ऐसी समझदारी की बजाय भावनाएं भड़काकर बेहतर लाभ लिया जा सकता है।
वरना, इस सवाल का और क्या जवाब हो सकता है कि 1950-60 के दशक में चीन एवं तिब्बत के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री नेहरू के ऊपर अपनी लच्छेदार भाषणशैली में हमला बोलते हुए अपनी राजनीतिक पहचान बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में जब बतौर प्रधानमंत्री चीन गए, तो पहली बार भारत की तरफ से तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग घोषित कर आए? उस समय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो डॉ. लोहिया के सबसे तेज-तर्राज शिष्यों में एक गिने जाते थे। नरेंद्र मोदी ने जब यूपीए के खिलाफ अपना अभियान छेड़ा तो उस पर चीन के सामने समर्पण भाव में रहने का आरोप लगाया। मगर जब प्रधानमंत्री बने तो शी जिन पिंग के साथ अहमदाबाद में झूला झूलने और फिर वुहान और मल्लपुरम भावना की बातें कहने में उन्हें कोई अंतर्विरोध नजर नहीं आया। और आज जबकि चीन (मीडिया खबरों के मुताबिक) हमारे इलाके में तीन किलोमीटर घुस आया है, तब उनकी सरकार वैसी लाल आखें उसे नहीं दिखा रही है, जैसा वो मनमोहन सिंह सरकार से अपेक्षा करते थे।
बहरहाल, हमारे लिए विचारणीय यह है कि आज हम इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं। भारत की आजादी और चीन की क्रांति सत्तर साल पुरानी बातें हो चुकी हैं। तब की भौगोलिक और सियासी अस्थिरता से आज ये दोनों देश काफी हद तक उबर चुके हैं। आज उनकी सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हैं। चीन अपनी 13 खबर डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत भी आर्थिक विकास दर के मामले में आज कहीं बेहतर स्थिति में है और पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है। खुद इन दोनों देशों के बीच सालाना आपसी कारोबार 95 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि अब बेहतर रिश्तों के लिए दोनों ही देशों के भीतर एक ठोस आधार तैयार है।
इसके बावजूद कभी तिब्बत तो कभी कश्मीर का पेच फंस जाता है और रिश्तों में सुधार की जारी प्रक्रिया पटरी से उतरती दिखने लगती है। फिलहाल माहौल पटरी से उतरने वाला ही है। अतीत में चीन से आने वाले बयान और विचार यह जाहिर करते हैं कि चीन के लिए भारत की मजबूती को स्वीकार करना आसान नहीं रहा है। उधर भारत ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका के साथ धुरी बनाने की जो दिशा तय की है, उससे भी चीन भड़का नजर आता है। अमेरिका के साथ चीन के बिगड़ते रिश्तों का साया भी भारत- चीन संबंधों पर पड़ रहा है। भारत में मौजूद अमेरिका समर्थक लॉबी की भारत- चीन तनाव को बढ़ाने में अक्सर ही भूमिका देखी जाती है। मेनस्ट्रीम मीडिया ऐसे तमाम प्रयासों का वाहक बनता है। इससे चीन की मंशाओं और उसकी रणनीति के बारे में देश में सही समझ नहीं विकसित हो पाती। बहरहाल, वुहान और मल्लपुरम में जो भावनाएं व्यक्त हुईं, वो क्यों जमीन पर नहीं उतरी हैं, यह सवाल अवश्य हमारे सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से देश अपेक्षा करता है कि वो इस बारे में अधिक स्पष्टता और भरोसा भारतीय जनता में पैदा करें। तभी आज के माहौल में भारत- चीन संबंधों को लेकर कोई सार्थक चर्चा आगे बढ़ पाएगी।