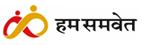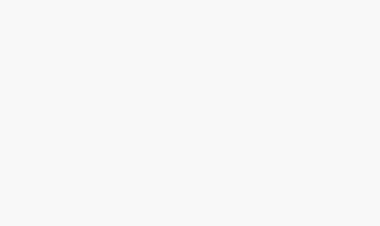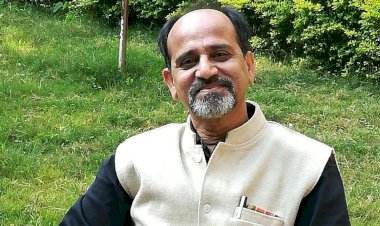संसाधनों के नियंत्रण को लेकर आदिवासियों और सरकार के बीच द्वंद्व
आदिवासी इलाके खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। भारत के बड़े व्यापारिक घरानों की नज़र इन पर है। ग्राम सभाओं की असहमति, आदिवासियों के असहयोग और प्रतिरोध के लिए लड़ने वाले कई प्रगतिशील संगठन इस लूट के खिलाफ खड़े हैं, जबकि सरकार कॉरपोरेट हितों की रक्षा के लिए आगे आती है और प्रशासनिक रूप से इन विरोधों को दबाती है।

देश के 15 प्रतिशत भूखंड में आदिवासी समूह रहते हैं। वन, खदान, बांध आदि परियोजनाओं ने आदिवासियों के जीवन व जीविका को काफी प्रभावित किया है। 58 आदिवासी बहुल जिलों में 67 प्रतिशत से अधिक जंगल है। इन्हीं इलाकों के बङे भाग के जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान रुप में बांट दिया गया है। इस कारण से यहां के रहने वाले आदिवासियों को जंगल का घुसपैठिया मान लिया गया है। देश का अधिकांश खनिज पदार्थ आदिवासी इलाके में ही है। इन्हीं खनिज पदार्थों को लेने के लिए बङे पैमाने पर जंगल की जमीन का हस्तांतरण किया गया है, जिससे भारी मात्रा में पर्यावरण प्रभावित हुआ है।
साथ ही जंगल का नाश होना, आदिवासी समुदायों का आजिविका खत्म होना, विस्थापन होना और इस कारण आदिवासी क्षेत्रों में अशांति फैलना शुरु हो गया। बङे - बङे बांधों का निर्माण आज विस्थापन का सबसे बड़ा कारण है। आज आदिवासियों का विभिन्न विकास परियोजनाओं से भयंकर विस्थापन हो रहा है, अभी तक देश में लगभग 3 करोड़ आदिवासी विस्थापित हुए हैं। जब से इन कम्पनियों को पता चला है कि सारे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार जंगल में है, भारी मात्रा में पैसा है, तब से जंगल को अपने कब्जे में लेने का मुहिम चालू है। आदिवासी समुदाय अपने जीवन यापन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। जब सरकारें इन संसाधनों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं, तो समुदाय अपने अधिकारों और आजीविका के लिए संघर्ष करने को मजबूर हो जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में कोयला खनन के लिए हसदेव अरण्य और रायगढ़ के जंगलों को काटा जा रहा है। इसके विरोध में स्थानीय समुदायों के साथ देश भर के लोग जुङ गए हैं। नर्मदा घाटी के इलाकों में प्रस्तावित मोरांड - गंजाल और बसनिया (ओढारी) बांध में लगभग 5 हजार हेक्टेयर घना जंगल और वन भूमि डूब में आने को लेकर आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है। पिछले जून माह में जन स्वाभिमान यात्रा के दौरान पता चला कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर और बिरसा विकास खण्ड के 55 वन खण्डों को रिजर्व फारेस्ट घोषित करने में 40 गांव प्रभावित होकर 36833.672 हेक्टेयर वन भूमि को रिजर्व फारेस्ट घोषित किया जा रहा है।
वहीं बालाघाट के परसवाड़ा विकास खंड के लौगुर जंगल क्षेत्र में 250 हेक्टेयर वन भूमि खनिज के लिए आबंटित किया गया जा रहा है। पिछले माह भरी बारिश में मध्य प्रदेश के जिला देवास, खातेगांव, खिवनी और डिंडोरी करंजिया विकास खंड के जारासुरंग में मकान तोड़ कर वन भूमि से बेदखली का मामला ने तुल पकड़ लिया है। आदिवासी संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सिवनी को बल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य के लिए खाली कराया जा रहा था।इस अभ्यारण्य के लिए कार्य कर रहे वन मंडलाधिकारी सिहोर का स्थानांतरण कर दिया गया है और अभ्यारण्य के कार्य को रोकने का आदेश सरकार को जारी करना पड़ा है।
दूसरी ओर एक नया मामला सामने आया है कि मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक द्वारा कटनी जिले के अपने चार आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर डिंडोरी जिले में बैगा आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी कर वर्ष 2009 से अभी तक लगभग 795 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। विधायक द्वारा आदिवासियों की इन जमीनों पर बाॅक्साइट खदान स्वीकृत कराकर खनन करने की तैयारी है। इन चारों आदिवासी व्यक्तियों के नाम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में हैं। इस धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाने आदिवासी संगठित हो गए हैं। देश के आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह के कई संघर्ष चल रहे हैं और सरकार द्वारा आंदोलनों पर दमन किया जा रहा है।
आदिवासी इलाके खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। भारत के बड़े व्यापारिक घरानों की नज़र इन पर है। ग्राम सभाओं की असहमति, आदिवासियों के असहयोग और प्रतिरोध के लिए लड़ने वाले कई प्रगतिशील संगठन इस लूट के खिलाफ खड़े हैं, जबकि सरकार कॉरपोरेट हितों की रक्षा के लिए आगे आती है और प्रशासनिक रूप से इन विरोधों को दबाती है। आदिवासियों और अन्य समूहों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित करने और उन्हें विस्थापित करने के लिए वह हर संभव ताकत का इस्तेमाल करती है। संविधान के अनुच्छेद 244 में पांचवीं अनुसूची में यह व्यवस्था है कि किसी भी कानून को पांचवीं वाले क्षेत्र में लागू करने के पूर्व राज्यपाल उसे जनजातीय सलाहकार परिषद को भेजकर अनुसूचित जनजातियों पर उसके दुष्प्रभाव का आकलन करवाएंगे और तदनुसार कानून में फेरबदल के बाद पांचवीं अनुसूची में लागू किया जाएगा।
इसमें प्रावधान किया गया है कि आदिवासियों से किसी प्रकार के जमीन हस्तांतरण का नियंत्रण करना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस संवैधानिक व्यवस्था की अनदेखी हो रही है। जबकि पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में प्रशासन स्थानीय समुदाय की सहमति से संचालित होना चाहिए। आदिवासी इलाकों के लिए पेसा कानून में दो महत्वपूर्ण विषय है। पहला गांव सीमा के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्राम सभा करेगा। दूसरा रूढ़िगत और परम्परागत तरीके से विवाद निपटाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। परन्तु सत्ताधीशों ने संविधान की मूल चेतना को समझा तक नहीं और यही कारण है कि छठी अनुसूची के आदिवासी इलाकों को छोड़कर देश के सभी आदिवासी इलाकों पर ऐसे कानून लाद दिए गए हैं जो उनकी परम्परा की अनदेखी ही नहीं करते हैं बल्कि उसके विपरीत भी हैं।
भारत में सत्ता और प्रशासन के जबरदस्त केंद्रीकृत ढांचे से भी मामला उलझता जाता है। केंद्र सबसे शक्तिशाली है और उसके बाद राज्यों की राजधानियों में सत्ता के केन्द्र हैं। इसके नीचे ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं या नगर निगमों को सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण नहीं हुआ है, उन्हें केवल उपर से पैसा मिलता है और उसमें भ्रष्टाचार करने का अधिकार मिलता है। जब इन इलाक़ों के लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो सत्ता के केंद्र दूर होने और सत्ता में उनकी विशेष भागीदारी नहीं होने से इस आवाज को अनसुना कर दिया जाता है या दबाने की कोशिश होती है।
वास्तव में, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग स्थिरता के सभी तीन आयामों से संबंधित है। सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और आर्थिक विकास। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग इन आयामों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। सामाजिक लाभों को अधिकतम करते हुए और पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करते हुए संसाधनों का दीर्घकालिक उपयोग बनाए रखना।
(लेखक राज कुमार सिन्हा बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ से जुड़े हुए हैं)