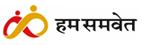अर्थव्यवस्था नहीं व्यवस्था की बात कीजिए
हमें यह समझना होगा कि वास्तविकता यह है कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं व्यवस्था खतरे में है। जीएसटी ने भारत के संघीय ढांचे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। सभी राज्य याचक की भूमिका में आ चुके हैं। इसलिए उन्हें नए सिरे से अपने शासन-प्रशासन के बारे में सोचना व समझना होगा। उन्हें केन्द्र की अधिनायकवादी प्रवृत्ति का सामना लोकतांत्रिक व नैतिक मूल्यों से करना होगा। क्या इसके लिए उनकी मानसिक तैयारी है?
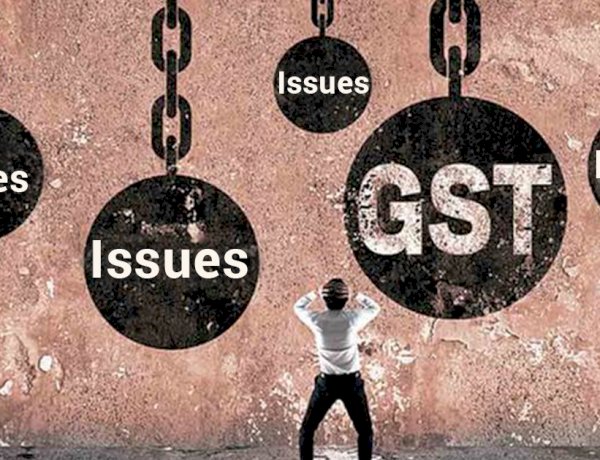
पिछले कुछ दिनों से भारत में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को लेकर आपाधापी मची हुई है। ऐसा कहा गया है कि इसमें करीब 24 प्रतिशत की गिरावट आई है। गौरतलब है, यह आंकड़े संगठित क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर सामने आए हैं। यदि इसमें असंगठित क्षेत्र में आई गिरावट को शामिल किया जाता तो यह आंकड़ा 40 से 60 प्रतिशत के बीच कहीं ठहरता। उधर, कोरोना के बढ़ते मामले हमें (यदि सबकुछ ऐसे ही चलता रहा तो) अगले दो महीनों में इसमें भी विश्व का सिरमौर बन सकते हैं। वैसे अर्थव्यवस्था की गिरावट में तो हम सिरमौर बन ही चुके हैं। अब कोरोना में भी?
सोचिए चीन जहां से यह संक्रमण फैला है, वहां अभी तक कुल 90000 लोग संक्रमित हुए हैं और हमारे यहां 6 सितंबर के आंकड़े बता रहे हैं, इतने ही (करीब 90000) एक ही दिन में भारत में संक्रमित हो चुके हैं। इसके बावजूद चारों ओर एक समझा बूझा सन्नाटा पसरा हुआ है। उपरोक्त दोनों ही मसलों पर हमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, वित्तमंत्री, वाणिज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उद्योग मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या अन्य किसी जवाबदेह व्यक्ति या संस्था की ओर से कोई टिप्पणी या स्पष्टीकरण सुनाई, दिखाई या लिखित में सामने आता नहीं दिखा। यह भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का "न्यू नार्मल" है या "न्यू लो"? यूं भी सत्तासीन अपनी व्यवस्था कर ही लेते हैं। इसीलिए इस बार संसद के अधिवेशन में प्रश्नकाल नहीं होगा। राहुल गांधी चूंकि असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए उनके सामने मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या का मामला खड़ा कर दिया है।
अत:एव हमें यह समझना होगा कि वास्तविकता यह है कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं व्यवस्था खतरे में है। चूंकि अर्थव्यवस्था व्यापक व्यवस्था का एक अंश मात्र है, इसलिए उसे इतना बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित व प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे उसके ठीक हो जाने से सब ठीक-ठाक हो जाएगा। अब यह तय सा हुआ लग रहा है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था संकट में या वेंटीलेटर पर नहीं है, बल्कि इसका प्राणान्त हो चुका है, यह मर चुकी है, यह निर्जीव हो चली है और इसे कोई एक या दो व्यक्ति संभाल नहीं सकते। हसन कमाल लिखते हैं,-
सबकी बिगड़ी को बनाने निकले। यार हम तुम भी दीवाने निकले।।
इसे लिखे जाने का संदर्भ शायद कुछ और रहा होगा। आज हम सबको इस मृत अर्थव्यवस्था को गले उतारने के लिए "टीना" (TINA) फेक्टर यानी :कोई विकल्प नहीं" (There is no alternative) का सहारा लिया जा रहा है। इसलिए "विकास" को आधार बताया जाता है। पर यह नहीं बताया जाता कि विकास का आधार क्या होगा? याद रखिए भारत में आधुनिक (नया) आर्थिक इतिहास सन् 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल सम्राट से बंगाल सूबे की दीवानी व भू-राजस्व संग्रह का अधिकार पाने से शुरु होता है। इसके बाद इसमें तमाम परिवर्तन लाये गए। हर 20-25 वर्षों में आर्थिकी का नया दौर प्रारंभ हुआ और यह रिवाज आज तक बदस्तूर चल रहा है। सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं "हम सभी इतिहास से बंधे हैं, पर इतिहास पढ़ने को बाध्य नहीं हैं। फिर भी जो लोग बाध्य होकर या बिना बाध्य हुए इतिहास पढते हैं, उनके सामने यह सवाल उठता है कि इतिहास क्यों पढ़ा जाए, औपनिवेशिक भारत का इतिहास क्यों पढ़ा जाए?"
यह बेहद विचारणीय कथन है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रवीन्द्रनाथ टेगौर कहते हैं "हम पेट की रोटी के बदले, सुशासन, सुविचार और सुशिक्षा, सबकुछ एक बड़ी दुकान से खरीद रहे हैं, बाकी बाजार बंद है। जो लोग भाग्यशाली हैं वे सदा स्वदेश को देश के इतिहास में ही खोजते और पाते हैं। हमारे मामले में इसका उलटा है। देश के इतिहास ने ही हमारे स्वदेश को ढंक रखा है" उनके कथन को एक शताब्दी से भी ज्यादा हो गया, लेकिन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन आया हो ऐसा स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। समाज का बड़ा वर्ग आज भी पेट की रोटी की व्यवस्था को लेकर हैरान-परेशान है। आत्महत्या कर रहा है। पर टीना फेक्टर अपना काम बखूबी कर रहा है।
इसी बात को रवीन्द्र बाबू के निबंध "व्यक्ति और प्रतिकार" सन् 1314 बंगाब्द (सन् 1910 ईस्वी) से भी समझते हैं। वे लिखते हैं, "आज हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे शहरी लोग जब गांव के निरक्षर मनुष्य के पास जाकर कहते हैं कि हम दोनों भाई-भाई हैं, तब वह बेचारा ग्रामीण इस "भाई" शब्द का अर्थ समझ नहीं पाता। जिन लोगों को हम "हलजोत्ता" कहकर पुकारते हैं, जिनके सुख-दु:ख का मूल्य हमारे सामने अत्यंत सामान्य है, जिनकी हालत जानने के लिए हमें गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित तथ्यों की तालिका पढ़नी होती है, उन्हें अचानक भाई-भाई के संबंध का परिचय देकर महंगे दामों पर चीजें अर्थात स्वदेशी सामान (टिप्पणी आज माल्स आदि) खरीदने अथवा गोरखे-चौकीदार के जूते खाने के लिए उनको बुलाने पर हमारे इरादों के प्रति उनके संदेह उठने की बात तो है ही।"
क्या एक शताब्दी से अधिक बीत जाने पर भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नजर आता है? हसन कमाल आगे कहते हैं:- कोई तो चीज नई मिल जाती, दर्द भी सदियों पुराने निकले।
रवींद्र बाबू के उपरोक्त कथन के करीब पांच वर्षों बाद (सन् 1915 ईस्वी) परिवर्तन की बात सामने आती है। इस परिवर्तन के पुरोधा यानी महात्मा गांधी ने उस समय अपने तरीके से "टीना फेक्टर" यानी कोई विकल्प नहीं को सिरे से नकार दिया था। जब तकरीबन सारा विश्व नए तरह से पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच उलझ रहा था और दोनों के प्रवर्तक स्वयं को एकमात्र समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, तब गांधी ने एक नए विचार या व्यवस्था को हमारे सामने रखा। यह विचार पारंपरिक अर्थव्यवस्था की परिधि व सीमाओं का अतिक्रमण करता था। यह विचार मनुष्य को सर्वोपरी मानकर आगे बढ़ता था और यह स्थापित करता था कि अर्थव्यवस्था या व्यवस्था मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य इनके लिए बना हुआ है।
परन्तु हम इस नए अविष्कार से तारतम्य नहीं बैठा पाए और गांधी विचार को एक ठहर सी गई परिस्थिति के रूप में आत्मसात करने की भूल कर बैठे। यह सोचा ही नहीं कि तकनीक या वैज्ञानिक विकास किस तरह नई परिस्थिति में मनुष्य और मनुष्यता के अनुकूल बन सकता है या इसे अनुकूल बनाया जा सकता है।
सन् 1915 से सन् 1947 तक हम एक आत्मनिर्भर व सही पर आत्मसम्मान से भरे एक राष्ट्र के रूप में विकसित होते रहे और यह स्थापित करने में कुछ हद तक सफल भी हुए कि मनुष्य महज एक आर्थिक प्राणी नहीं है। बाकी की दुनिया से अलग एक विचार जो हमारे यहां पनप रहा था, अपनी हड़बड़ाहट में हम उससे दूर भाग खड़े हुए। इसका परिणाम क्या हुआ?
सव्यसायी भट्टाचार्य बताते हैं, "इस देश में सन् 1947 से और इस उपमहाद्वीप में स्थित अन्य देशों में अर्थनीतिक विकास अथवा किसी क्षेत्र में पुनरावृत्ति स्वाधीनता पूर्व के अर्थनीतिक स्वरूप और चलन द्वारा प्रभावित हुआ था। पिछले चार दशकों (अब तो सात दशक बीत चुके हैं) में जो समाज तथा अर्थनीति विकसित हुई है वह लगता है जैसे एक पांडुलिपि है, जिसे बार-बार लिखा गया हैं। नई लिखावट के पीछे जहां-तहां औपनिवेशिक काल की लिखावट पुरानी बातें लेकर उभर रही हैं।"
आज पूरे विश्व में गांधी अकेले हैं, जो विकल्पहीनता को पूरी तरह झुठला देते हैं। वर्तमान में इस मृत अर्थव्यवस्था और अर्थहीन अर्थनीति से भारत सरीखे बड़े राष्ट्र का गतिमान हो पाना सर्वथा असंभव है। परन्तु हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है यह है कि लोग वर्तमान अर्थव्यवस्था की आलोचना केवल इस आधार पर कर रहे हैं कि इसका ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया। यह बात सिरे से ही गलत है।
अत:एव आवश्यकता इस बात की है कि "टीना" फेक्टर को नकार कर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जिन राज्यों में सत्तारूढ़ हैं, वहां पर नए सिरे से सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकल्पों पर बात करें। वे अर्थव्यवस्था के मरने का शोक मनाना बंद करें और व्यवस्था को संपूर्णता में पटरी पर लाने की योजना बनायें। जीएसटी ने भारत के संघीय ढांचे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। सभी राज्य याचक की भूमिका में आ चुके हैं। इसलिए उन्हें नए सिरे से अपने शासन-प्रशासन के बारे में सोचना व समझना होगा। उन्हें केन्द्र की अधिनायकवादी प्रवृत्ति का सामना लोकतांत्रिक व नैतिक मूल्यों से करना होगा। क्या इसके लिए उनकी मानसिक तैयारी है? राज्यों को केन्द्र की सरकार की गलतियों, नाकामयाबियों, अदूरदर्शिता, अक्खड़पन व अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को सामने लाते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने भारतीय विकल्प प्रस्तुत करना होगा, जबकि अभी की स्थिति तो यह है:-
चांद को रात में मौत आई थी। लाश हम दिन में उठाने निकले।।