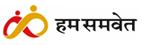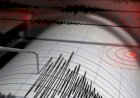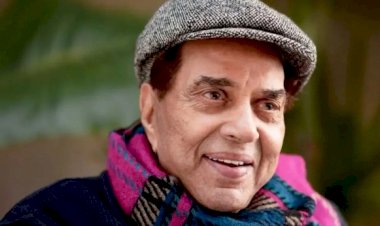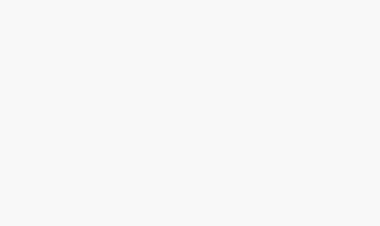खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं, फिर भी परिवार और समाज में उपेक्षित हैं महिलाएं
खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। क्योंकि वे न केवल भोजन का उत्पादन करती हैं, बल्कि भंडारण, प्रसंस्करण, पोषण और उपभोग के संतुलन में भी प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

समाज में आवाज उठाने से पहले या सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रतिरोध करने से पहले हर महिला का पहला संघर्ष घर से शुरू होता है। पिछले कुछ सालों से वंचित समुदाय के लोग चाहे वो महिला, दलित या आदिवासी हों वो अपने हको के लिए लङने के लिए बुलंदी से आगे आ रही हैं। इन संघर्षों का एक प्रमुख ताकत यह है कि इनके व्यक्तिगत लीडर नहीं हैं बल्कि सामुहिक नेतृत्व का मॉडल है, जिनमें महिलाएं बङी भूमिका निभा रही है। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के कृषि, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, और ग्रामीण विकास में योगदान को मान्यता देना और सम्मानित करना है।
इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1995 में बीजिंग महिला सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। औपचारिक रूप से 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 अक्टूबर को "अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस" घोषित किया गया। यह दिवस विश्व खाद्य दिवस (16 अक्टूबर) के एक दिन पहले मनाया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण महिलाओं की भूमिका खाद्य उत्पादन और सुरक्षा में कितनी अहम है। ग्रामीण महिलाएं विश्व की लगभग 43% कृषि श्रमशक्ति का हिस्सा हैं। वे खेतों में काम करने, पशुपालन, जल संग्रहण, बीज संरक्षण, और स्थानीय खाद्य प्रणालियों की रीढ़ हैं। उनके प्रयासों के बावजूद, उन्हें अक्सर भूमि के स्वामित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋण, और तकनीक तक समान पहुंच नहीं है।
भारत में यह दिवस महिला किसान, स्व-सहायता समूहों, ग्रामीण उद्यमियों और स्वयंसेवी संगठनों के योगदान को पहचानने का अवसर है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक संवैधानिक, विधिक, सामाजिक और आर्थिक प्रयास किए गए हैं। भारत का संविधान महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देता है, जैसे अनुच्छेद (14) कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15(1) और 15(3) लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, अनुच्छेद (16) सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देता है, अनुच्छेद 39(ए), 39(डी) समान कार्य के लिए समान वेतन और जीवन यापन के साधन और अनुच्छेद (42) मातृत्व अवकाश और कार्य की उचित परिस्थितियां सुनिश्चित करता है।
महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 , कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण) अधिनियम, 2013, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधित 2017) शामिल है। 73 वां और 74 वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों और नगर निकायों में एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए अनिवार्य किया गया गया है। कई राज्यों ने इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पारित हुआ है। इससे संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। क्योंकि वे न केवल भोजन का उत्पादन करती हैं, बल्कि भंडारण, प्रसंस्करण, पोषण और उपभोग के संतुलन में भी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वे बीज बोने, निराई-गुड़ाई, कटाई, मवेशी पालन, सब्जी उत्पादन और डेयरी कार्यों में सक्रिय रहती हैं।
अनेक ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक बीजों को संरक्षित रखती हैं जो स्थानीय खाद्य विविधता और जैविक खेती के लिए आवश्यक है। कई महिला किसान जैविक खेती, किचन गार्डन और सामुदायिक बीज बैंक चलाती हैं। यह खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देता है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफओए) का कहना है कि यदि महिलाओं को पुरुषों के समान संसाधन मिलें, तो उत्पादन 20–30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है और भूख से पीड़ित लोगों की संख्या घट सकती है।
यह ज्ञान भविष्य की खाद्य आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन के समय बहुत उपयोगी साबित होता है। विश्व में 'खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति' रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में कुपोषित लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है, और 19.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के वैश्विक आंकड़ों को देखें तो सालाना कुल खाद्य उत्पादन का 19 फीसदी बर्बाद हो रहा है, जो करीब 105.2 करोड़ टन के बराबर है। दूसरी ओर दुनिया में 78.3 करोड़ लोग खाली पेट सोने को मजबूर हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा की सभी योजनाओं, जिसमें ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ (पीडीएस) भी शामिल है, को स्थानीय उत्पादन, खरीदी, भंडारण, वितरण की सार्वभौमिक और विकेन्द्रीकृत प्रणालियों में बदला जाए।
भारत की कुल महिला आबादी का लगभग 70% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 8 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। जलाऊ लकड़ी एकत्र करने या जल लाने के झंझट से मुक्ति के कारण, महिलाएं (ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शामिल हुई हैं। जनधन खाताधारकों में 55% महिलाएं हैं, जिससे उन्हें बैंकिंग सुविधा और ऋण उपलब्ध हो रहे हैं। मार्च 2023 तक, स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 40,710 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है, जिसमें 80% महिला उद्यमियों को उद्यम दिया गया, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला है।
मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7.27 करोड़ है, जिसमें लगभग 5.25 करोड़ से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इनमें 2.54 महिलाएं और 2.71 करोड़ पुरुष शामिल हैं। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे करीब 62 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। अब तक 30 हजार 264 महिला समूहों और 12 हजार 685 महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत ब्याज दर से अनुदान के रूप में 648.67 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है।
लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने 1.27 करोड़ बहनों के खाते में 1551.86 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता पहुंच रही है। इस योजना के तहत 1.27 करोड़ महिलाओं को अब तक 35,329 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, 25 लाख महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 882 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके परिवारों में बचत को प्रोत्साहित कर रही है। आर्थिक विकास के बावजूद, पारंपरिक सामाजिक जातीय महिलाओं को वेतन वाले काम में भाग लेने से हतोत्साहित किया जाता है और उन्हें घरेलू तक ही सीमित रखा जाता है।
दूसरी ओर एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। दुष्कर्म के मामलों में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2023 में दहेज हत्या के 468 मामले दर्ज किए गए, जबकि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के प्रकरण हजारों की संख्या में सामने आए हैं। मध्यप्रदेश महिला अपराधों में शीर्ष राज्यों में शामिल है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023 के अनुसार, आर्थिक भागीदारी में भारत 146 देशों से 127 वें स्थान पर है, जो गंभीर रूप से असमानता और लैंगिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, 90% से अधिक श्रमिक महिला बेरोजगार हैं, जिसके अनुसार उनके लिए काम उपलब्ध नहीं हैं।नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ईयर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2020-2022 में आत्महत्या करने वाली आधी से ज्यादा महिलाएं गृहिणी थीं। सरकारी प्रयासों के बाबजूद अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और स्थायी रोजगार, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं।ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन अब भी यह शहरी क्षेत्रों से अधिक है। एनीमिया (रक्ताल्पता) और कुपोषण ग्रामीण महिलाओं में बड़ी समस्या है।स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, स्वच्छ जल और सैनिटेशन की कमी भी चिंता का विषय है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज और लिंग आधारित भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियां अब भी मौजूद है।
15 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय ग्रामिण महिला दिवस और 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस पर विशेष लेख।
(लेखक राज कुमार सिन्हा बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ से जुड़े हैं)