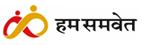हमेशा देर क्यों कर देता हूँ मैं
महात्मा गांधी अपने लिए एक बेहद मजेदार वाक्य का प्रयोग उन दिनों के लिए करते हैं जो उनकी वकालत का शुरुआती दौर था। यह शब्द है “संवैधानिक शर्मीलापन” (Constitutional Shyness)। क्या हमारा समाज जिसमें न्यायालय भी शामिल हैं इस संवैधानिक शर्मीलेपन का शिकार होते जा रहे हैं?

हमेशा देर कर देता हूँ मैं... हर काम करने में,
जरुरी बात कहनी हो या कोई वादा निभाना हो
उसे आवाज देनी हो उसे वापस बुलाना हो
हमेशा देर कर देता हूँ।
मुनीर नियाजी
सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः बुलडोज़र न्याय के खिलाफ दो हफ़्तों की रोक लगा ही दी। बुलडोज़र पिछले 6-7 वर्षों से भारत के भाजपा शासित अधिकांश राज्यों में सत्ता का नया प्रतीक और अभिनव एवं त्वरित न्याय प्रक्रिया का “आदरणीय और प्रिय प्रतीक” बनकर स्थापित सा हो गया है।
हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से लेकर पत्थर फेंकने जैसे साधारण अनदेखी कर देने वाले अपराधों का एक ही दंड बन गया था, “बुलडोज़र से घरों-दुकानों आदि को ढहा देना।” बड़ी बात यह है कि बुलडोज़र सामान्यतया “उन्हीं नागरिकों” के खिलाफ सक्रिय किया जा रहा है, जिन्हें अब दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की तरफदारी की जा रही है।
“हमेशा देर कर देता हूँ” यह न्यायपालिका पर लगा कोई आरोप नहीं बल्कि भारतीय न्यायप्रणाली को समझने का नया “सूत्र” नया “मंत्र” है। भारतीय प्रशासनिक तन्त्र बेहद चालाकी से न्याय की धारणा या नैरेटिव को बदलने में काफी हद तक सफल हो गया है। इसने सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मसलों पर केन्द्रित रहने के बजाय एक “जमानत” न्यायालय में बदल देने का सुनियोजित प्रयत्न किया है। इसकी सफलता और असफलता का आंकलन बेहद कठिन है। परंतु इस प्रक्रिया में इसने सहायक न्यायालयों (ट्रायलकोर्ट) और उच्च न्यायालयों को कमोवेश श्रीहीन सा साबित करने का जोखिम भी खड़ा कर दिया है।
यह जानना रुचिकर होगा कि जमानत के सबसे पहले प्रमाण ईसा पूर्व 399 में मिलते हैं जब सुकरात को स्वतंत्र कराने के लिये प्लेटो ने “बाँड” की व्यवस्था की थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहता है कि, मुकदमे से पहले हिरासत से बचना सर्वोत्तम है। परंतु हर दूसरी बात में चाणक्य का उदाहरण देने वाले तो ठीक परंतु चाणक्य कहलाने से गौरवान्वित होने वाले भी मुकदमे से पहले (प्री ट्रायल) हिरासत के सबसे बड़े पक्षधर नजर आते हैं और बरसों बरस तमाम लोगों की जमानत पर लगाम लगाए रहते हैं।
वैसे भारत में सबसे पहले “जमानत नियम है जेल अपवाद” की स्थापना सन 1978 में राजस्थान राज्य बनाम बालचंद उर्फ़ बलिये के मामले में न्यायमूर्ति वी.आर कृष्णाअय्यर ने की थी। आज 46 वर्षों बाद उनकी बात को बार-बार दोहराया जा रहा है लेकिन अधिकांश न्यायालय इसे अपना नहीं पा रहे हैं। वे हमेशा देर क्यों कर देते हैं?”
मुनीर नियाजी आगे लिखते हैं
“मदद करनी हो उस की, यार की ढांढस बंधाना हो
बहुत देरीनी (दूरस्थ) राहों पर किसी से मिलने जाना हो
हमेशा देर कर देता हूँ, मैं”
यदि बुलडोज़र कथा पर लौटें तो पाएंगे कि पिछले एक दशक में न जाने कितने हजार घर-मकान ढहा दिये गए। उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में तो जैसे विप्लव ही आ गया। सबसे विकट एवं विकृत स्थिति यह बनी कि लोग स्वयं इस बात की मांग करने लगे कि कथित आरोपी का घर ढहा दिया जाए। सरकारों ने इस मामले में जनता की मांग का अक्षरशः पालन किया और मकान ढहा दिये। न्यायालय भी स्थगन देने में संकोच में पड़े रहे। इसकी वजह क्या पब्लिक डिमांड का “मान” रखना था?
महात्मा गांधी अपने लिए एक बेहद मजेदार वाक्य का प्रयोग उन दिनों के लिए करते हैं जो उनकी वकालत का शुरुआती दौर था। यह शब्द है “संवैधानिक शर्मीलापन” (Constitutional Shyness)। क्या हमारा समाज जिसमें न्यायालय भी शामिल हैं इस संवैधानिक शर्मीलेपन का शिकार होते जा रहे हैं? मदद करनी हो उसकी -----! जिन्हें आज न्यायालयीन हस्तक्षेप की जरुरत है, वह यदि उन्हें नहीं प्राप्त होती तो ऐसी व्यवस्था को किस तरह “न्यायसंगत” ठहराया जा सकता है।
पिछले दिनों एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा था कि हमने पूरा दिन एक जमानत याचिका को समर्पित कर दिया! यह बेहद विचारणीय और झकझोर देने वाली स्वीकारोक्ति है। गौरतलब है सर्वोच्च न्यायालय ने करीब 11 वर्ष पहले कोयला घोटाले की सुनवाई करते समय सी बी आई को “पिंजड़े में बंद तोता” कहा था। अब इसे दोहराने में यदि ग्यारह वर्ष लगेंगे तो तोता “मुक्त” कैसे हो पाएगा। वैसा ही कुछ “बुलडोज़र” वाले मामले में भी है। न्यायालय ने अभी इस पर दिशानिर्देश तैयार करने की पहल भर की है।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाशन, “भारत के न्यायालय: अतीत से वर्तमान” में वाल्टेयर: कानून के बारे में (On Laws) दार्शनिक शब्दकोष, के आधार पर एक कार्टून छापा है। उसके संवादों पर गौर करीये। वकील अपने मुवक्किल को दिलासा देते हुए
“खुश हो जाओ, तुम्हे अब कानूनी मदद मिल गई है।
मुवक्किल:- न्याय के बारे में क्या?
वाल्टेयर लिखते हैं : मेरे वकील ने मुझे बताया कि मैं किसी अन्य न्यायालय में जीत सकता था।
मैंने उनसे कहा, “यह तो बेहद हास्यास्पद है। यानी प्रत्येक न्यायालय के अपने कानून हैं?
उन्होंने कहां- हाँ
वाल्टेयर का जीवनकाल सन 1694 से 1778 तक का है। यानी उन्हें गुजरे करीब 330 बरस बीत गये हैं, लेकिन उपरोक्त कथन कई मायनों में आज बेहद भेड़ समकालीन जान पड़ता है।
अब महाराष्ट्र विधानसभा के मामले पर गौर करें। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका संभवतः जून 2022 से लंबित है और इसी महीने महाराष्ट्र विधानसभा के अगले चुनावों की घोषणा हो सकती है। तो फिर न्यायालय द्वारा एक विवादस्पद निर्णय पर समयबद्ध सुनवाई न करने से एक ऐसी सरकार शासन चलाती रही जिसकी वैधता ही संदिग्ध थी।
ऐसा ही कुछ-कुछ कारपोरेट चंदे को लेकर दिए गये निर्णय की दीर्घ अवधि को लेकर भी सामने आया है। एक राजनीतिक दल पूरी तरह से लाभ में रहा और बाकी के दल आहें भरते रहे। वहीं न मालूम क्यों उद्योगपतियों के मामले बेहद जल्दी-जल्दी निपट गए।
नियाजी साहब आगे लिखते हैं,
बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो,
किसी को याद रखना हो किसी को भूल जाना हो
हमेशा देर कर देता हूँ।
यह देरी सायास है या अनायास। कुछ याद रखना और कुछ भूलना स्वाभाविक प्रक्रिया है या चयन प्रक्रिया। इनमें बेहद मामूली विभाजन रेखा है। अब कोलकता बलात्कार कांड में उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दे देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप जांच को नए दिशानिर्देश देता है। वहीं हड़ताली डाक्टर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद काम पर नहीं लौटते। इस पर भी कोई त्वरित कार्यवाही सामने नहीं आती। खैर, कौन सा निर्णय या आदेश याद रखना है कौन सा नहीं यही तो न्यायालयीन विशेषाधिकार है।
अभी यह बात सामने आई कि वकीलों की कमी की वजह से मुकदमों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी और मेडिकल छात्र स्नातक, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 50 प्रतिशत से ज्यादा अगले कुछ वर्षों तक स्नातकोत्तर परीक्षाओं में बैठने के लिये स्वास्थ्य सेवाओं से नियमित तौर पर नहीं जुड़ पाते। अतएव हम कितने भी नये मेडिकल कालेज खोल लेंगे, डाक्टरों की कमी बनी रहेगी।
बड़ी संख्या में महिलाएं एक विशेष अवधि के बाद मेडिकल व्यवसाय से किनारा कर लेती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय इन परिस्थितियों के मद्देनजर चिकित्सकों के कार्य के बढ़ते समय पर गौर करेगा? शायद नहीं? क्योंकि तब यह मामला नीतिगत हो जाएगा। सजावटी कार्यवाहियों से समस्याओं का निदान संभव ही नहीं है।
“देरी” का स्थायी भाव बन जाना कहीं न कहीं स्वयं न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए दोषपूर्ण साबित हो रहा है। न्यायालयों को भारत में संभवतः सर्वाधिक स्वायत्तता प्राप्त है। वे चयन से लेकर प्रशासन तक प्रत्येक कार्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करने को सर्वाधिक स्वतंत्र हैं। इसके बावजूद कानूनी व्यवस्था की चलने की रफ्तार धीमी ही है।
सुनवाई के मुद्दों की प्राथमिकता तय करना भी उनके विशेषाधिकार का हिस्सा है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि चूक को सुधारने की जिम्मेदारी भी उन पर ही आती है। “ग्रामीण न्यायालय” के क्रियान्वयन में भारतीय न्यायव्यवस्था अभी तक असफल ही नजर आ रही है।
मुख्य मुद्दा है न्यायालयीन व्यवस्था में भरोसा स्थापित करना। चार्ल्स डि साल्वो अपनी पुस्तक “दि मेन बिफोर दी महात्मा : एम. के गांधी, अटार्नी एट लॉ” का अंत बेहद महत्वपूर्ण आंकलन से करते हैं। वे लिखते हैं “जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार न्यायालय में अपना जुर्म कबूल करने और दंड स्वीकार करने के लिए खड़े हुए थे तो प्रतिवादी गांधी ने, अधिवक्ता वकील गांधी का परित्याग कर दिया था और उन्होंने इसके बजाए यह दुनिया और इसके क़ानून कैसे होने चाहिए के प्रति अपनी श्रद्धा दर्ज कराई।
गांधी सन 1908 में दो बार और 1909 में एकबार और 1913 में पुनः जेल गये और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी दक्षिण अफ्रीका में सीखा था। उसे लेकर भारत आए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल गए। उन पर मुकदमा चलने के प्रत्येक अवसर पर जब भी उन पर सजा मुकर्रर हुई उन्होंने झुककर उसे स्वीकार किया। सजा या दंड को स्वीकार करके उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक व्यक्ति अपने निजी हितों से ऊपर उठकर अपने समुदाय की बेहतरी के काम आ सकता है। अपने बचाव को लेकर लगातार इंकार करने की वजह से उन्होंने एक जैसे न्याय की धारणा पर एकाग्र किया और सिविल नाफरमानी की वजह से वे उम्मीद की मशाल बन गये।”
सवाल आज सर्वोच्च न्यायालय वहां लंबित है। तमाम मामलों को लेकर है। सरदार सरोवर बांध में नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर अनुच्छेद 142 के विशेषाधिकार का प्रयोग कर निर्णय पर पुनर्विचार जरुरी है। निर्णय की शर्ती का पालन न करने के बावजूद बांध का स्तर अधिकतम ले जाने से और उसके समानांतर विस्थापन और पुनर्वास को समयबद्ध न कर पाने की वजह से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न्याय नहीं कर पा रहा है।
ऐसे तमाम लोग जो विकास से त्रस्त हैं या तमाम दमनकारी कानूनों की वजह से लंबे समय तक जेलों में है उन सबके लिये निर्णयों में हो रही देरी दुखदायी ही साबित हो रही है।
अंत में मुनीर नियाजी की नज्म के अंतिम शेर पर गौर फरमाइये,
“किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो
हकीकत और थी कुछ उस को जा के ये बताना हो
हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हर काम करने में”
देर को “दूर” करने वाली सुबह कभी तो आयेगी!