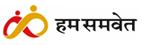पूर्वाग्रहों से मुक्ति ही स्वतंत्रता है
नेहरु ने गुलाम भारत में भारत की बागडोर संभाली, भारत को आजादी का द्वार पार कराया, भारत का संविधान तैयार कराया, वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव कराया और चुनाव को भारतीय लोकतंत्र का एक मानक या मानदंड बनाया अपवाद नहीं।

“स्वतंत्रता का इतना ही अर्थ है कि हम किसी से भी न डरकर जो हमारे दिल में हो वही कह सकें और वही कर सकें। जो लोग स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा को अधिक पसंद करते हैं, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं।” महात्मा गांधी
स्वतंत्रता को लेकर भारत में बहस लगातार एक मुद्दा बनी रहती है। एक वर्ग स्वतंत्रता के हनन से हतप्रभ है तो दूसरा स्वतंत्रता के कथित अतिरेक से। तर्कों और कुतर्कों के महासागर में अधिकांश लोग यह समझना ही नहीं चाहते कि भारत द्वारा 15 अगस्त 1947 को अर्जित स्वतंत्रता के क्या मायने हैं और किन लोगों ने किस तरह से इस मानव सभ्यता को स्वतंत्रता को देखने का एकदम नया नजरिया दिया। भारतीय स्वतंत्रता का अनूठापन उसका वह नजरिया ही है, जिसको समझकर वर्तमान “सभ्य” संसार स्वतंत्रता को वास्तव में अंगीकार कर सकता है।
भारतीय संदर्भों में स्वतंत्रता को 20वीं सदी के दो महानतम व्यक्तियों महात्मा गांधी और प. जवाहरलाल नेहरु को समझ कर ही समझा जा सकता है। इन दोनों के माध्यम से ही स्वतंत्रता की संभवतः अब तक की सबसे अनूठी परिभाषा भी स्वमेव विकसित हुई है और इसे इस तरह से व्याख्यायित किया जा सकता है कि, “स्वतंत्रता का अर्थ है अपने पूर्वाग्रहों से मुक्ति पा लेना।” यह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के संबंध में एक सी और एकसाथ लागू होती है।
गांधी कहते हैं, “मैं हिंसा का विरोध इसलिये करता हूँ कि वह जो भला करती दिखाई देती है, वह केवल अस्थायी भला होता है। लेकिन हिंसा जो बुराई पैदा करती है, वह स्थायी होती है। मैं इस बात को नहीं मानता कि प्रत्येक अंग्रेज को मार डालने से हिन्दुस्तान का थोड़ा भी भला होगा। अगर कोई आदमी कल प्रत्येक अंग्रेज की हत्या को संभव बना दे तो भी करोड़ों लोग उसी तरह दुखपूर्ण जीवन बितायेंगे, जिस तरह वे आज बिता रहे हैं। आज हमारे लोगों की जो स्थिति है, उसके लिये अंगेजों की अपेक्षा हम देशवासी ज्यादा जिम्मेदार हैं। अगर हम केवल भला ही काम करें, तो अंग्रेजों में बुरा काम करने की ताकत नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आंतरिक सुधार पर जोर देता हूँ।”
उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी क्रूर व दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से पूर्णतया मुक्त थे। वहीं, पंडित नेहरु के बारे में कहा गया है कि, “प्रजातंत्र, कानून का शासन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा के लिए सम्मान, सामाजिक समता और समानता, अहिंसा, राष्ट्र निर्माण हेतु माननीय सरोकारों के लिए न्यायप्रियता को मार्गदर्शक मानना और नैतिकता आधारित राजनीति ही राष्ट्र निर्माण को लेकर उनकी आधारभूत सोच थी। इस ध्येय की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और भारतीय जनमानस के प्रति उनका प्रेम और विश्वास ही उनकी मुख्य संपत्ति या गुण था।”
उपरोक्त प्रतिबद्धताओं से लैस नेहरु ने गुलाम भारत में भारत की बागडोर संभाली, भारत को आजादी का द्वार पार कराया, भारत का संविधान तैयार कराया, वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव कराया और चुनाव को भारतीय लोकतंत्र का एक मानक या मानदंड बनाया अपवाद नहीं। मानव सभ्यता को मार्क्स और एंजेल्स के बाद एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने वाले दो व्यक्ति मिले, जो मूलतः नजर तो गुरु-शिष्य जैसे आते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों अपने आप में परिपूर्ण ही हैं।
उपरोक्त संदर्भों में भारत की स्वतंत्रता का आकलन करने से स्पष्ट होता है कि आजाद होते ही भारत ने एकदम नए सिरे से स्वयं को गढ़ना शुरू किया। पहले अभी-अभी बांग्लादेश में जो हुआ, उस पर थोडा मनन कीजिए। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या, फौजी शासन, खालिदा जिया का शासन, शेख हसीना का शासन और अब विधार्थी विद्रोह तक की गाथा कमोवेश पूर्वाग्रहों और प्रतिशोध पर ही गतिमान है।
हालिया तख्ता पलट के बाद मंत्रियों आदि की गिरफ्तारी आगजनी एक प्रतिशोधात्मक रवैया ही हमारे सामने लाते हैं। परंतु भारत की आजादी के बाद शुरुआती शासन करने वालों में वे भी शामिल थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और भारत के विभाजन के लिए पूर्वरुपेण उत्तरदायी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार बनाई थी और तभी महात्मा गांधी को नोआखली में हिन्दुओं को नरसंहार से बचाने के लिए लगातार पदयात्रा करनी पडी थी। परंतु 15 अगस्त 1947 को भारत एकदम नई और साफ़ “स्लेट” था, जिस पर अब सब नए तरह से लिखा जाना था। भारत ने कि शासन द्वारा ब्रिटिश सम्मानपात्र, रायबहादुरों, जमींदारों, सर की पदवी पाए भारतीयों और क्रांतिकारियों के खिलाफ पैरवी कर उन्हें सजा, यहाँ तक फांसी दिलाने वाली किसी एक भी व्यक्ति के खिलाफ बदले की कोई कार्यवाही नहीं की।
यह दुनिया के इतिहास में अद्वितीय घटना है। जहां विदेशी शासक मित्र बनकर अपने मूल देश लौटता है और भारत में उसका साथ देने वाले अपने ही देश में अपराधी भी नहीं माने जाते। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठन गांधी-नेहरु को कमजोर मानते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं, वीर की क्षमा ही अर्थवान होती है। डरपोक या कमजोर क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो पहले से डरे हुए होते हैं।
गौर करिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आजादी के साथ कोई द्वेष नहीं लाया था बल्कि उसने पूरे भारत को करुणा के सागर में परिवार्तित कर दिया था। सन 1932 में गांधी और डा. अंबेडकर के बीच हुआ पूना समझौता भी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पूर्वाग्रहों से मुक्त कराने में सहायक हुआ है। भारतीय राजनीति या यूँ कहे कि भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक संघर्ष महात्मा गांधी और डा. अंबेडकर के बीच ही हुआ है। डा. अंबेडकर तो गांधी जी से कह ही चुके थे कि अछूत तो हिंदू धर्म का हिस्सा है ही नहीं। इसलिये उन्हें तो पृथक मतदान का अधिकार दिया जाए। वे एक हद तक ठीक भी थे कि हिन्दुओं ने अछूतों को अपना हिस्सा माना ही नहीं।
गांधी ने उनसे सहमति जताते हुए अंततः उन्हें मनाया और दलित हिंदू समाज का पहली बार अविभाज्य अंग बने। उन्हें चाहे गये से दुगने स्थान प्राप्त हुए और सामान्य स्थान (सीट) पर चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। डा. अंबेडकर का संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनना भी इसी विचार को मजबूती प्रदान करता है। यहां भी भारत अपने पूर्वाग्रहों से मुक्ति ही तो पाता है और नए क्षितिज की तलाश में लग जाता है।
निर्मल वर्मा एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि, “अनुभव के उन क्षणों जब व्यक्ति अपने को “धर्मसंकट” में पाता है, तो यह भी पता चलता है कि यह व्यक्ति का ही नहीं स्वयं “धर्म का संकट” भी है।” दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति और राष्ट्र के संकट दो अलग-अलग स्थितियां नहीं हैं। न्यायालय में न्याय न होना व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए एक सा घातक है। बांग्लादेश की हालिया घटना इसे एकदम स्पष्ट तौर पर सामने ला रही है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए कई निर्णय व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को असहज बना रहे हैं। यही बात राजनीति के साथ भी है। अनैतिक राजनीति व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए एक सी घातक है।
राहत इंदौरी समझाते हैं,
“टूट कर बिखरी हुई तलवार के टुकड़े समेट,
और अपने हार जाने का सबब मालूम कर।”
अतएव यह समझना होगा कि शासन महज अतिरिक्त दृढ़ता या असीम बल प्रयोग से सुचारू नहीं चलता। जितने अधिक सख्त और दमनकारी कानून बनते जायेंगे, वैसे-वैसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर खतरा और अविश्वास बढ़ता जाएगा। सख्त और दमनकारी कानूनों के जरिये शासन चलाने का अर्थ है कि सत्ता के सूत्र प्रत्यक्ष तौर पर पुलिस (कुछ मामलों में सेना- अर्ध सैनिक बलों) और न्यायालयों को हस्तांतरित होते चले जाएंगे और संविधान की उद्देशिका में निहित मूल्य कमजोर होते चले जाएंगे।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बंधुता, समता और व्यक्ति की गरिमा क्या दमनकारी कानूनों से प्राप्त किये जा सकते हैं? साथ ही इन्हें संविधान में निहित मूल अधिकारों से प्राप्त किया जा सकता है या उन्हें स्थगित करके या कमतर बना कर? ईसा मसीह कहते हैं, पापी में भी ईश्वर है और बुद्ध तो दो पापियों को संत बना देते हैं।
अंगुलीमाल की घटना से हम सब परिचित हैं। याद करिए वैशाली की अंबापाली की गाथा। वो एक बेहद स्वार्थी जीवन बिता रही थी। अपने आनंद के अलावा सब कुछ गौण था उसके लिए। उसने बुद्ध के बारे में सुना कि उनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं तो काफी नाराज हुई। इतना ही नहीं वह बुद्ध का अपमान करने अपने सर्वश्रेष्ठ आभूषण और वस्त्रों से लैस होकर बुद्ध के पास पहुंची। वहां पहुंच कर उसने बेहद घृणा और क्रोध के साथ बुद्ध को देखा। बुद्ध ने बेहद प्रेम और करुणा से उसकी ओर देखा वह शर्म से लाल हो गई।
बुद्ध ने उससे पूछा, “बेटी तुम्हारी इच्छा क्या है?” वह रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर गई और बोली महान सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए आप मेरे घर भोजन को पधारें। बुद्ध उसके घर गए क्योंकि कोई भी कभी इतना दीन हीन नहीं होता कि उसकी मदद न की जा सके। अंगुलीमाल को 1000 उँगलियों की माला में सिर्फ एक ऊंगली की कमी थी। तब बुद्ध उससे मिले। हजारों लोगों की हत्या करने वाला वह दैत्य बुद्ध की करुणा के सामने नतमस्तक हो गया। वो बदल गया। उसके भीतर का दिव्य जागृत हो गया और उसने बाकी का जीवन एक सन्यासी की तरह बिताया।
समय काल के हिसाब से तरीके बदल सकते हैं लेकिन बिना बातचीत और आपसी विश्वास के स्वतंत्रता को उसके सही अर्थों में स्थापित नहीं किया जा सकता। आज भारत में तमाम असहमत लोग वर्षों से जेलों में बंद है। दमनकारी कानूनों की बदौलत इन्हें लगातार निरुद्ध रखा जा रहा है। न्यायालय भी एक हद तक ही न्याय दिला पाने में सफल हो पा रहे हैं। कानून का राज और न्याय की व्यवस्था जैसे आज आमने सामने खडी दिख रहीं हैं, जबकि उन्हें तो समानांतर होना चाहिए। जो भी शासन कर रहा हो उसकी सफलता इसी में निहित है कि, वह आपसी बातचीत से समाधान तक पहुँचने को कितना महत्व देता है।
स्वराज्य-शास्त्र में विनोबा प्रश्न करते हैं
प्रश्न- क्या अहिंसा पर आधारित राज्य पद्धति टिक सकेगी?
उत्तर – इस प्रश्न के मूल में यह मान्यता-सी रही है कि हिंसा पर निर्मित राज्य पद्धति टिक सकती है। वस्तुतः अब तक के सारे इतिहास सभी ने राज्य पद्धति को स्थाई बनाने के लिए हिंसा के ही प्रयोग किए है। किन्तु कोई भी राज्य पद्धति हिंसा के आधार पर टिक सकी हो, ऐसा अनुभव कहीं भी नहीं हुआ। फिर भी अब तक हमारे मन पर हिंसा की ऐसी कुछ पकड़ बैठी हुई है कि हिंसा के हजारों बार असफल होने के बाद भी उसकी सफलता में हमारी श्रद्धा बनी हुई है।
विनोबा ने आजादी के पहले सन 1942 में स्वराज्य शास्त्र लिखा था। ध्यान रखिये भारत ने अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त कर वैश्विक सभ्यता को एकदम नया आयाम दे दिया। यह कोई दैवीय घटना नहीं थी। गांधी, नेहरु, विनोबा, पटेल, मौलाना आजाद जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने “सत्य और अहिंसा” पर लगातार विश्वास बनाये रखा और सत्ता, संघर्ष और क्रांति को लेकर जितने भी पुराने आग्रह, दुराग्रह या पूर्वाग्रह थे, उन्हें दरकिनार कर भारत की स्वतंत्रता की नींव करुणा के इस सिद्धांत पर रखी कि जो कुछ किया जाए “अंतिम व्यक्ति” को ध्यान में रखकर किया जाए। उसे यदि स्वतंत्रता नहीं मिली तो हम भी पूर्ण स्वतंत्र होने का वैध दावा तो नहीं कर सकते।
अन्त में राहत इंदौरी के इन दो शेरों पर बारी-बारी से गौर करिये। इन दोनों में समस्या और समाधान दोनों ही मौजूद हैं।
“हम अपने शहर में महफूज भी हैं, खुश भी हैं
ये सच भी नहीं है, मगर एतबार करना है।”
“न हमसफ़र न किसी हमनशीं से निकलेगा
हमारे पाँव का कांटा हमी से निकलेगा”