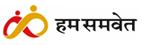राजनीतिक दर्शन में महंगाई, सांप्रदायिकता और भारतीय समाज
राजनीति में दार्शनिकता का सर्वथा अभाव नजर आ रहा है। इसलिए तात्कालिकता हावी है और वह किसी भी तरह के संघर्ष की बुनियाद को मजबूत बनने ही नहीं दे रही। जॉन एलिया की पंक्तियां इसीलिए आज बेहद महत्वपूर्ण है। हम अब बिना शरीर छोड़े ही किसी और के कंधों पर सवार हो गये हैं और अब यह उन कंधों पर निर्भर है कि वह हमें कहा ले जाएं। आम नागरिक बेहद यंत्रवत व्यवहार में डूब सा गया है। उन्हें हर ओर से लालच और प्रलोभन दिया जा रहा है और हमारा स्नायुतंत्र उसी के वशीभूत हो गया है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगौर इस प्रवत्ति को 100 साल से भी पहले तकरीबन सन् 1917 में पहचान गए थे। वे लिखते है, ‘‘जो प्रलोभन शक्तिशाली के लिए घातक है, वह कमजोर के लिए तो और भी ज्यादा घातक होगा। भारतीय जीवन के लिए मैं कभी इसका स्वागत नहीं करुंगा, भले ही यह अमीरों के ईश्वर द्वारा क्यों न भेजा जाए, मेरी तो प्रार्थना है कि हमारा जीवन बाहर से सादा तथा भीतर से समृद्ध हो। हमारी सभ्यता सामाजिक सहयोग के आधार पर दृढ़ता से टिकी रहे, न कि आर्थिक शोषण व संघर्ष के आधार पर। जब हमारे जीवन तत्व पर आर्थिक अजगरों के दांत गड़े हों, तब यह कैसे संभव होगा।

शम्मीर (तलवार) मेरी, मेरी सिपर (ढाल) किसके पास है.. वो मेरा खुद, पर, मिरा सिर किसके पास है.... दरपेश एक काम है हिम्मत का साथियों, कसना है मुझको, मेरी कमर किसके पास है ? जॉन एलिया
भारत में मंहगाई बेतहाशा बढ़ रही है। अखबार वगैरह भी कभी-कभार इस पर बात कर लेते हैं। वैसे उनका पूरा ध्यान पेट्रोलियम पदार्थों यानी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के आसपास ही लगा रहता है। चलते-चलते कभी-कभार गेहूं, चावल, आटा, तेल, साबुन, मसालों की भी चर्चा कर लेते हैं। हमने अपने प्रतिरोध के सारे उपकरण अन्य लोगों को सौंप दिए हैं। हमारा सबकुछ कहीं और गिरवी हो गया है।
गौर करिए आज, बढ़ती महंगाई और बढ़ती सांप्रदायिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महंगाई पर रोक को लेकर सरकार का बेबस हो जाना, अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता में आए उछाल की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है | मुख्य समस्याएं हैं, महंगाई व बेरोजगारी, परंतु इसे धार्मिक उन्माद से दबाने का कमोवेश सफल रास्ता निकाला जा रहा है। क्या सरकार हमें यह समझा सकती है कि जब देश में गेहूँ और चावल का आधिक्य (अतिरिक्त) है तो फिर इन दोनों खाद्यान्नों और आटे के भाव क्रमशः 40 व 30 प्रतिशत क्यों बढ़े? जिस वस्तु की कमी हो या आयात होता हो, उसके भाव बढ़ना तो एक हद तक न्यायोचित (हमेशा नहीं) ठहराया जा सकता है, लेकिन जो वस्तु देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उसके दाम क्यों बढ़े? क्या निर्यात के लिए देश के नागरिकों को तड़पाया जाना उचित है?
खाने के विभिन्न तेलों के दाम 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ गए। भवन निर्माण आदि में काम आने वाले सरिये का दाम कमोवेश दोगुना हो गया। आज वह 82 हजार रु. टन यानी 82 रु. किलो है। सीमेंट व रेती-गिट्टी के भाव आसमान छू रहे हैं। अनेक बड़े शहरों में बिल्डरों ने भवन निर्माण को अस्थाई तौर पर रोक दिया है। परंतु मनुष्य के पेट का क्या करें, उसे तो दिन में दो बार (कम से कम) भूख लगती ही है।
तो बात यहीं नहीं रुकती। सरकार ने पिछले 12 दिनों में पेट्रोलियम पदार्थो के भाव में 10 बार वृद्धि की। इससे यात्री व मालभाड़ा महंगा हुआ और दाम बढ़ने लगे। पर सरकार यहीं नहीं रुकी। उसने तो तय कर लिया है कि आम या खास कोई भी हो, उसका सुख-चैन छीन ही लेगी। सरकार ने टोल टेक्स में बढ़ोत्तरी को भी मंजूरी दे दी। चाहती तो इसे टाल सकती थी। सरकार ने जीवनरक्षक दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति भी दे दी।
दूसरी ओर सांप्रदायिकता की जैसे सुनामी ही आती जा रही है। कर्नाटक का हिजाब विवाद, हिन्दू देवस्थानों पर मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार से होता हुआ हलाल (मांसाहारी भोजन) तक पहुच गया। कर्नाटक से उठी सांप्रदायिकता की आंच की तपन इंदौर जैसे शहरों में पहुंच गई है और यहां भी हिन्दू धार्मिक स्थलों में छोटे-बड़े मुस्लिम दुकानदारों के व्यवसाय को रोकने की बात खुल कर सामने आने लगी है।
हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में पेट्रोल-डीजल, व खाने-पीने की वस्तुओं के अलावा अब बिजली और यहां तक कि विद्यार्थियों के लिए नोटबुक (कागज) तक की जबरदस्त कमी हो गई है और छात्रों की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। अखबार निकलना बंद हो गए हैं। जातीय व सांप्रदायिक संघर्ष ने श्रीलंका जैसे बेहद विकासशील राष्ट्र को कहीं का नहीं छोड़ा और कोरोना ने तो उसे पूरी तरह खोखला कर दिया। राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल व कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन भूख न तो आपातकाल को तो जानती है और न कर्फ्यू को भारत में चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत ने सत्ताधारी दल को समझा दिया है कि जनता से जुड़े रोजमर्रा के मुद्दे जनता को प्रभावित ही नहीं करते और सत्ता के खिलाफ जाने के लिए उन्हें प्रेरित भी नहीं करते।
इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारत में मँहगाई आदि के खिलाफ कोई व्यापक और लंबा संघर्ष, पिछले एक दशक में सामने नहीं आ रहा है। अभी जो सत्ता में हैं वे मुद्दों को किसी प्रतीक से दबा देते हैं। उनकी चालाकी अंततः देश के लिए घातक ही सिद्ध होगी। परिवर्तन का कोई नैसर्गिक मार्ग सुझाई नहीं दे रहा है। राजनीति में दार्शनिकता का सर्वथा अभाव नजर आ रहा है। इसलिए तात्कालिकता हावी है और वह किसी भी तरह के संघर्ष की बुनियाद को मजबूत बनने ही नहीं दे रही। जॉन एलिया की पंक्तियां इसीलिए आज बेहद महत्वपूर्ण है। हम अब बिना शरीर छोड़े ही किसी और के कंधों पर सवार हो गये हैं और अब यह उन कंधों पर निर्भर है कि वह हमें कहा ले जाएं। आम नागरिक बेहद यंत्रवत व्यवहार में डूब सा गया है। उन्हें हर ओर से लालच और प्रलोभन दिया जा रहा है और हमारा स्नायुतंत्र उसी के वशीभूत हो गया है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगौर इस प्रवत्ति को 100 साल से भी पहले तकरीबन सन् 1917 में पहचान गए थे। वे लिखते है, ‘‘जो प्रलोभन शक्तिशाली के लिए घातक है, वह कमजोर के लिए तो और भी ज्यादा घातक होगा। भारतीय जीवन के लिए मैं कभी इसका स्वागत नहीं करुंगा, भले ही यह अमीरों के ईश्वर द्वारा क्यों न भेजा जाए, मेरी तो प्रार्थना है कि हमारा जीवन बाहर से सादा तथा भीतर से समृद्ध हो। हमारी सभ्यता सामाजिक सहयोग के आधार पर दृढ़ता से टिकी रहे, न कि आर्थिक शोषण व संघर्ष के आधार पर। जब हमारे जीवन तत्व पर आर्थिक अजगरों के दांत गड़े हों, तब यह कैसे संभव होगा।’’
इस पूरे उद्धहरण को यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आकें तो साफ नजर आता है कि छोटे-छोटे प्रलोभनों से बड़े-बड़े स्वार्थ साधे जा रहे हैं। अमीरों के ईश्वर कौन हैं ? ये वे जानते थे, समझते थे और ये अमीरों के ईश्वर वर्तमान समय में हमारे सामने चट्टान बने खड़े हैं। सामाजिक सहयोग को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। भारत जातीय संघर्ष को समाप्त नहीं कर पाया था कि सांप्रदायिकता का बवंडर नए सिरे से सामने आ गया | महंगाई जैसी हर वक्त प्रभावित करने वाली त्रासदी भी अब हमें विचलित नहीं कर पाती है और हम भूखे पेट डकार ले रहे हैं। इस अन्यायपूर्ण स्थिति से कैसे निपटा जाए? राजनीतिज्ञों ने घनघोर असुरक्षा का वातावरण तैयार कर दिया है। ऐसे में कोई भी अपने घरों से बाहर आकर बात करने को कतई तैयार ही नहीं है। कहीं से कोई आवाज आती सुनाई नहीं देती। इन पंक्तियों पर गौर करिए,
कोई नहीं खामोश, कोई पुकारता नहीं
शहर में एक शोर है और कोई सदा (आवाज) नहीं।
रोजमर्रा की अनिवार्यता वाली वस्तुओं के दामों में एक-डेढ़ महीनों में 40 प्रतिशत की वृद्धि से पूरे देश में खलबली तो मची हुई है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। विरोध में जो स्वर उठ भी रहे हैं, वे अपनी आवाज को गूंज में परिवर्तित कर पाने के इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक दिन या एक सप्ताह का विरोध प्रदर्शन जड़ हो चुकी आवाज को पुनः स्पंदित नहीं कर सकता। आँखे खोलेंगे तो पाएंगे कि एक विशिष्ट धर्म के लोगों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है और दूसरी ओर आकंठ कर्ज में डूबी राज्य सरकार एक अन्य विशिष्ट धर्म के स्थलों को विकसित करने हेतु करीब 1,100 करोड़ रु. का बजट में प्रावधान कर रही है।
मुख्य मुद्दों से ध्यान बंटाने की यह नई कला वास्तव में एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रही है जिसमें कि सारा वातावरण दमघोंटू होता चला जाएगा। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त हैं। किसी एक के अधिकार को छीनने से दूसरा शक्तिशाली नहीं बनता। अंततः दोनों ही कमजोर होते चले जाते हैं। महंगाई को सामान्य चर्चा से बाहर कर देने से महंगाई कहीं बाहर नहीं चली जाएगी। खाली पेट तो बजेंगे ही। थोड़े दिन तक गगनभेदी नारे इन खाली पेटों की आवाज को दबा लेंगे, लेकिन अंततः तो यह आवाज सबसे ऊपर निकल ही जाएगी क्योंकि भूख मानव सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी और यंत्रणा दोनों ही है। याद रखिए विगत आठ वर्षों में सरकारी अनुदान से मिले खाद्यान्न पर निर्भर रहने वालों की संख्या 20 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ तक पहुंच गई है। यदि स्थितियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह संख्या कहां पर रुकेगी, यह अकल्पनीय है।
राहुल सांकृत्यान लिखते हैं, ‘‘गरीबों की गरीबी और दरिद्रता के जीवन का कोई बदला नहीं। हाँ, यदि वे हर एकादशी के उपवास, हर रमजान के रोजे तथा सभी तीरथ-व्रत, हज और जियारत बिना नागा और बिना बेपरवाही से करते रहे, अपने पेट को काटकर यदि पंडे - मुजावरों का पेट भरते रहें, तो उन्हें भी स्वर्ग और बहिश्त के किसी कोने में कोठरी तथा बची-खुची हूर अप्सरा मिल जाएगी। गरीबों को बस इसी स्वर्ग की उम्मीद पर अपनी जिंदगी काटनी है।’’
यह अजीब सी बात है कि भारतीय समाज आगे बढ़ते-बढ़ते यकायक बिना पीछे मुड़े उल्टा चलने लगा। उसे लगने लगा है कि वह जो कुछ भी पाना चाहता है, वह तो सामने है, लेकिन उसे आगे चलकर हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए वह पीछे की ओर चल पड़ा है और समझ ही नहीं पा रहा है कि बिना पीछे देखे चलने से वह खाई में गिर सकता है। मगर उस पर एक नशा सा चढ़ गया है। सांप्रदायिकता का यह नशा उसे लगातार रोमांचित कर रहा है। सबकुछ जैसे हमारी - आपकी अस्मिता पर आकर अटक गया हो। यह अस्मिता भी परिभाषित नहीं है। इसलिए कभी उसकी खोज किसी धर्मस्थल में तो कभी किसी फिल्म में तलाशी जा रही है। वहीं पूरी तरह से परिभाषित महंगाई, भूख, गरीबी, बीमारी अमूर्त व्याख्या का शिकार हो गई हैं। दुःखद तो यह है कि सार्वजनिक तौर पर कहा जा रहा है कि जुमलेबाजी से चुनाव जीते जा सकते हैं और यह स्वीकारा जा रहा है कि हमने जो कहा था वह जुमलेबाजी ही थी।
गौर से सोचिए, रुस की धरती पर दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पहली बार किसी अन्य देश ने हमला किया। हमला भी ऐसे देश ने किया, जिसे वह नेस्तनाबूत कर देना चाहता है, काफी हद तक कर भी चुका है। परंतु युक्रेन ने वह संभव कर दिखाया जो पिछले 77 वर्षों से नहीं हुआ था। इसी परिप्रेक्ष्य में सोचिए कि बढ़ती मँहगाई और इसके परिणामस्वरूप बढ़ती गरीबी, भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद दर्दनाक व खतरनाक है। महंगाई की व्यापकता को कम करने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ने देना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
अतीत में भारत के राजनीतिज्ञ कतिपय ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर चुके हैं, जिन्होंने उन्हें ही शिकार बनाया है। इसलिए आवश्यक है कि महंगाई को महंगाई ही रहने दें और उसे आर्थिक ताने-बाने से काबू में लाएं। बापू ने समझाया है, ‘‘कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहां आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एकदूसरे के साथ आजादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज हैं।’’ तो हम सबको समझना होगा कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही और सांप्रदायिकता क्यों फैल रही है।