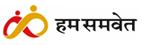Independence Day 2025: एक तमन्ना का पूरा होना, आजादी के संघर्ष के नौ दशक
स्वतंत्रता दिवस पर महात्मा गांधी की स्वतंत्रता की इस व्याख्या पर गौर करें, “सत्य और अहिंसा के जरिये सम्पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति का मतलब है, जात-पात, वर्ण या धर्म के भेद से रहित राष्ट्र के प्रत्येक घटक की और उसमें भी उसके गरीब से गरीब व्यक्ति की स्वतंत्रता की सिद्धि। इस स्वतंत्रता से किसी को भी दूर नहीं रखा जा सकता।” क्या पिछले आठ दशकों में यह पूरी तरह संभव हो पाया है? सोचिए। जवाब आपके ही पास है।

“आज शहीदों ने है तुमकों अहले वतन ललकारा.
तोड़ो गुलामी की जंजीरे बरसाओ अंगारा,
हिन्दू, मुस्लमां, सिख हमारा भाई-भाई प्यारा,
यह है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा”
:- सन 1857 के संग्राम के बागी सैनिकों का कौमी गीत
स्वतंत्रता दिवस को मनाने के समानांतर यह भी अनिवार्य है कि भारत के इस मुकाम पर पहुँचने की यात्रा या संघर्ष को भी ठीक-ठीक समझा जाए। उसी के बाद हम शायद यह जान पायें कि किसी लक्ष्य को पा लेने के बाद उसकी पृष्ठभूमि को बिसरा देना लक्ष्य के निहितार्थों और उद्देश्यों से भटक जाना भी होता है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इतिहास से (या में) कुछ भी न तो मिटता है और न मिटाया जा सकता है। वह सिर्फ छिप जाता है। हम जब भी धूल हटायेंगे वह फिर हमारे सामने ठीक उसी तरह होता है, जैसा कि उसके “वर्तमान” में वह रहा होगा।
इतिहास के आईने से अपना चेहरा हटा भी लें तो भी वह आईना पूरी पृष्ठभूमि तो झलकाता ही रहेगा। 23 जून 1757 को बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुए युद्ध में नवाब की हार हुई और जो कंपनी यहां व्यापार करने आई थी वह राज करने लगी। इसके ठीक 100 साल बाद सन 1857 में ईस्ट इंड़िया कंपनी के खिलाफ व्यापक स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसके बीच सन 1795, और 1806 में भी संघर्ष हुआ। इसके बाद करीब आधी शताब्दी तक कंपनी का विस्तार और राज निर्बाध जारी रहा।
29 मार्च 1857 को बंगाल के ही बहरमपुर में मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अफसरों को मार कर स्वतंत्रता संग्राम की नीव रखी। अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को महज 10 दिनों में मुकदमा चलाकर फाँसी पर चढ़ा दिया। परन्तु इसका प्रभाव यह हुआ कि 31 मई 1857 को पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई। यह संग्राम बरहमपुर, मेरठ, झांसी, कानपुर, महू, हैदराबाद, बिहार, महाराष्ट्र सहित तक़रीबन पूरे देश में विस्तारित होता चला गया।
पहला स्वतंत्रता संग्राम इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने वास्तव में पहली बार भारत को दृढ़ता के साथ आपस में जोड़ा था। यह संघर्ष शताब्दियों बाद भारत को एकबार पुनः एकसूत्र में पिरोने में सहायक बना। स्वतंत्रता दिवस पर इस संघर्ष को याद करने का निहितार्थ यह भी है कि हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश से दूरियां कम हों। इस संघर्ष में जो शहीद हुए वे मूलतः स्वतंत्रता के उपासक थे। इस स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की संख्या को लेकर भिन्नता है। परंतु यह न्यूनतम 4 (चार) लाख से अधिकतम 10 (दस) लाख के मध्य रही। वैसे अंग्रेज इसमें अकाल, महामारी की गिनती भी करते हैं। वैसे इस संग्राम में 6,000 अंग्रेज मारे गए। इतना ही संघर्ष की समाप्ति के बाद करीब एक लाख भारतीयों को मार डाला गया था।
हमें इस संघर्ष की व्यापकता को जानना जरुरी है। बात साम्राज्यवाद पर गांधी के दृष्टिकोण से शुरू करते हैं। उनके अनुसार, “जहां तक साम्राज्यवाद का सवाल है, तो मैं जहां भी देखता हूँ वहां झूठ, धोखा, घमंड, अत्याचार, नशाखोरी, जुआबाजी, व्यभिचार, रात दिन लूट और डायरवाद ही दिखाई देता है। साम्राज्य की वेदी पर सब कुछ बलिदान किया जाता है। वह केवल व्यापार के लिए जीता है और उसकी रक्षा के लिए मरता भी है।” यह बात ब्रिटिश साम्राज्य पर लागू होती थी और आज कथित लोकतंत्र के प्रणेता बने अमेरिका पर भी। इन दोनों राष्ट्रों का अंततः निशाना भारत ही था और है।
बहरहाल दस लाख लोगों के बलिदान से शुरू इस संघर्ष के एक हमराह, अवध के नवाब वाजिदअली शाह “अख्तर” तत्कालीन हालत को कुछ यूँ बयां करते हैं,
“सारे अब शहर से होता है “अख्तर” रुखसत,
आगे बस अब नहीं कहने की है मुझको फुर्सत,
हो न बर्बाद मिरे मुल्क की यारब खल्कत,
दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं,
रुखसते अहले वतन! हम तो सफ़र करते हैं।”
अवध का संघर्ष हमारी आँखों के सामने आज भी तैर जाता है। भारत की आजादी का यह शुरुआती संघर्ष अनेक मायनों में आजाद भारत की परिकल्पना भी सामने रखता है। एक ओर अनूठे धार्मिक समभाव और वर्गविहीनता की शुरुआत होती है तो दूसरी ओर भयानक स्वार्थ परकता भी सामने आती है। इसी दौर में बेगम हजरत महल कहती हैं,
“एक तमन्ना थी कि आजाद वतन हो जाए,
जिसने जीने न दिया, चैन से मरने न दिया”
नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के साथ जो हुआ या उनका हश्र हमें मालूम है और उसे लेकर विभिन्न विचार भी हमारे सामने हैं। परंतु ख़ास बात उस दौर के समाज और उसके आचरण की है जो बेहद साफ़गोई एवं दृढ़ता के साथ एक धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रख रहा था। शाही परिवार की वेदना के समानांतर अवध के बाशिंदे किस सोच के साथ इस संघर्ष से जुड़े थे, उसकी बानगी अवध लोकगीत की निम्न पंक्तियों में साकार होती है,
“मत छोड़िये रे हथियार / अल्ला है बेली ।
मत छोड़िये रे हथियार / हो राम रावैया ।
मरना न दूसरी बार / देवों भा चेता ।
मुरुभा बाँकुडों / मत छोडियों रे हथियार”
अंग्रेजों द्वारा करीब एक शताब्दी के “फूट डालो राज करो” का जवाब पूरा हिन्दुस्तान अपनी तरह से बिना किसी शोर-शराब के दे रहा था। एक ऐसे में जब “सुराज” का नाम लेना भी अपराध था, तब बुंदेलखंड के निवासी इस तरह से सच्चाई सामने रख रहे थे,
“बुंदेलखंड को गांउन-गांउन, फेर ढ़ोडरे पिटवाओ,
जो सूरज का नाम लेवेंगे, तो हम कीला ठुकवाओं,
गांवन-गांवन में पी.ए. फिशर ने करो दमन भौंतई भारी,
अंग्रेजन के गुलाम राजा, तिनके हम गुलाम भारी।"
तो सुराज को लेकर बुंदेलखंड का संघर्ष जन-जन में पैठ तो कर ही गया था। वहीं की महज बीस (20) वर्ष की रानी लक्ष्मीबाई सन 1857 के संघर्ष की एक प्रमुखता प्रतीक ही नहीं किवदन्ती बन गई। इंदौर के पास स्थित महू छावनी से सर ह्यूरोज जो 6 जनवरी 1858 को चला था। रायगढ़, सागर, बानापुर, चंदेरी जैसी अनेक रियासतों को जीतता हुआ 20 मार्च को सेना के साथ झांसी के नजदीक पहुंचा था। वहां उसका रानी लक्ष्मीबाई से संघर्ष हुआ।
पं सुंदरलाल लिखते हैं, “26 तारीख की दोपहर को कंपनी की सेना ने नगर के दक्षिणी फाटक पर इतने जोर से गोले बरसाए कि उस तरफ की झांसी की तोपें ठंडी हो गई। इस पर पश्चिमी फाटक के तोपची ने अपनी तोप का मुंह उस ओर कर शत्रु के ऊपर गोले बरसाने शुरू किये। गोले ने अंगरेजी सेना के सबसे अच्छे तोपची को उड़ा दिया। इस पर अंगरेजी तोप ठंडी हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने खुश होकर अपनी ओर के तोपची को, जिसका नाम गुलाम गौस खां था, सोने का कड़ा इनाम में दिया।” दुःख की बात यही है कि हमारी कहानियां नायक/नायिका पर आकर स्थिर हो जाती हैं, अटक जाती है। उसमें हजारों हजार “गुलाम गौस खां” के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आगे तो जो हुआ हमें मालूम है। करीब तीन महीने बाद 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से तो हम सभी परिचित है, लेकिन उस भयानक युद्ध के दौरान बुंदेलखंड का “लोक” गा रहा था,
“दरिया में तूफ़ान / बड़ी दूर इंगलिस्तान,
जल्दी जाओं, जल्दी जाओ / फिरंगी बेईमान।”
तो यह संघर्ष तब तक जनसंघर्ष का रूप ले चुका था। पूरे देश में इस दौरान रचे लोकगीत इसके प्रमाण हैं। मध्य भारत में तात्या टोपे की रणनीति को लेकर तत्कालीन “लंदन टाइम्स” में जो छपा है उसे पढ़कर रोमांच हो आता है। पत्र लिखता है “हमारा अत्यंत अद्भुत मित्र तात्या टोपे इतना कष्ट देने वाला और चालाक शत्रु है कि उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। पिछले जून महीने से उसने मध्य भारत में तहलका मचा रखा है।” काफी लंबी रिपोर्ट है।
गौरलतब है तात्या अक्टूबर 1858 में अपनी सेना सहित राव साहब और बांदा के नवाब के साथ नागपुर तक पहुँच गए थे। नवाब बांदा ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः 18 अप्रैल 1959 को करीब दो वर्ष तक संघर्ष के बाद उनके साथ हुए विश्वासघात के बाद, उन्हें फाँसी दे दी गई। उसके बाद फीरोज शाह और राव साहब बच निकले थे। अंततः सन 1862 में यानी करीब 5 वर्षों तक संघर्ष चलने बाद अंतिम रूप से भारत अंग्रेजों के हाथ आ पाया था।
इसी दौरान ब्रज भूमि भी पीछे नहीं थी। वह यह लोरी गा रही थी,
“री बहना मेरी भारत में फिरंगी डाकू धंसि आए
जिनने डारी ये लूट मचाया, री बहना”
एक ओर जहां इस लूट की गूंज थी तो वहीँ इस लोरी पर गौर करिये “ भारत के लोग आज दाना बिना तरसे भैया / लन्दन में कुतवा उड़ावे मजा माल / हो विदेशी तौर रजक में।”
वहीं दूसरी ओर ब्रज के एक और अंचल में गूंज रहा था
“फिरंगी लुट गयो रे, हाथरस के बाजार में,
गोरा लुट गयो रे, हाथरस के बाजार में,
टोप लुट गयो, घोड़ा लुट गयो,
तमंचा लुट गयो, जाको चलते बाजार में।”
वहीं ब्रज से लगा हरियाणा गा रहा था,
“आठ फिरंगी नौ गोरा/ लड़े जाट का दो छोरा।”
यह संघर्ष शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्रों में भी फ़ैल गया था। सन 1857 में गाये जाने वाले एक गोंडी गीत की पंक्तियाँ हैं,
हम भारत के गोंड बैगा, आजादी ख्यार।
अंग्रेजन ला भार भगाओं, भारत ले रे।।
भारत तब तक पूरा आकार ले चुका था। एक सुद्दढ राष्ट्र बनने की प्रक्रिया भी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। पडौस में बसा आदिवासी छतीसगढ़ गा रहा था,
धधके लगिस वीर बंगाल,
दिल्ली के रंग होंगे लाल,
माचिस रकत होले फाग,
आजादी के पहिली राग,
कांपिस अंग्रेज शासन,
डोलिस लंदन के शासन।
इस सबके साथ-साथ दिल्ली भी दहल रही थी। बादशाह बहादूर शाह जफ़र, एक बार पुनः भारत के सम्राट बनाये गए। उनके दो बेटों मिर्जा मुग़ल और मिर्जा असगर सुल्तान के साथ उनके पोते अब बुकर हुमांयु को गिरफ्तार कर मार डाला गया। मुगलवंश खत्म हो गया। जब उन तीनों के कटे सिर बादशाह के सामने लाये गए तो उस बुजुर्ग बादशाह ने जो कहा वह सचमुच थर्रा देता है।
वे धैर्यपूर्वक बोले,
“अलहमदुलिल्लाह तैमूर की औलाद ऐसी ही सुर्खरु होकर बाप के सामने आया करती थीं।”
इसी रौ वे कहते हैं,
न था शहर देहली / यह था चमन,
फकत अब तो उजड़ा दयार है,
जो खिताब था वह मिटा दिया,
फकत अब तो उजड़ा दयार है,
यही तंग हाल तो सबका है,
यह करिश्मा कुदरते रबका है,
जो बहार थी वह खिजा हुई,
जो खिजा (पतझड़) थी वह अब बहार है।
पहले स्वतंत्रता संग्राम को इन तमाम लोक गीतों आदि के जरिये देखना-समझना शायद हमें आपस में और भी जोड़े। वहीँ सन 1858 में मलका विक्टोरिया द्वारा भारत को ब्रिटिश सरकार के अधीन करने का फरमान जहां हमारी गुलामी पर मोहर लगाता है। वहीं, दूसरी ओर बेगम हजरत महल का जवाब हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की लौ जलाए रखता है।
दिल्ली उजड़ी कलकत्ता को राजधानी बनाया गया। अंग्रेजों ने बाद में दिल्ली को पुनः राजधानी बनाया और राज भी किया। पंरतु अंततः उन्हें यहां से जाना पड़ा। पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद के 90 साल कमोवेश मुक्ति संघर्ष के ही रहे हैं। सन 1915 में महात्मा गांधी के इसमें प्रवेश के बाद लक्ष्य प्राप्ति का तरीका बदला मगर उद्देश्य और भावना तो वही बनी रही। तभी तो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पंडित नेहरु ने आजाद भारत के पहले उद्बोधन में कहा था, “भारत के सपने दुनिया के सपने भी हैं। क्योंकि आज सभी राष्ट्र एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि कोई अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता।” वे आगे कहते हैं, “भारत संसार में अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण करेगा और संसार व्यापी शांति और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए योगदान करेगा।”
आजादी के 78 बरस बाद भारत आज पुनः दो राहे पर खड़ा है। पूरी दुनिया हिंसा और नस्लीय और धार्मिक अतिवादिता के दौर में पहुँच गई दिखती है। ऐसे में आवश्यकता है कि भारत अपने आजादी के संघर्ष और आदर्शों को पुनः समझे और उन्हें नए सिरे से अपनाए। स्वतंत्रता दिवस पर महात्मा गांधी की स्वतंत्रता की इस व्याख्या पर गौर करें, “सत्य और अहिंसा के जरिये सम्पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति का मतलब है, जाट-पात, वर्ण या धर्म के भेद से रहित राष्ट्र के प्रत्येक घटक की और उसमें भी उसके गरीब से गरीब व्यक्ति की स्वतंत्रता की सिद्धि। इस स्वतंत्रता से किसी को भी दूर नहीं रखा जा सकता।” क्या पिछले आठ दशकों में यह पूरी तरह संभव हो पाया है? सोचिए! जवाब आपके ही पास है।
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।