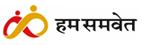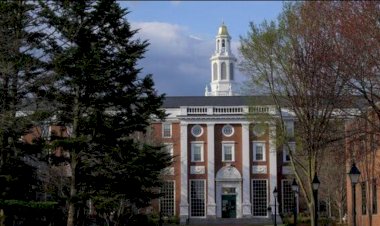जानलेवा साबित हो रहा है एक्स्ट्रीम वेदर, हर साल 18.9 करोड़ लोग हो रहे प्रभावित
इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक 273 दिनों में से 270 दिन देश के किसी न किसी हिस्से को मौसम की एक्स्ट्रीम वेदर का सामना करना पड़ा है। इन घटनाओं में 4064 लोगों की जानें गई, 99,533 घर ढह गए, 94.7 हेक्टेयर खेत में फसल बर्बाद हो गई और 58,982 मवेशी मारे गए।

भारत में चरम मौसम (एक्स्ट्रीम वेदर ) तेजी से बढ़ रहे हैं और अब यह केवल मौसमी उतार–चढ़ाव नहीं, बल्कि जीवन और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। हीटवेव, बाढ़, चक्रवात, सूखा, बादल फटना, आकाशिय बिजली गिरने, समुद्री तूफान और हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झील फटना जैसी घटनाएं पिछले एक दशक में रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं की आवृत्ति, अवधि और तीव्रता में बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का स्पष्ट संकेत है।
इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक 273 दिनों में से 270 दिन देश के किसी न किसी हिस्से को मौसम की एक्स्ट्रीम वेदर का सामना करना पड़ा है। इन घटनाओं में 4064 लोगों की जानें गई, 99,533 घर ढह गए, 94.7 हेक्टेयर खेत में फसल बर्बाद हो गई और 58,982 मवेशी मारे गए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 532 लोगों की मौत हुई है। पिछले तीन वर्षों में 2022 में 241,2023 में 235 और 2024 में 255 दिनों तक एक्स्ट्रीम वेदर रहा था, जिसके कारण क्रमशः 2755, 2923 और 3238 लोगों की जानें गई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के जलवायु, पर्यावरण और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वायु प्रदुषण से विश्व में प्रतिवर्ष 90 लाख मौतें होती है। इसके अलावा 18.9 करोड़ लोग हर साल चरम मौसम से जुड़ी घटनाओं से प्रभावित होते हैं। भारत में 1990 से 2020 के बीच चरम मौसम से 100 बिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है।
जर्मन वाच के एक नए क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार, पिछले 30 वर्षों में चरम मौसम से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत नौवें स्थान पर है।
इस चरम मौसम के कारण सबसे ज्यादा मछुआरा समुदाय, तटीय मजदूर, किसान और दिहाड़ी कामगार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
द लैंसेट काउंटडाउन 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ती गर्मी से हर मिनट एक व्यक्ति की मौत हो रही है और गरीब देशों की आय का छह फीसदी हिस्सा खत्म हो गया है। 'ट्राॅपिकल मेडिसिन एंड हेल्थ' जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशिया में हर साल 2 लाख से अधिक लोग बेहद गर्मी से जान गंवा रहे हैं। अनुमान है कि 2045 तक यह संख्या 4 लाख प्रतिवर्ष तक पहुंच सकती है। यानी हर घंटे 46 लोगों की मौत हो सकती है। पृथ्वी पर जीवन हमेशा गतिमान रहा है, चाहे इंसान हो या दूसरे जीव हमेशा एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते रहते हैं। वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा किए इस नए अध्ययन से पता चला है कि इंसानों की कुल आवाजाही अब धरती पर मौजूद सभी जंगली जानवरों, पक्षियों, स्तनधारियों और कीटों की कुल हलचल से करीब 40 गुणा ज्यादा हो चुकी है।
अंतराष्ट्रीय जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि पिछले तीन दशकों में भारत के अधिकांश हिस्सों में धूप के घंटे कम होते जा रहे हैं। यह अध्ययन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (आईआईटीएम), पुणे और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से जुड़े वैज्ञानिकों के दल द्वारा किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल से जुड़े जलवायु वैज्ञानिकों की एक टीम ने शोध-पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारत का औसत तापमान पिछले एक दशक (2015–2024) में लगभग 0.9°C बढ़ गया है, जो 20 वीं सदी की शुरुआत (1901–1930) की तुलना में है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में वर्ष के सबसे गर्म दिन का तापमान 1950 के दशक से अब तक 1.5 से 2°C तक बढ़ चुका है।
21वीं सदी में, 'जलवायु संकट' मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है, जिससे राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जिससे तापमान में तीव्र वृद्धि हो रही है और वैश्विक स्तर पर सभी कमजोर समुदायों के लिए खतरा बढ़ गया है। भारत में अनियंत्रित गति से बढ़ते जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है कि बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा अभी भी कोयला आधारित थर्मल प्लांटों से आता है। परिवहन क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल की खपत लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों का भारी उपयोग हो रहा है। जिससे तापमान में वृद्धि और वायु प्रदूषण दोनों बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ते शहरों में कंक्रीट का फैलाव बढ़ रहा है दूसरी ओर शहरों में ग्रीन स्पेस, झीलें और जलाशय घटते जा रहे हैं। ऊंची इमारतें, सड़कें और औद्योगिक क्लस्टर, सब मिलकर “हीट आइलैंड प्रभाव” को बढ़ा रहे हैं।
भारत को त्वरित, समन्वित और स्थानीय स्तर पर अनुकूलित जलवायु नीति की आवश्यकता है। जलवायु अनुकूलन (क्लाइमेट एडपटेशन) मजबूत करना और जोखिम वाले जिलों की क्लाइमेट एटलस तैयार कर योजनाओं को उसी आधार पर बजट देना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल निकासी, बाढ़ सुरक्षा, हीट एक्शन प्लान लागू करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नदी संरक्षण और वेटलैंड संरक्षण को मजबूत करना होगा।समाधान केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों, पंचायतों, नगर निकायों, वैज्ञानिक संस्थानों और नागरिकों की संयुक्त भागीदारी से ही संभव है। जलवायु परिवर्तन को कम करने और इसके प्रभावों से निपटने के लिए अभी कदम उठाना अनिवार्य है, क्योंकि आने वाला दशक भारत के लिए निर्णायक है। प्राथमिकता से प्रत्येक राज्य में आधुनिक, तकनीकी आधारित चेतावनी तंत्र विकसित करना और पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है।
(लेखक राज कुमार सिन्हा बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ से जुड़े हुए हैं।)