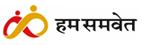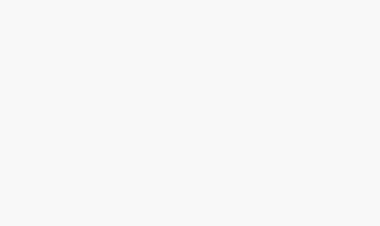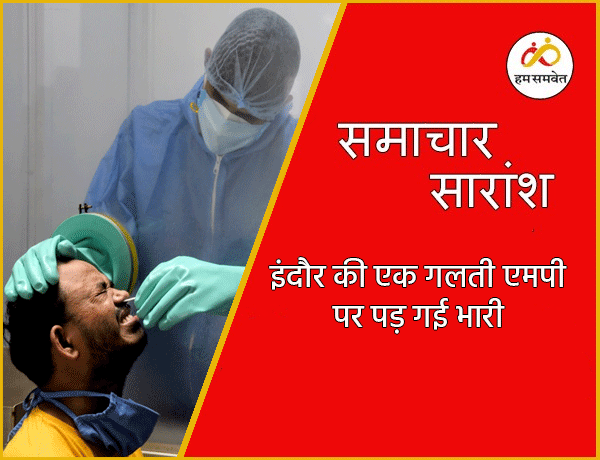भारतीय लोकतंत्र: अतीत में निहित है भविष्य
आज ठीक 100 साल बाद हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां बहुमत नहीं बहुमतवाद का बोलबाला हो रहा है। 35 या 36 प्रतिशत मत लाकर बनी सरकारें पूरी तरह से मनमानी पर उतर आई हैं। अतएव आवश्यकता है बाकी के 65 प्रतिशत को सक्रिय करने की और सत्ता पक्ष के आँख में आँख डालकर राजनीतिक गतिविधियों को समाज के सबसे निचले स्तर से पुनः शुरू करने की।

दर्द की दवा का असर/हवा हो जाए जब,
तब जो दर्द लौट आया है/ उसे नया मान लो,
और उपाय भी उसका / नया खोजो कोई।
भवानीप्रसाद मिश्र
दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों से यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय राजनीति अब ठहरे पानी की मानिंद हो गई है और इसमें सड़ांघ उठने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने चुनाव को और उसके बाद सत्ता पाने तक को ही राजनीति का ध्येय मान लिया है। अतएव हमें कथित वर्तमान राजनीतिक सक्रियता पांच वर्षों में महज पांच-छ: महीने ही दिखाई पड़ती है। बाकी समय आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भारत को एक पूर्णकालिक चुनावी देश में बदल दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के ठीक पहले आठवें वित्त आयोग के गठन की घोषणा, प्रधानमंत्री का संगम स्नान और उसका मीडिया कवरेज और उसके अलावा केंद्रीय बजट में मध्यवर्ग को आयकर में 12 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त किया जाना, बहुत सीधे, सपाट और स्पष्ट संकेत हमें दे रहा है। भारत में व्याप्त वर्तमान परिस्थितियों से बहुत से प्रश्न खड़े हो रहे हैं और यह बात भी उभरकर आ रही है कि भारतीय राजनीतिक परिदृष्य में अब आमूलचूल परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है और इसे लंबे समय तक टाला भी नहीं जा सकता।
भारत के वाम आंदोलन के प्रणेता एम.एन.राय ने कहा था, “यह एक निर्विवाद तथ्य है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं कर सकता। दो चुनावों के बीच की अवधि में लोकतंत्र दृश्य से पूरी तरह से बाहर रहता है। इस अवधि में संसद में बहुमत वाला दल संवैधानिक रुप से अधिनायकवादी शक्तियां ग्रहण कर सकता है। लोकतांत्रिक अनुमोदन से संभव शक्ति के इस दुरूपयोग के विरुद्ध कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। यह सुरक्षा केवल बहुमत दल के नैतिक बोध पर निर्भर करती है।"
इस प्रकार औपचारिक संसदवाद हर परिस्थिति में लोकतंत्र को बचाने और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा में सफल नहीं हो सकता। इस संदर्भ में वे केवल हिटलर को ही अपवाद नहीं मानते हैं। आज भारतीय लोकतंत्र भी इसी तरह की दुविधा में झूल रहा है। राज्य हो या केन्द्र, चुनावों के बीच का काल कमोवेश राजनीतिक और सामाजिक शून्यता का काल बनता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि इन वर्षों में भारत की राजनीतिक चेतना गहरी निंदा की भेंट चढ़ जाती है। जब भी दो चुनावों के बीच जिस किसी ने भी राजनीतिक सक्रियता कायम रखी है, उसके नतीजे बेहद सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं।
इसके उदाहरण हैं अस्सी के दशक में जय प्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जिसने सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया और दूसरा हालिया उदाहरण है राहुल गांधी की कन्या कुमारी से कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर की 136 दिवसीय यात्रा और इसके बाद न्याय यात्रा। इन यात्राओं का भी राजनीतिक लाभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला है।
वस्तुतः चुनाव के तुरंत पहले किसी भी बदलाव को लेकर मतदाता बहुत आशान्वित नहीं हो पाता है। उसे लगता है कि इस जंग लगे उपकरण से काम नहीं चलेगा। राजनीति तो सतत् प्रवाहमय प्रक्रिया है और इसे पूरी तरह से विकेंद्रित करके ही गतिमान एवं सामयिक बनाया जा सकता है।
अतएव यह आवश्यक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजादी के पहले वाले समावेशी चरित्र का पुनः अध्ययन किया जाए। आज की परिस्थितियों और महात्मा गांधी के सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। उसे दौरान में देश में बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, बीमारी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, किसानों और मजदूरों की बेकद्री आदि कमोवेश चरम पर थी। आज 110 साल बाद हालात फिर बिगड़ रहे हैं। बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों के चरम पर है। आजादी के बाद से देश कभी इतना सांप्रदायिक नहीं था जितना आज है। किसानों से सालों साल चुनी हुई सरकारें मिलने तक से इनकार कर देती हैं। 40 (चालीस) दिन से अनशन पर बैठे किसान से बात करने का समय एक महीने बाद का दिया जाता है। वहीं आर्थिक असमानता तो औपनिवेशिक काल की सीमा को भी पार कर चुकी है।
महात्मा गांधी ने सन 1925 में समझाया था, “मैं यहां सिद्ध कर दिखाने की आशा रखता हूँ कि सच्चा स्वराज थोड़े लोगों के द्वारा सत्ता प्राप्त करने से नहीं, बल्कि सब लोगों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करने से हासिल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में स्वराज जनता में इस बात का ज्ञान पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर नियंत्रण और नियमन करने की क्षमता उसमें है।” जबकि आज स्थिति एकदम उल्टी नजर आ रही है। जनता के मन में कमोवेश या बैठा दिया गया है कि वह शासन नहीं बल्कि शासित होने के लिए है। इतना ही नहीं उसे यह भी समझा दिया गया है कि उस पर राज्य/शासन/नियंत्रण/काबू आदि रखने के लिए सिर्फ एक कठोर ही नहीं कमोवेश निष्ठुर नेता की आवश्यकता है और आमुख नेता उस आवश्यकता की पूर्ति अत्यंत अलोकतांत्रिक होकर लोकतंत्र में संसद या विधानसभाओं के जरिए करता है।
कठोरता और निष्ठुरता की आड़ लेकर आज शासन-प्रशासन की सारी असफलताओं को बड़ी सफाई और सफलता से दबाया जा रहा है। यही नहीं गांधी इसे और भी स्पष्ट से समझाते हुए कहते हैं कि, “हमें लंबे समय से यह सोचने की आदत हो गई है कि सत्ता केवल विधानसभा के जरिए ही हाथ में आती है। यह हमारी जड़ता या मोह का परिणाम है। सत्य यह है कि सत्ता जनता के हाथ में होती है और वह कुछ समय के लिए उन लोगों के हाथ में सौंपी जाती है, जिन्हें जनता चुनती है। जनता से अलग पार्लियामेंटों की कोई सत्ता या हस्ती नहीं होती। और पार्लियामेंट की पद्धति तभी लाभकारी हो सकती है, जब उसके सदस्य बहुमत की इच्छा के अनुसार चलने को तैयार हों।”
आज ठीक 100 साल बाद हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां बहुमत नहीं बहुमतवाद का बोलबाला हो रहा है। 35 या 36 प्रतिशत मत लाकर बनी सरकारें पूरी तरह से मनमानी पर उतर आई हैं। अतएव आवश्यकता है बाकी के 65 प्रतिशत को सक्रिय करने की और सत्ता पक्ष से जुड़े समुदाय की आँख में आँख डालकर राजनीतिक गतिविधियों को समाज के सबसे निचले स्तर से पुनः शुरू करने की। गांधी ने भी यही किया था। कुलीनों की कांग्रेस को उन्होंने किसानों और वंचितों की कांग्रेस में परिवर्तित कर दिया और पहली बार महिलाओं को अनेक मोर्चों की सीधी जिम्मेदारी सौंपी थी। शराबबंदी एक राष्ट्रीय मिशन बन गया और भारत की अधिकांश जनता उसके माध्यम से जुड़ती चली गई।
जाहिर तब आजादी प्राप्त करना संघर्ष का केंद्र बिंदु था। आज तो ऐसे तमाम विषय मौजूद हैं जो लोगों को एकजुट कर सकते हैं। हम पाते हैं कि राज्यों ने तो वस्तुतः अपने स्थानीय मुद्दों को जैसे गैरजरूरी समझ लिया है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले बीस वर्षों में किसी भी दल द्वारा कोई भी ऐसा राजनीतिक आंदोलन सामने नहीं आया, जिससे किसी तरह की राज्यस्तरीय हलचल हुई हो। राजनीतिक आंदोलन अब विरोध प्रदर्शन तक सीमित हो गए हैं और दलों के राज्य अध्यक्ष अधिकांश मामलों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने राजनीतिक कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं।
इतना ही नहीं वह किसी व्यापक सामाजिक आंदोलन को भी अपना प्रत्यक्ष समर्थन नहीं देते क्योंकि उनके मन में रहता है कि जब वे सत्ता में आएंगे तो इनसे भी पाला पड़ सकता है। राजनीतिक दल स्वयं किसी सामाजिक हस्तक्षेप में रुचि नहीं दिखाते हैं और तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपना मत प्रकट ही नहीं करते। अपनी इसी बेरुखी के चलते वे राजनीतिक शक्ति भी खो बैठते हैं। आज यही स्थिति सामने आ रही है।
शोचनीय तथ्य यह है कि भाजपा सरकार के द्वारा जारी नई शिक्षा नीति को लेकर विपक्षी दलों की ओर से शायद ही कभी कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी या विमर्श का आयोजन सामने आया हो। ठीक वैसा ही आर्थिक नीतियों को लेकर भी है।
कॉर्पोरेट एकाधिकार के बरस्क बाकी दलों खासकर कांग्रेस की नीति क्या होगी? किसान और कृषि समस्या का हल तीन कानून के रद्द होने या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलवा देने से नहीं निकल सकता। प्रसिद्ध समाजवादी विचारक मधु लिखते हैं, “कांग्रेस के अधिवेशन में सन 1920 तक सामाजिक प्रश्नों पर न कभी विचार हुआ (कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हो गई थी) न उनके ऊपर किसी तरह का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। यह स्थिति गांधी जी के आगमन तक रही। सन 1919 में रौलेट कानून विरोधी आंदोलन को लेकर गांधी जी ने अखिल भारतीय राजनीति के मंच पर अपना कदम रखा। उनके असहयोग के अभिनव विचार और कार्यक्रम ने कांग्रेसजनों तथा साधारण लोगों को आकर्षित किया और गांधी जी का नेतृत्व सन 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन तक सुप्रतिष्ठित हो गया। नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया और मुख्य प्रस्ताव में पहली बार कांग्रेस ने सामाजिक प्रश्नों का उल्लेख किया।”
इसके बाद ही कांग्रेस सामाजिक प्रश्नों को अपने आंदोलन का प्रबल हथियार बनाने लगी थी। बाद के प्रत्येक राष्ट्रीय अधिवेशन भविष्य या आजादी के बाद के भारत के सपने को साकार करने के विभिन्न आयामों और विषयों पर अपना निर्णायक मत रखते चले गए। इन्हीं अधिवेशन में भविष्य का धर्मनिरपेक्ष भारत गढ़ा गया है। वर्तमान समय की राजनीति की एक बड़ी समस्या यह है कि यह पूरी तरह से सिर्फ कार्यकर्ताओं पर निर्भर हो गई है और लोक शिक्षण, प्रशिक्षण और जन भागीदारी का कार्य पूरी तरह से ठप्प सा हो गया है। मुख्य धारा के मीडिया की बेरुखी भी भारत के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो रही है। परंतु राजनीतिक दलों को इसका विकल्प तो तैयार करना ही होगा।
आजादी के पहले भी भारतीय प्रिंट मीडिया का अधिकांश तो अंग्रेज सरकार का भक्त ही था। तब गांधी जी ने अपने प्रकाशनों और कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड आदि के माध्यम से जो वातावरण तैयार किया वह सबके सामने है। प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ की पुस्तक “दि लॉस्ट हीरोज : फुट सोल्जर्स ऑफ़ इंडियन फ्रीडम” में एक अनूठे पत्रकार कर्नाटक के स्व. एच.एस दोरेस्वामी पर बेहद रोचक आलेख है। इसका शीर्षक है “वन न्यूज़ पेपर मेनी नेम्स” । दोरेस्वामी ने 104 वर्ष की उम्र पाई थी। वह बताते हैं, “कलेक्टर ने यह जानकारी नहीं ली कि मैं इतने सारे समाचार पत्रों का पंजीकरण क्यों कर रहा हूँ। मुद्दा यह है कि जब वह एक शीर्षक (टाईटल) पर बंदिश लगा देते थे तो मैं दूसरा (अखबार) शुरू कर देता था। तो जब उन्होंने “पूर्ववाणी” पर रोक लगाई तो मैंने “पौरावीरा” को छापना शुरू कर दिया।” आज फिर इसी जुनून की आवश्यकता है। वैसे कांग्रेस के पास अभी भी नेशनल हेराल्ड मौजूद है। जरूरी है कि आम जनता में लोकप्रिय बनाने के पहले इसे दल अपने सदस्यों के बीच तो ठीक तरह से साझा करें जिससे कि वह अपने दल के राजनीतिक मन्तव्य को समझ सकें।
भारतीय लोकतंत्र के लिए हालात लगातार प्रतिकूल होते जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तक भारत के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के साथ ही साथ तमाम प्रबुद्ध लोगों की प्रतिबद्धता सामाजिक राजनीतिक सरोकारों से थी और वह विपक्षी दलों को काफी नैतिक संबल भी प्रदान कर रहे थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रत्येक प्रबुद्धता के खिलाफ जैसे संग्राम छेड़ दिया है और गैर सरकारी संगठनों की नाक में नकेल डाल दी है। अधिकांश संगठन अब इस नकेल के आदी भी होते जा रहे हैं। अतएव राजनीतिक दलों को अब परिवर्तन की पूरी लड़ाई अकेले ही लड़ना होगी।
वर्तमान परिस्थितियों पर चंद्रकांत देवताले की लंबी कविता “थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चों” की यह पंक्तियां याद आ रही हैं,
ईश्वर होता तो इतनी देर में उसकी देह कोढ़ से
गलने लगती /
सत्य होता तो वह अपनी न्यायाधीश /
की कुर्सी से उतर जलती सलाखें आँखों में खुपस लेता/
सुंदर होता तो वह अपने चेहरे पर तेज़ाब पोत/
अंधे कुएँ में कूद गया होता, लेकिन..... ।।”
जाहिर है अब राजनीतिक दलों को इस “लेकिन” को निश्चितता में बदलना होगा।