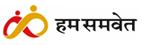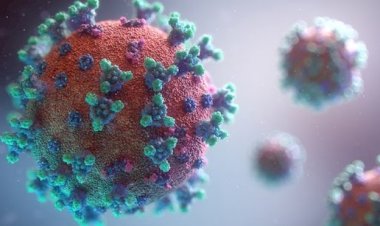कांग्रेस की नई सोच को सलाम
कोई भी सकारात्मक पहल कभी भी असफल नहीं होती, बदलाव को आत्मसात कर पाना प्रत्येक युग में बेहद कठिन रहा है

"कल्पना कीजिए एक ऐसी बहन की जिसे एक भी अक्षर नहीं आता है। ककहरा भी नहीं जानती, फिर भी वह अपने काम में मगन रहती है। जो अपना ना हो, ऐसे घास के तिनके को भी हाथ नहीं लगाती। सपने में भी कोई चोरी नहीं करती। उससे पूछो कि "भागवत" क्या है, तो वह तुम्हारा मुंह ताक ने लगेगी, लेकिन सब पर ऐसा प्रेम भाव रखती है मानो साक्षात जगदंबा हो!"
महात्मा गांधी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जो मानस "लड़की हूँ लड़ सकती हूँ" बनाया है, वह वास्तव में आज के दौर में कमोवेश अविश्वसनीय ही नहीं असंभव भी लगता है। वर्तमान में इस तरह से सोचना भी आश्चर्य का विषय बन गया है। भारतीय प्रेस जगत और कमोवेश संपूर्ण पढ़ा-लिखा तबका आज नैतिकता को राजनीति का पैमाना बनाने के प्रति पूर्णतः उदासीन जान पड़ता है। याद रखिए, कोई भी सकारात्मक पहल कभी भी असफल नहीं होती। बदलाव को आत्मसात कर पाना प्रत्येक युग में बेहद कठिन रहा है। महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद कांग्रेस में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दिलवाना भी कोई आसान कार्य नहीं रहा। गांधी जी ने अक्टूबर 1920 के आखिरी हफ्ते में भारत में रह रहे अंग्रेज के नाम लिखे पत्र में ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण, ब्रिटिश नागरिकों को अत्यधिक वेतन, सेना पर असाधारण खर्च और अत्यधिक कार्यालयीन खर्च को भारत की गरीबी से जोड़ते हुए इसमें सरकार व ब्रिटिश नागरिकों से स्वप्रेरणा से अपने वेतन व खर्चे कम करने का आग्रह किया था। तमाम पत्र इसके विरोध में आए और कुछ पत्र इसके समर्थन में आए। कई पत्र बेहद घृणास्पद थे। एक गुमनाम पत्र में उन्हें, झूठों का राजकुमार, सात वेश्याओं का पुत्र और हजारों अपराधियों का पिता कहा गया। उन्हें तब भी कहा गया कि वे एक बेवकूफ हिंदू हैं जो कि मुसलमानों का साथ देता है। यह भी कहा गया कि यदि वे जर्मन आधिपत्य वाले राष्ट्र में रह रहे होते तो उन्हें कुत्ते की तरह फांसी पर चढ़ा दिया जाता। वर्तमान परिस्थितियां पुनः बेहद डरावना मोड़ लेती जा रहीं हैं। जिस तरह का गालीगलौज आज हमारे आसपास मंडरा रहा है, उससे लगने लगा है कि हम 100 साल पहले जिन विषम परिस्थितियों में थे आज शायद उससे भी कठिन दौर में हैं।
बहरहाल परिवर्तन बहुत आसान नहीं होता। खासकर वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह इसलिए और भी कठिन है क्योंकि राजनीति को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाने की मनस्थिति ही लुप्त होती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने जो बीड़ा उठाया है वह तात्कालिक तौर पर तो शायद उतना महत्वपूर्ण व आकर्षक नहीं जान पड़ता लेकिन कांग्रेस यदि इस पर टिकी रहती है और इसे प्राप्त करने के लिए गहन विमर्श में उतरती है तो यह असंभव भी नहीं है। परंतु यह समझ लेना होगा कि महिला सशक्तिकरण या उनकी राजनीतिक भागीदारी का माध्यम मकर संक्रांति पर उनके साथ तिल गुड़ बांटना कतई नहीं हो सकता। कांग्रेस को तमाम लुभावने खासकर धार्मिक प्रतीकों से छुटकारा पाना होगा और बेहद वैचारिक स्पष्टता से इस लड़ाई को पूरी निष्ठा से लड़ना होगा।
सौ साल पीछे लौटते हैं। सन् 1920 में। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की बात उठाते हैं। कांग्रेस में इसको लेकर बेहद असमंजस था। इसी बीच कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। गांधी जी ने 5 सितंबर को असहयोग को लेकर मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 8 सितंबर को इसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। इसे लेकर वहां कमोवेश हंगामा सा मच गया। उनके इस प्रस्ताव का समर्थन स्व. मोतीलाल नेहरु ने किया था। इसके विरोध में जिन्ना, मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट थे। सभी के भाषण के बाद मतदान हुआ। कुल 1855 प्रतिनिधियों ने गांधीजी के प्रस्ताव के पक्ष में और 873 ने इसके विरोध में मत दिया। यदि आंचलिक विभाजन पर गौर करें तो बम्बई 243 पक्ष में 93 विपक्ष, उत्तरप्रदेश 259 पक्ष 28 विपक्ष, पंजाब ने सबसे तगड़ा समर्थन दिया 254 पक्ष 92 विपक्ष, मद्रास 161 पक्ष 135 विपक्ष। वही मध्य प्रांतों से 30 ने पक्ष में और 33 ने विपक्ष में मत दिया था। संख्या के हिसाब से तो गांधी जीत ही गए थे। लेकिन कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता समझौते की तरफदारी कर रहे थे। अतः यह तय हुआ कि दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होने वाला है उसमें इसे पारित करवाया जाए।
और पढ़ें: बापू का अंतिम उपवास यानी नए भारत के निर्माण के सात दिन
गौरतलब है नागपुर मध्य प्रांत में था। बापू ने अपना अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन के बाद पहले महीने में 19 सभाओं को दूसरे महीने 29 सभाओं को संबोधित किया। अधिकांश सभाएं उन प्रतिनिधियों के समक्ष थीं जिन्हें नागपुर सम्मेलन में शिरकत करना थी। वे ट्रेन से सफर करते थे। 20 दिसंबर को वे नागपुर पहुंचे। वहां तमाम वर्गों को संबोधित किया। 30 दिसंबर को सम्मेलन में अपना असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इसी के माध्यम से भारतीय गणराज्य की स्थापना की पैरवी की। जिन्ना ने यहां भी उनका विरोध किया और कहा कि गांधी के माध्यम से कांग्रेस जिस राह पर जा रही है, वह न तो तार्किक है और ना ही राजनीतिक रूप से ठोस। गौरतलब है इस वार्षिक सम्मेलन में कुल 14582 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इनमें से 1050 मुस्लिम थे और 169 महिलाएं। याद रखिए कांग्रेस की स्थापना के बाद से तब तक कभी भी इतनी महिलाएं वार्षिक सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थीं। महात्मा गांधी का प्रस्ताव कमोवेश सर्वसम्मति से पारित हुआ और परिणाम हमारे सामने हैं। भारत की आजादी।
और पढ़ें: झांसी वालों, झाँसों से बचो
वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस के नवीनतम प्रस्ताव को लेकर उठ रही शंकाएं भी पूरी तरह से जायज हैं। अतएव यह आवश्यक है कि इसे संप्रेषित करने के लिए विस्तृत रणनीति पर काम हो और आंतरिक असहमति को व्यक्त करने का पूरा मौका मिले। कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन व नागपुर वार्षिक अधिवेशन पश्चात बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस से स्वयं को अलग कर लिया था। इससे महात्मा गांधी व उन असंतुष्टों के आपसी रिश्तो में फर्क नहीं पड़ा। हाँ मोहम्मद अली जिन्ना जरुर एक अपवाद रहे। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इसी प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात आजादी के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और यदि भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो उसमें उनकी संख्या असाधारण रूप से बढ़ती गई। कई जगह तो वे संख्या में पुरुषों की बराबरी पर थीं। इतना ही नहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाएं काफी संख्या में ब्रिटिश बलों की गोली से मारी भी गई थीं। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का यह स्वर्णिम युग भी था।
बापू के इस कथन पर गौर करिए, "अहिंसक लड़ाई की खूबसूरती यह है कि इसमें पुरुषों की तरह स्त्रियां भी हिस्सा ले सकतीं हैं। हिंसक लड़ाई में उस तरह हिस्सा लेना स्त्रियों के बस में नहीं है जिस तरह पुरुष ले सकते हैं। भारत में पिछली अहिंसक लड़ाई में स्त्रियों ने पुरुषों से भी अच्छा काम किया है। कारण सीधा-साधा है। अहिंसक लड़ाई अधिक से अधिक कष्ट सहन की अपेक्षा रखती है और स्त्रियों से अधिक शुद्ध और उदात्त कष्ट-सहन और कौन कर सकता है।" इसलिए "लड़की हूँ लड़ सकती हूँ" जैसे अभियान को यदि मूर्त रूप देना है तो यह समझना होगा कि राजनीति परिवर्तन का मार्ग है और सत्ता इसका सहउत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है। आजादी से पहले सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन तमाम गतिविधियां भारतीयों के हिसाब से ही संचालित होतीं थीं। असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ ही साथ, रोजगार, अछूतों के साथ बराबरी का व्यवहार, महिलाओं की हिस्सेदारी, शिक्षा व इस जैसे तमाम मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण बने रहे और भारतीय समाज व इस दौरान सक्रिय तमाम समूह (दक्षिणपंथी समूहों को छोड़कर) दोनों आयामों पर लगातार काम करते रहे।
और पढ़ें: क्या मैं तुम्हारी लहर नहीं हूँ, गंगा जी और जमना जी
आज स्थितियां बेहद अरुचिपूर्ण होती जा रहीं है। भाषा का संयम ही नहीं सामान्य विवेक भी जैसे तमाम राजनीतिज्ञों से पृथक होता जा रहा है। प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर उठे विवाद के बाद असम के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में बदनुमा दाग है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व अन्य कई भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व तमाम केंद्रीय व राज्य के मंत्रियों के आरोप न सिर्फ अलोकतांत्रिक हैं बल्कि भाषा की मर्यादा का भी उल्लंघन हैं। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह पहल बेहद दुस्साहसपूर्ण ही कही जाएगी। ऐसा करना इसलिए भी जरुरी हो गया था क्योंकि अब साधारण या सामान्य साहस से बात नहीं बन पाएगी। यह तय है है कि कांग्रेस के भीतर भी इसे लेकर असहजता तो व्याप्त है। परंतु हमें समझना होगा कि परिवर्तन सत्ता से नहीं बल्कि राजनीति के माध्यम से होता है। कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के कुछ लोकोपयोगी कानून जैसे सूचना का अधिकार, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
भारतीय लोकतंत्र आज रास्ता भटक सा गया है। भटके को पुनः सही रास्ते पर पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि उसे पहले वहां पहुंचना होता है, जहां से वह भटका था। थोड़ा उल्टा चलना पड़ता है। आलेख की शुरुआत में बापू एक अनपढ़ लेकिन बेहद संवेदनशील नारी को प्रतीक बनाकर हमें उसकी ताकत समझाते हैं। लेख के अंत में उनके इस उदाहरण से उसी बात को एकदम नई तरह से समझते हैं। वे कहते हैं, "द्रौपदी बुद्धि का रूपक है और पांच पांडव उसकी वशीभूत पांच इंद्रियां हैं। इंद्रिया वशीभूत हो जाएं यह तो अच्छी बात है। पांच इंद्रियां बुद्धि की वशीभूत हो गईं और इस तरह उनका परिष्कार हुआ, इसी बात को यों कहा जा सकता है कि बुद्धि ने उनका वरण कर लिया। द्रौपदी ने अगाघ बल का परिचय दिया। भीम भी द्रौपदी से डरता था। युधिष्ठिर धर्मराज थे, भी उससे डरते थे।"
सोचिए यदि भीम और युधिष्ठिर डरते थे, तो कौरवों की क्या स्थिति होगी ? यदि आज लड़कियां लड़ने लगें तो आधुनिक कौरवों का क्या होगा ?
(गांधीवादी विचारक चिन्मय मिश्रा के यह स्वतंत्र विचार हैं)