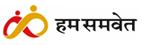किसान आंदोलन: धरती माता के यहां रिश्वत नहीं चल सकती
किसान आंदोलन ने संघर्ष के नौ माह पूरे कर लिए। इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि इससे क्या हासिल किया और क्या खोया

‘‘किसान वास्तविक धन का उत्पादक है, क्योंकि वह मिट्टी को गेहूँ, चावल, कपास के रूप में परिणत करता है। दो घंटे रात रहते खेतों में पहुंचता है। जेठ की तपती दुपहरी हो या माघ-पूस के सबेरे की हड्डी छेदने वाली सर्दी, वह हल जोतता है, ढेले फोड़ता है, उसका बदन पसीने से तरबतर हो जाता है, उसके एक हाथ में सात-सात घट्टे पड़ जाते हैं फिर भी वह मशक्कत करता रहता है। क्योंकि उसे मालूम है कि धरती माता के यहां रिश्वत नहीं चल सकती। वह स्तुति प्रार्थना के द्वारा अपने ह्दय को नहीं खोल सकती।’’
राहुल सांकृत्यापन
किसान आंदोलन ने संघर्ष के नौ माह पूरे कर लिए। इसलिए यह सवाल उठना लाज़मी है कि इससे क्या हासिल किया और क्या खोया? किसान आन्दोलन खोने और पाने से आगे की स्थिति पर पहुंच गया है। यह भारत को पुनः लोकतंत्र की ओर मोड़नेवाला उपक्रम बन गया है। इस आंदोलन ने मूलतः दो बातों को पुर्नस्थापित किया है। पहली यह कि भारतीय संविधान का पूर्ण क्षरण नहीं हुआ है और दूसरी अधिनायकवादी लोकतंत्र को जवाब दिया जा सकता है, उसका विकल्प अभी भी मौजूद है। इस आंदोलन के प्रति सरकार/सरकारों की बेरुखी भी यह दर्शा रही है कि शासक वर्ग किसानों की सच्ची निर्मलता से आँख मिला पाने में असमर्थ है। साथ ही सरकार को अपने को सही सिद्ध करवाना कमोवेश असंभव होता जा रहा है। इसलिए आम जनता का ध्यान लगातार बांटा जा रहा है।
नवीनतम उदाहरण है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक पूरे देश में समारोहित किया जाएगा। यह ऐसे समय हो रहा है, जबकि कोरोना महामारी अभी थमी नहीं हैं, इससे तड़प-तड़पकर हुई मौतों का मंजर अभी आँखों से ओझल नहीं हुआ है, बेराजगारी अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था हांफ रही है, अपराध दिन दूने, रात चौगुने हो रहे हैं, मँहगाई रोज नए रिकार्ड बना रही है, सांप्रदायिकता नये कलेवर के साथ सर्वव्यापी होने को तैयार है 2 अक्टूबर को गाँधी जयंती भी है, आदि - आदि।
किसान आंदोलन ने पिछले नौ महीनों में यह तो बतला दिया कि भारत में एक बार पुनः संघर्ष की राह पर चलने की ललक पैदा हुई है। साथ ही सामूहिकता का असाधारण संकल्प भी सामने आया है। 500 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मृत्यु के बावजूद किसान आंदोलन का अहिंसक बना रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाल ही में करनाल में हुई महापंचायत, प्रदर्शन व सचिवालय का घेराव इसकी गवाही दे रहे हैं। आधुनिक समाज का बड़ा वर्ग सत्य और अहिंसा से बचना चाह रहा है, यह आंदोलन उनके लिए मिसाल है। इस आंदोलन ने सत्ता के दंभ को भी बेनकाब किया है और स्वयं को लगातार विस्तारित किया है। किसान आंदोलन ने भारतीय मीडिया को भी आईना दिखाया है। उन्होंने मीडिया को भी यह समझा दिया है कि उनके बिना भी आंदोलन किया जा सकता है।
यह तय है कि भारत के तमाम लोग कृषि क्षेत्र व किसान की समस्याओं के प्रति अनभिज्ञ हैं और इस तरह के आंदोलन को कमोवेश गैरजरुरी मानते हैं। इस अलगाव के पीछे बहुत से कारण हैं और सबसे बड़ा कारण यह है कि संपन्न वर्ग किसान व किसानी को समझना ही नहीं चाहता। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, ‘‘महीनों की भूख से अधमरे उसके बच्चे चाहभरी निगाह से उस राशि (अनाज) को देखते हैं। वे समझते हैं दुख की अंधेरी रात कटने वाली है और सुख का सबेरा आने वाला है। उनको क्या मालूम कि वह उनके लिए नहीं है। इसके खाने के अधिकारी सबसे पहले वे स्त्री-पुरुष हैं, जिनके हांथों में एक भी घट्टा नहीं है, जिनके हाथ गुलाब जैसे लाल और मक्खन जैसे कोमल हैं, जिनकी जेठ की दुपहरिया खस की टट्टियों (अब एयर कंडीशनर), बिजली के पंखों या शिमला और नैनीताल में बीतती है।’’ दशकों बाद भी आज वहीं स्थिति है। अधिकांश किसान उन 80 करोड़ भारतीयों में आते हैं जो सरकार द्वारा दी जा रही 15 किलो राशन की कथित सौगात को प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले झोले में अपने घर ले जाकर जैसे तैसे अपना पेट भर रहे हैं। पोषण तो दूर की कौड़ी है।
वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी इस अवसर पर वैसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी उनसे अपेक्षा थी। दुखद यह है कि किसान आंदोलन तीन कानूनों और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तक सिमटा सा दिख रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि मूल्य बढ़ा देने आदि से भी कृषि लंबे समय तक बच नहीं पाएगी।
आंदोलन की अवधि का उपयोग इस तलाश में होना था कि किस तरह से सामान्य किसान खेती कर पाए। वर्तमान कृषि का यह औद्योगिक स्वरूप किसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। कितना भी परिश्रम वर्तमान कृषि प्रणाली के अन्तर्गत कर लिया जाए अंततः वह अस्थायी ही सिद्ध होगा। जमीन से यदि वर्ष में 3-4 फसलें ली जाएंगी तो उसमें कितने दिन तक उर्वश शक्ति बनी रहेगी? क्या सिंचाई होने से कृषि संकट समाप्त हो जाएगा? रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक कृषि को स्थायित्व प्रदान कर पाएंगे? बिक्री की आसानी हो जाने से क्या कृषि का उद्धार संभव है? क्या हाईब्रिड व जीएम फसलें खेती - किसानी को बचा पाएंगी? क्या नकदी फसलें उगा लेने से किसान संकट मुक्त हो जाएंगे? ऐसे और भी तमाम प्रश्न कृषि के सामने हैं। कृषि और पर्यावरण के आपसी संबंधों पर विचार करना होगा। कृषि में बढ़ती ऋणगस्तता भी चिंता का विषय है। कृषि का घटता रकबा भी विचारणीय प्रश्न है।
उपरोक्त तमाम प्रश्नों या जिज्ञासा पर पिछले नौ महीनों में गंभीरता से विचार होना चाहिए था। किसानों के सामने भी सुनहरा मौका था, जबकि वे अपने बारे में विस्तार से विचार कर सकते थे। ऐसा ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को करना चाहिए था। अगर अब तक नहीं किया है तो, अभी भी देरी नहीं हुई है। कृषि की जटिलताओं पर बहुत गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। इतने दिनों में किसी विकल्प पर बात तो शुरु होना चाहिए थी। किसान तो आंदोलन कर ही रहे हैं। परंतु अधिकांश विपक्ष प्रतिक्रिया देने में ही है। किसानों के बारे में सभी को सम्मिलित रूप से विचार करना होगा।
कृषि कानूनों की वापसी और फसलों का उचित मूल्य आज की अनिवार्यता है। परंतु यह तो केवल आरंभ है। कृषि की वास्तविक समस्या उसकी आधुनिक उत्पादन पद्धति है और उसमें सुधार नहीं आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है। अतएव राजनीतिक दलों और कृषि विशेषज्ञों का यह कर्तव्य बनता है कि वे कृषि पर बरप रहे संकटों पर गंभीरता से विचार करें। वे प्रतिक्रिया से क्रिया पर लौटें। अब लगने लगा है कि राजनीतिक दलों में कृषि और कृषक को लेकर धैर्य ही नहीं समझ भी कम होती जा रही है। राजनीति में चुनाव जब भी मुख्य मुद्दा बन जाता है, तब राजनीति अर्थात सामाजिक सरोकर जिसका पर्यायवाची है, कहीं पीछे छूट जाती है।
आज से करीब 80 बरस पहले राहुल सांकृत्यायन ने एक निबंध लिखा था, ‘‘तुम्हारी जोकों की क्षय’’। यह आज के संदर्भ में बेहद समकालीन लगता है और दूसरी ओर यह भी समझाता है कि आजादी के बाद तस्वीर ज्यादा नहीं बदली बल्कि पिछले कुछ बरसों में यह बेहद डरावनी हो गई है। ’’जोंके ? जो अपनी परवरिश के लिए धरती पर मेहनत का सहारा नहीं लेतीं। वे दूसरों के अर्जित खून पर गुजर करती हैं। मानुषी जोंके पाशविक जोकों से ज्यादा भयंकर होती हैं।’’ बाकी के लेख में वे मानुषी जोंकों की उत्पत्ति, उनके विकास व उसके द्वारा किए जा रहे विध्वंस को समझाते हैं और यह आलेख हिटलर पर आकर पूर्ण होता है। गौरतलब है भारत ही नहीं दुनियाभर के किसान बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अब तो गर्व से बताया जा रहा है कि अमुक धनपति के पास ढ़ाई लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है।
और वहीं भारत में जो किसान नौ महीनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, रोज अपमानित हो रहे हैं, जिन्हें वही अन्न खाते हुए गरिआया जाता है, जो उन्होंने अपने हाथ में घट्टे बनाकर उपजाया है। ऐसे घट्टे जिनकी वजह से हाथ में अब पानी भी नहीं ठहर पाता, इन उतार चढ़ावों से बह जाता है, और गुलाब के फूल के रंग की मक्खनी हथेलियां अठखेलियां करतीं रहतीं हैं। भारत में किसानों के पास औसतन 3 एकड़ से कम जमीन है और उस पर औद्योगिक कृषि का थोपा जाना सबसे बड़ा अन्याय है। रोज नई खाद, नए बीज, नए ट्रेक्टर के विज्ञापन बता रहे हैं कि कैसे जमीन को दांव पर लगातार और निश्चित तौर पर हारकर उसे जुए में गवां देना बजाए अपराध की श्रेणी में आने के विकास के नए पैमाने और मायने बनते जा रहे हैं।
लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कुछ भी नतीजा सामने नहीं आया। लाखों किसान करनाल में धरना दिए बैठे है। एक एसडीएम तक को बर्खास्त तो क्या निलंबित नहीं करवा पा रहे हैं। यह किसानों की नहीं लोकतंत्र की हार है। दिल्ली में नौ महीनों से बैठे किसानों की सुनवाई न होना लोकतंत्र की हार के साथ ही पूरे विपक्ष की भी हार है। कछुआ केवल कहानियों में ही जीतता है। असल जिंदगी में कछुए व खरगोश की दौड़ होती ही नहीं है। परंतु लोकतंत्र न तो कछुआ है और न खरगोश। अपशब्द बोलने वाले अधिकारी को सजा न दे पाना राजनीतिक शासन तंत्र की बेचारगी का प्रतीक है। यह घटना हमें बता रही है कि अफसरशाही पूरी व्यवस्था पर हावी हो चुकी है और राजनीति व राजनीतिज्ञ कठपुतलियों की तरह पीछे से आ रहे आदेशों को दोहरा रहे हैं। व्यवस्था अंततः नागरिकों की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है ना कि उन्हें दंडित करने के लिए।
और पढ़ें: अपने अपने तालिबान और अफगानिस्तान
ऑलिवर गोल्ड स्मिथ कहते हैं, ‘‘वो देश बदहाल होता है जहां दौलत इकट्ठा होने लगती है और इंसान का पतन होने लगता है।’’ करोड़ों किसान दौलत का विकेन्द्रीयकरण करते हैं। वे अपने पास कुछ भी जमा रख ही नहीं पाते। उनके द्वारा अर्जित धन हमेशा प्रचलन में रहता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में आता - जाता रहता है। इसलिए यदि इस विश्व को बचना है तो उसे छोटी जोत की खेती को बचाना होगा। अडाणी - अंबानी महज प्रतीक हैं। पूरी दुनिया में खासकर विकसित देशों में नया नारा है ‘‘फूड इज गोल्ड’’ यानी खाद्यान्न सोना है। तो सोचिए समृद्ध समाज यह सोना छोटे, मझौले व गरीब किसान को की हतेली में क्यों डालेगा । वो तो इसे रोकेगा ही। भारत सहित दुनियाभर की सरकारें यहीं कर रहीं हैं।
और पढ़ें: अफ़गानिस्तान: मर्ज से पहले मरीज को पहचानिए
भारत के किसान के लिए खुले में बैठना या सोना कोई अंजान स्थिति नहीं है। वह साल के आधे दिन ऐसे ही रहता है। वह जितने दिन खुले में रहेगा, लोकतंत्र उतना ही झुर्रीदार होता जाएगा। केंद्र सरकार से अपेक्षा रखना स्वयं को धोखे में रखना है। विपक्षी दलों के पास मौका है खुद को, भारत के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का। एक समानांतर राजनीतिक आंदोलन आज की अनिवार्यता है जो कि पूरी तरह किसानों को भूमिहीनों को, खेत मजदूरों को समर्पित हो। संभव हो तो गांधी के भारत लौटने के बाद के शुरुआती सालों की राजनीति और उनके हस्तक्षेप को समझें। हल उसी में छिपा है। क्योंकि सत्य तो हर काल में सत्य ही होता है।
और पढ़ें: आंदोलन कभी हारते नहीं
भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति पर फुकुओका का की पुस्तक एक तिनके से क्रांति (वन स्ट्रा रिवोल्युशन) की ये पंक्तियां याद आती हैं। वे कहते हैं, ‘‘इंसान अपनी छेड़छाड़ से कुछ गलत कर बैठते हैं और उस नुकसान को सुधारते नहीं और जब तमाम दुष्प्रभाव इकट्ठे होने लगते हैं तो उन्हें सुधारने पर पिल पड़ते हैं। और जब सुधार संबंधी काम ठीक जान पड़ते हैं तो वे इसे बेहतरीन उपलब्धि मान बैठते हैं। लोग ऐसा बार - बार करते हैं। यह कुछ ऐसा है कि कोई बेवकूफ अपने ही घर की छत पर उछलकूद मचाए और छत के सारे कबेलू तोड़ डाले। बरसात में जब छत टपकने लगे तो उसे खपरेल की मरम्मत करे। अंततः इस बात की खुशी मनाए कि उसने कैसा अद्भुत समाधान ढूंढा है।
क्या हम भी यही नहीं कर रहे हैं ?
(गांधीवादी विचारक चिन्मय मिश्रा के यह स्वतंत्र विचार हैं)