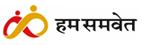संविधान में किसके लिए है मूल संरचना का कवच
Keshavananda Bharati case: वकील एन.ए पालखीवाला ने बहस के दौरान कहा कि लिखित संविधान बनाया ही इसलिए जाता है कि मनुष्य अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता। वह अपनी स्वतंत्रता को बचाकर रखना चाहता है और इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को असीमित शक्ति नहीं देता। इन्हीं मायने में मौलिक अधिकार वे तत्व हैं, जिन्हें संविधान के संशोधनों से बदला नहीं जा सकता। पालखीवाला ने तो एक प्रश्न के जवाब में यहां तक कहा कि उन्हें चुने हुए प्रतिनिधियों से राजतंत्र कायम किए जाने का भी खतरा है।

केरल के एडनीर मठ के महंत, केशवानंद भारती श्रीपादगलवारु, जिन्हें शंकराचार्य भी कहा जाता था, के निधन ने उस मुकदमे की याद ताजा कर दी है जिसका भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में विशेष महत्व है। हालांकि केशवानंद भारती जिन अधिकारों के लिए यह मुकदमा लड़ रहे थे, वह अधिकार एक पक्षकार के रूप में उन्हें हासिल नहीं हुए। लेकिन देश के एक नागरिक के रूप में उन्होंने देश को वह दिला दिया जो इससे पहले स्पष्ट रूप से मिला नहीं था। वे चाहते थे कि संविधान के जिन संशोधनों के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, उन्हें असंवैधानिक बताते हुए निरस्त किया जाए। इसीलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 13, 25, 26, 27 और 29 का हवाला देते हुए धार्मिक और अल्पसंखयक यानी चर्च की संपत्ति के प्रबंधन अधिकारों का भी हवाला दिया था। इस आधार पर उन्होंने अनुच्छेद 368 में दिए गए संशोधन के असीमित अधिकारों को चुनौती दी थी। उन्होंने 24 वें, 25 वें और 29 वें संविधान संशोधन को और नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर बताने वाले अनुच्छेद 31C को भी चुनौती दी थी।
यह ऐसा मुकदमा था जिसे हार कर भी पक्षकार केशवानंद भारती जीत गए और इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार जिसे जीतकर भी हार गई। हालांकि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम.सीकरी के नेतृत्व में 13 सदस्यीय पीठ ने यह पूरी कोशिश की कि इस फैसले में एक प्रकार का समझौता दिलाने वाला समन्वयकारी फार्मूला निकल आए। फार्मूला इस बात पर कि देश का सामाजिक आर्थिक विकास भी हो और लोगों के मौलिक अधिकार भी सुरक्षित रहें। संविधान पीठ के एक जज ने पक्षकार से कहा भी कि आप संपत्ति के मौलिक अधिकार को कुरबान कर दीजिए और बाकी अधिकार सुरक्षित ले लीजिए। कोशिश यह भी थी कि भूमि सुधार कानूनों को संरक्षित करने वाले संविधान संशोधनों से छेड़छाड़ न हो लेकिन बाकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता भी बची रहे। एक प्रकार से यह फैसला संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच और न्यायपालिका और विधायिका के मध्य भी एक प्रकार का समन्वय बिठाने का प्रयास था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि वह समन्वय बच नहीं पाया। न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव बढ़ा और जिसका परिणाम था आपातकाल आया और उसके बाद मूल संरचना के सिद्धांत की चर्चा तो बहुत चली लेकिन उस पर खतरा निरंतर बना रहा। आज अगर संविधान और उसमें वर्णित मौलिक अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है तो, उसकी वजह यह नहीं है कि केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित संविधान की मूल संरचना (जिसमें मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत प्रमुख है) किसी नई संवैधानिक पीठ द्वारा खारिज कर दी गई है। बल्कि हकीकत यह है कि देश की न्यायपालिका ने उस सिद्धांत को नागरिकों की हिफ़ाजत की बजाय अपनी हिफ़ाजत के लिए पहन लिया है।
अगर यह मुकदमा अपने जटिल और बिखरे हुए फैसलों के लिए जाना जाता है तो यह मुकदमा देश के तमाम नामी वकीलों की विद्वता और मेहनत से तैयार की गई उनकी दलीलों के लिए भी मशहूर है। इसमें अगर एक ओर अटार्नी जनरल निरेन डे और सोलिसिटर जनरल एल.एन सिन्हा, राजस्थान के एडवोकेट जनरल एल.एम सिंघवी और महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल एच. एम सीरवई थे तो दूसरी ओर से जेबी दादाचानजी, एन.ए पालखीवाला , सीके दफ्तरी, एमसी छागला, सोली सोराबजी और अनिल धवन शामिल थे। इतने नामी वकीलों के बावजूद इस मामले में जिन दो दिग्गजों की बहस मशहूर हुई वह थी, वो थे पालखीवाला और एच. एम सीरवई। वे दोनों मित्र थे और इस मामले में बहस के बाद उनके संबंध ऐसे बिगड़े कि वर्षों तक बात नहीं हुई।
रोचक बात यह है कि एच. एम सीरवई जिन्होंने संभवतः संविधान पर भारत में सबसे अच्छे खंड रचे हैं वे यह कह रहे थे कि मौलिक अधिकार सार्वदेशिक अधिकार नहीं हैं। वे महज सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं और वे संविधान की रचना से पहले भारत के लोगों को प्राप्त नहीं थे। जबकि पालखीवाला कह रहे थे कि मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार चार्टर से निकले अधिकार हैं और वे मैग्ना कार्टा की तरह आधुनिक विश्व के लिए अनिवार्य और मौलिक दस्तावेज हैं। उससे भी रोचक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए पालखीवाला 14, 15 और 16 फरवरी 1955 को टाइम्स आफ इंडिया में `फंडामेंटल राइट्सः बेसिक इश्यू’ शीर्षक से प्रकाशित एच.एम सीरवई के लेखों का उल्लेख कर रहे थे और यह आलेख उन्हें अनिल धवन ने उपलब्ध करवाए थे।
इस बहस में अगर सीरवई कह रहे थे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ भी स्थिर नहीं रखा है और जो भी किसी समय मूल संरचना के रूप में देखा गया है उसे बदला जा सकता है। उनका कहना था कि चुने हुए प्रतिनिधियों का काम कानून बनाना है और उन्हें संविधान में संशोधन का अधिकार भी संविधान में ही दिया गया है। लेकिन पालखीवाला ने साफ कहा कि लिखित संविधान बनाया ही इसलिए जाता है कि मनुष्य अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता। वह अपनी स्वतंत्रता को बचाकर रखना चाहता है और इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को असीमित शक्ति नहीं देता। इन्हीं मायने में मौलिक अधिकार वे तत्व हैं, जिन्हें संविधान के संशोधनों से बदला नहीं जा सकता। पालखीवाला ने तो एक प्रश्न के जवाब में यहां तक कहा कि उन्हें चुने हुए प्रतिनिधियों से राजतंत्र कायम किए जाने का भी खतरा है।
इस मामले में अनुच्छेद 31C पर भी विस्तार से चर्चा हुई और उस पर पालखीवाला ने बहुत तेज हमला बोला। उनके हमले का ही असर था कि वह अनुच्छेद पूरी तरह से तो नहीं समाप्त किया गया लेकिन अदालत ने उस हिस्से को खारिज कर दिया जिसके तहत इस अनुच्छेद की नीतियों को लागू करने के लिए बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अनुच्छेद यह कहता है कि अगर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे मौलिक अधिकारों से टकराव के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। पालखीवाला की सबसे ज्यादा आपत्ति इसी बात पर थी कि संविधान में नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं होते हैं और न ही उन्हें किसी अदालत में लागू करवाया जा सकता है फिर उन्हें वरीयता क्यों दी जा रही है। उन्होंने ऐसे सात आधार बताए हैं जो 31C द्वारा संविधान को नष्ट करने का मौका देते हैं।
पहला आधार यह है कि यह संशोधन संविधान की सर्वोच्चता को खारिज करता है और संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। यह मानवाधिकार के बारे में संसद ही नहीं राज्य की विधानसभाओं को मनमाना हक देता है।
दूसरा आधार यह है कि यह संशोधन मौलिक अधिकारों को नीति निदेशक तत्वों के अधीन लाता है।
तीसरा आधार यह है कि इस प्रावधान के तहत मौलिक अधिकारों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को खत्म करने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए तो 31C के तहत उसे साधारण बहुमत से रद्द किया जा सकता है।
चौथा आधार यह है कि अनुच्छेद 31C संपत्ति, जोकि सभी अधिकारों के मूल में है, उसे ही रद्द कर देता है। संपत्ति के अधिकार ही नहीं 31 C के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरे अन्य छह अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा सकता है।
उनका पांचवा आधार नागरिकों को मुकदमा करने के अधिकार से वंचित करना और
छठा आधार राज्य विधानसभाओं को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार देना और
सातवां अल्पसंख्यकों के अधिकार को हड़प लेना है।
निश्चित तौर पर हमारा संविधान जिन तीन उद्देश्यों को लेकर बना है उनमें देश की एकता अखंडता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति मुख्य हैं। इन तीनों उद्देश्यों का संतुलन कायम करना हमारे संविधान की अनिवार्य संरचना है। ग्रैनविल आस्टिन ने केशवानंद भारती मामले पर अपनी व्याख्या करते हुए लिखा था कि इस फैसले ने उस अनिवार्य संरचना को फिर से बहाल करने की कोशिश की थी। आज उस फैसले की रोशनी में यह बात ध्यान देने की है कि अगर सत्तर के दशक में सामाजिक क्रांति (भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स का छीना जाना) के उद्देश्य को लेकर तमाम कानून बनाए जा रहे थे और उन्हें नीति निदेशक तत्वों के आधार पर सही ठहराया जा रहा था तो आज एकता और अखंडता के नाम पर ऐसे तमाम कानून बनाए जा रहे हैं जो मौलिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं।
अगर मौलिक अधिकारों को, समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर संपत्ति के अधिकार छीने जाने का खतरा है, तो देश की एकता और अखंडता और राष्ट्रद्रोह के नाम पर बनने वाले तमाम कठोर कानूनों से भी कम खतरा नहीं है। इसलिए आज जब संपत्ति के तमाम अधिकार पूंजीवादी सोच के तहत नया विस्तार पा रहे हैं, तब आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर और राष्ट्र निर्माण के बहाने नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बढ़ गया है। ऊपर से दिक्कत यह है कि केशवानंद भारती मुकदमे के फैसले के बहाने हमारी न्यायपालिका ने आरंभ में इस देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का जो कवच और कुंडल पहनाया था वह उससे छिन गया लगता है। लगता है कि उसे न्यायपालिका ने अपनी स्वायत्तता के रूप में धारण कर लिया है और वह उसे नागरिकों की रक्षा में उपयोग नहीं होने देना चाहती। न्यायपालिका के हाल के फ़ैसलों से सवाल उठे हैं कि उसकी चिंताओं में नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, गरीब मजदूर आदिवासियों के अधिकार, स्त्री अधिकार क्यों नहीं दिख रहे हैं। अपने कालेजियम और जजों की सेवा शर्तों की चिंता उसके हाल के तमाम फैसलों पर क्यों हावी लगती है।
केशवानंद भारती मामले की नज़ीर आज भी हमारी न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ी नज़ीर है। अदालतें अपने फैसलों में उसका उल्लेख करती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट, एडीएम जबलपुर मामले में अपने नज़रिए के लिए खेद भी प्रकट कर चुकी है और केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना का सिद्धांत देने वाले न्यायमूर्ति एचआर खन्ना के प्रति (एडीएम जबलपुर मामले में) असहमति जताने के लिए आदर भी जता चुकी है। लेकिन नागरिक अधिकारों के लिए न्यायालय में वह भावना नहीं है जो उस मामले से निकलती है। इसलिए केशवानंद भारती मामले की सच्ची भावना तभी बचेगी जब उसे जनता स्वयं समझे और धारण करे।
कहा गया है, “आजादी हमारे स्त्री और पुरुषों के हृदय में बसती है। जब यह वहां मर जाती है तो कोई संविधान, कोई कानून, कोई अदालत उसे बचा नहीं सकते। कोई संविधान, कोई कानून और कोई अदालत उसकी ज्यादा मदद भी नहीं कर सकती।’’
केशवानंद भारती के फैसले में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पालखीवाला ने फैसले के एक साल बाद 1974 में `अवर कांस्टीट्यूशन डिफेस्ड एंड डिफाइल्ड’ जैसी पुस्तक लिखी और उसमें साफ तौर पर कहा कि देश में अराजकता बढ़ रही है और संवैधानिक नैतिकता पर खतरा मंडरा रहा है। नतीजतन तानाशाही आ सकती है। आज उनकी चिंताओं को 2020 के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उन्होंने उस समय की आर्थिक स्थिति को लेकर ही अराजकता और तानाशाही का खतरा प्रकट किया था। 1973-74 में महंगाई बढ़ रही थी और बेरोजगारी चरम पर थी। वही स्थिति आज भी देखी जा सकती है। जब देश की जीडीपी अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। बेरोजगारी अपने इतिहास के सबसे उच्च स्तर पर है और नागरिक अधिकारों की चेतना घायल है। नागरिक अधिकारों की बहस पूरे देश के परिदृश्य से ग़ायब है।
इन्हीं संदर्भों में केशवानंद भारती के फैसले को भावी संविधान का आधार बताते हुए प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने चेतावनी दी थी कि अभाव की अर्थव्यवस्था में मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों को एक साथ नहीं लागू किया जा सकता। उसी संदर्भ में बढ़ते तानाशाही के खतरे को भांपते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, “अगर लोग अपनी आजादी का इस तरह से उपभोग करते हैं कि वे उसे समर्पित करते हैं तो क्या वे गुलामों से कम हैं? अगर लोग जनमत संग्रह से ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो उनके ऊपर तानाशाही कायम कर सके तो क्या वे इस वजह से स्वतंत्र रह सकते हैं कि इस तानाशाही को उन्होंने स्वयं चुना है? क्या उस शासक द्वारा जो बाध्यकारी आदेश दिए जाते हैं उन्हें इसलिए वैधानिक माना जाए क्योंकि वे उनके मतों के ही परिणाम हैं? ’’