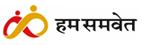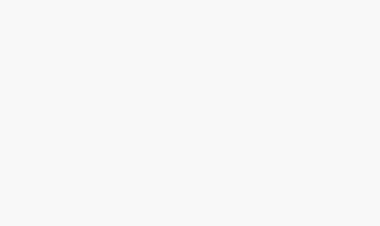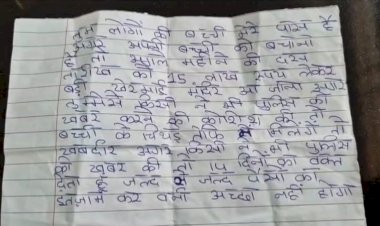आदिवासी हितों का पूरक है वन अधिकार कानून और वन संरक्षण अधिनियम
एक ओर वन अधिकार कानून वनवासियों को पक्का मकान का अधिकार देता है, वहीं वन संरक्षण अधिनियम वन क्षेत्र में इस प्रकार के स्थायी निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करे, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आवासीय मकानों के निर्माण की अनुमति देने का दायरा, तरीका और प्रक्रिया क्या होगी, और यह सब वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुरूप किस प्रकार किया जाएगा।
जहां एक ओर वन अधिकार कानून वनवासियों को ‘पक्का मकान’ का अधिकार देता है, वहीं वन संरक्षण अधिनियम वन क्षेत्र में इस प्रकार के स्थायी निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। न्यायालय ने यह राय दी कि वन (संरक्षण) अधिनियम को इस तरह नहीं समझा जाना चाहिए कि वह वनवासियों के लिए पक्का मकान बनाने पर रोक लगाता है। इस संबंध में न्यायालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को विस्तृत विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने यह मामला सुना। न्यायालय ने कहा कि यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दो प्रमुख कानूनों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, एक ओर वन अधिकार कानून के तहत वनवासियों को न्यूनतम मूलभूत आवास का अधिकार देना है, और दूसरी ओर वन संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य तथा नागरिकों का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय वन संसाधनों की रक्षा करें।
दोनों कानूनों के बीच मतभेद को रेखांकित करते हुए न्यायालय ने कहा कि “जहां वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4 वनवासियों के कुछ अधिकारों को मान्यता और स्वामित्व प्रदान करती है, वहीं धारा 3 यह निर्धारित करती है कि वे अधिकार क्या हैं। धारा 3(2) के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह वनवासियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकती है, भले ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में इसका अलग प्रावधान हो। लेकिन यह छूट केवल उन्हीं गतिविधियों पर लागू होती है जो धारा 3(2) में विशेष रूप से उल्लिखित हैं और इन गतिविधियों में पक्का मकान निर्माण शामिल नहीं है।”
न्यायालय ने प्राथमिक दृष्टि से यह माना कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को इस तरह नहीं समझा जाना चाहिए कि वह कुछ गतिविधियों (जैसे आवास निर्माण) को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है, बल्कि इसका उद्देश्य वन भूमि पर गैर-वन उपयोग को नियमित और निगरानी में रखना है। न्यायालय ने कहा कि "हमारे मत में, यह अधिनियम ऐसा कानून नहीं है जो किसी कार्य को निषिद्ध करता हो, बल्कि यह एक नियामक व्यवस्था है जो वन क्षेत्र में गैर-वन गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के मूल्य को स्थापित करती है और यह हमारे वन संसाधनों के सुरक्षित और सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है।”
अतः, न्यायालय ने यह कहा कि दोनों अधिनियमों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि “इन कानूनों को इस प्रकार लागू किया जा सके कि वे एक-दूसरे का पूरक और सहयोगी बनें, जिससे वनवासियों को लाभ मिले, क्योंकि वे वन से गहराई से जुड़े हैं और साथ ही वन में गैर-वन गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके।” इसी के अनुसार, न्यायालय ने निर्देश दिया कि "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय विस्तृत विचार-विमर्श करें और एक हलफनामा दाखिल करें, जिसमें यह बताया जाए कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्र में आवासीय मकानों के निर्माण को सक्षम करने का दायरा, तरीका और प्रक्रिया क्या होगी, और यह सब वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुरूप कैसे किया जाएगा।”
वन अधिकार कानून आदिवासियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को उनके परंपरागत वन-भूमि पर अधिकार देता है। यह उन्हें रहन-सहन, खेती, और छोटे निर्माण जैसे अधिकारों की कानूनी मान्यता प्रदान करता है। जिसका उद्देश्य है कि वनवासियों को सम्मानजनक जीवन और बुनियादी सुविधाएं मिलें जैसे आवास, पानी, बिजली, शिक्षा, आदि। यह कानून वनवासियों को वन संरक्षण में भागीदारी के लिए भी सशक्त बनाता है, ताकि वे वन को केवल उपयोगकर्ता नहीं बल्कि संरक्षक बनें।
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का कानून वन भूमि के गैर-वन उपयोग पर नियंत्रण रखता है। इसका उद्देश्य है कि वनों की अंधाधुंध कटाई और अतिक्रमण रोका जा सके। यह अधिनियम किसी भी विकास कार्य (जैसे सड़क, बांध, उद्योग आदि) के लिए वन भूमि परिवर्तन पर केंद्र सरकार की अनुमति को अनिवार्य बनाता है। जब दोनों कानून को संतुलित रूप से लागू किया जाए, तो यह सुनिश्चित होता है कि आदिवासी सम्मानजनक आवास और जीवन पा सकें और वन संरक्षित व नियंत्रित रहें।
सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि वनवासी समुदायों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके और साथ ही वन संपदा का संरक्षण और प्रबंधन भी सुचारु रूप से चलता रहे।वन अधिकार कानून और वन संरक्षण अधिनियम एक साथ मिलकर मानव और प्रकृति के बीच संतुलन की व्यवस्था है। ये दोनों मिलकर आदिवासियों के हितों को सुरक्षित रखते हैं और भारत की हरित धरोहर की रक्षा करते हैं।”
“वन विभाग और स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच का संघर्ष” भारत के पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे में एक गहरी जड़ें रखने वाली समस्या है। ब्रिटिश शासनकाल में जब वन कानून बनाए गए, तब से ही वन विभाग को वनों का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण दे दिया गया था। जबकि पारंपरिक रूप से जो आदिवासी और वनवासी समुदाय पीढ़ियों से वनों में रहते आए थे और जंगल से अपनी आजीविका प्राप्त करते थे, उन्हें “अतिक्रमणकारी” या “अवैध निवासी” घोषित कर दिया गया। इस तरह वन विभाग का नियंत्रण बढ़ता गया और स्थानीय समुदायों का अधिकार घटता गया।
यहीं से वन निवासियों और वन विभाग के बीच संघर्ष की नींव पड़ी।आदिवासी समुदाय वनों को जीवन और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। जबकि वन विभाग वनों को राजकीय संपत्ति मानकर प्रशासनिक नियंत्रण के तहत रखता है। इससे अधिकार और नियंत्रण के बीच टकराव होता है। सुप्रीम कोर्ट और नीति आयोग ने कई बार कहा है कि वन संरक्षण के निर्णय स्थानीय ग्राम सभाओं के परामर्श से किए जाए। वन विभाग और आदिवासियों के बीच विश्वास का रिश्ता पुनर्स्थापित करना जरूरी है। वन विभाग और आदिवासी समुदायों का रिश्ता प्रतिस्पर्धा का नहीं,बल्कि सहयोग और साझेदारी का होना चाहिए। वनों का संरक्षण तभी संभव है जब उन्हें बचाने वाले लोग यानि आदिवासी समुदाय को सम्मान और अधिकार के साथ उस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए।
(लेखक राज कुमार सिन्हा बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ से जुड़े हैं।)