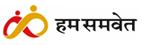तकनीक की गुलाम बनती शिक्षा
ऑनलाइन पाठ्यक्रम को लेकर डींगें हांक रहे हैं लेकिन यह नहीं सोच रहे हैं कि इस प्रक्रिया से कितनी बड़ी संख्या में छात्र बहिष्कृत हो रहे हैं।

‘उपनिषद का राजा अपने राज्य का वर्णन कर रहा है ‘न अविद्वान- मेरे राज्य में विद्वान न हो ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नहीं, सभी विद्वान हैं।’ - विनोबा
हाल ही में अखबारों में शिक्षा को लेकर दो खबरें छपी हैं। पहली खबर केरल है जहां पर ऑनलाइन कक्षा में शामिल ना हो पाने के कारण दलित छात्रा ने अपने घर से कुछ दूरी पर स्वयं को आग के हवाले कर आत्महत्या कर ली। यह समाचार अखबार के आखिरी पन्ने पर एक कॉलम में 3.5 सेंटीमीटर में वर्णित है। इसी अखबार के पहले पन्ने पर दो कॉलम में 9 सेंटीमीटर में छपे समाचार का शीर्षक है ‘कोरोना का असर : सभी आईआईटी ने किया अनुरोध- गरीबों का कोटा भरने के लिए आईआईटी ने मांगा एक वर्ष का समय।’ इसका कारण वे सोशल डिस्टेंस की शर्तें पूरी कर पाने में स्वयं की असमर्थता बता रहे हैं। इसलिए EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोर का कोटा नहीं भरा जा सकता। उनका कहना है कि इसके लिए उनके पास हॉस्टल आदि की व्यवस्था नहीं हैं। देश की 23 आईआईटी में कुल 6700 सीटें बढ़ानी हैं और इनकी भर्ती सत्र 2021 में होना है। रोचक बात यह है कि मानव संसाधन विभाग ने आईआईटी के इस अनुरोध को सामाजिक न्याय मंत्रालय को प्रेषित कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मानव संसाधन विभाग भी आईआईटी की दलीलों से सहमत है। सवाल उठता है कि यह तकनीकी संस्थान एक वर्ष के लिए अपने सामान्य स्थानों में से 6700 स्थान कम करके गरीबों को क्यों नहीं आवंटित कर देते?
उपरोक्त दोनों घटनाएं भारतीय समाज के दलितों और वंचितों के प्रति सोच को उधेड़ कर रख देती हैं। भारत एक ओर मंगल पर मानव रहित विमान उतार चुका है और चांद पर अपने नागरिकों को उतारने की तैयारी के अंतिम दौर में है। वहीं दूसरी ओर लाखों लाख भारतीय हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों को लौट रहे हैं। सैकड़ों इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा बैठे हैं। करीब दो महीने में बाद सरकार को याद आई कि उनके पास रेल और बस की व्यवस्था भी है। इसके बावजूद जो हो रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। खैर, केरल की जिस अबोध छात्रा ने आत्महत्या की, उसकी पृष्ठभूमि में हमारी शिक्षा प्रणाली है जिसमें किसी भी किस्म की सह्रदयता की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकारी आयोगों के आंकड़ें बताते हैं कि भारत की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रही है। कोरोना वायरस के बाद तो स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ी हैं। ऐसे में इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की योजना का जो शगुफा फैलाया गया है, उसमें केरल की बालिका जैसी तमाम छात्र-छात्रों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बली चढ़ती जाएगी।
पुरातन काल में सवर्ण और दलितों के बीच शिक्षा के भेदभाव का एक कारण संस्कृत भाषा भी बनी। उपनिवेशिक काल में श्रेष्ठी वर्ग ने संस्कृत के स्थान पर अंग्रेजी को अपना लिया और आजाद भारत में अपना वर्चस्व बनाए रखा। तमाम प्रयासों के बाद अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया और शिक्षा का अधिकार कानून बना। इस आधे अधूरे मन से बने चौथाई कानून ने थोड़ी बहुत उम्मीद जताई थी कि शायद बच्चों की शिक्षा के मामले में न्यायपूर्ण व्यवस्था हो पाएगी। देश के वंचित परिवारों के बच्चे पहले भाषा और आर्थिक अभाव की वजह से बेहतर शिक्षा (यह भी एक भुलावा ही है) से वंचित थे, उनकी बदहाली में अब एक नई चीज़ जुड़ गई है वह है तकनीक। विद्यालयों को बैठे-ठाले का काम मिल गया। एक तरफ सभी चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्री कह रहे हैं कि बच्चों का लगातार मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठना घातक है। वहीं दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारें पढ़ाई की इस तकनीक के माध्यम को पूरी तरह से अपनाने पर हाथ धोकर पीछे पड़ी हैं। यह कैसा विरोधाभास है?
गौर कीजिए कि भारत के कितने परिवारों को स्मार्टफोन,लैपटॉप और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं? अगर एक गरीब परिवार में दो या अधिक बच्चे विद्यालयीन शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षण का समय एक ही है तो उन्हें कितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की व्यवस्था करना होगी? इसके लिए वे धन कहां से लाएंगे? जिनके माता-पिता दोनों काम पर (यह स्थिति मध्यम वर्ग के साथ भी संभव है) जाते हों उनके बच्चे कैसे इस परिस्थिति में शिक्षा ले पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे नीति निर्माता और विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के कर्ताधर्ता चुप्पी साधे बैठे हैं। इस मामले में सड़ांध सिर्फ विद्यालयीन शिक्षा में नहीं, बल्कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिन्हें हम उच्च शिक्षा का आदर्श (IIT) आदि मान रहे हैं, वहां पर भी फैली हुई है। सीबीएसई और प्रदेश के शिक्षा बोर्ड ऑनलाइन पाठ्यक्रम को लेकर डींगें हांक रहे हैं लेकिन वह यह नहीं सोच रहे कि इस प्रक्रिया से कितनी बड़ी संख्या में छात्र बहिष्कृत हो रहे हैं और कितने मासूम बच्चों की आंखें और शारीरिक तथा मानसिक अवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्या वे यह सोच पा रहे हैं कि भारतीय परिवारों में महिलाओं की स्थिति क्या है? वह घरों में सबसे पहले उठतीं हैं और बाद में सोती हैं, उठने और सोने के बीच का औसतन फासला 14 से 16 घंटे का होता है, और इस अवधि में उन्हें चैन से बैठना तक नसीब नहीं होता, ऐसे में बच्चों के लिए समय कैसे निकाल पाएंगी?
जिन घरों में 100 वर्ग फीट में खाना बनता है, पांच लोगों का परिवार सोता है, क्या वहां यह सब संभव है? परंतु हमारी पूरी व्यवस्था और इसके हामी, मनुष्य को मनुष्य ही नहीं समझ रहे हैं।
प्रसिद्ध शिक्षाविद कृष्ण कुमार लिखते हैं ‘उपनिवेशवाद का प्रधान लक्ष्य था आर्थिक शोषण और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक रूप से भारतीय समाज को कुचलना जरूरी था। शिक्षा की प्रधान भूमिका इस संदर्भ में थी और वह आज तक निभा रही है। भारतीय समाज की दासता के औजार के रूप में शिक्षा का इस्तेमाल करने के लिए उपनिवेशवादी शास्त्र ने स्कूली अध्ययन की स्वायतता छीन ली है।’ वे विस्तार से बताते हैं कि उपनिवेश से पहले भारत के ग्रामीण समाज में शिक्षा का जाल (नेटवर्क) फैला हुआ था। शिक्षक तब भी बच्चों को दबाते थे, लेकिन अध्यापक एक स्वतंत्र व्यक्ति होता था, बच्चों को लेकर वह खुद फैसले लेता था, उस पर नौकरशाही का दबाव नहीं था। अध्यापक एक बौद्धिक व्यक्ति था और आज की स्थिति हमारे सामने है, सिवाय अच्छे पैकेज के शिक्षा का कोई अन्य प्रयोजन जैसे रह ही नहीं गया है। गौरतलब है कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा पूरी तरह से नौकरशाही के अधीन आ गई और आजादी के बाद सात दशकों में स्थितियां और भी बदतर हो गईं। अध्यापक कमोबेश बिना पढ़े लिखे (शिक्षण संस्थाओं के) संचालकों के अधीन हो गए। इसी से जुड़ा सवाल परीक्षा पाठ्यक्रम का भी है, जैसा अंग्रेज चाहते थे कि विद्यार्थी उतना ही पढ़े, जितने में वह साक्षर हो सके और गुलामी बनाए रखने में सहयोग कर सके। ठीक वैसा अभी हो रहा है, सारा तंत्र व श्रेष्ठ वर्ग चाहता है कि शिक्षा में स्वतंत्र विचारों के उपजने की जाने की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म किया जाए। कृष्ण कुमार समझाते हैं कि गांधी की प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा योजना के चलते एक नई हवा देश में बही। यह हवा पाठ्य पुस्तकों के धंधे के लिए बड़ी कष्टप्रद थी। जिन तमाम सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों ने बुनियादी शिक्षा की जड़ें खोदीं, उनमें पाठ्यपुस्तक व्यवसाय के मालिक शामिल थे। अत: बुनियादी शिक्षा पराजित हुई। अपने हाथ से काम करने और अपनी आंख से देखने की क्रांतिकारी शिक्षा दफना दी गई और पाठ्य पुस्तकों की फिर बन आई। इतिहास पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि बीच के कुछ दशकों तक पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन पर राज्य का प्रभुत्व रहा, परंतु अब निजी प्रकाशक पुनः हावी हो गए हैं, और हम देख रहे हैं कि बच्चे बस्ता नहीं ट्रॉली वाली सूटकेस में किताब-कॉपी ले जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत ने पिछले करीब तीन शताब्दियों से मनन-चिंतन की प्रक्रिया (अपवाद को छोड़ कर) पर रोक लगा दी है। हमें विचार करना होगा कि जिस शिक्षा की वजह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और कथित श्रेष्ठ संस्थान गरीब वर्ग को एक साल के लिए (बाद में अवधि बढ़ाई भी जा सकती है) प्रवेश नहीं देना चाहते उसमें आगामी एक वर्ष के लिए ‘तालाबंदी’ कर दी जाए। यह निश्चित है कि इससे देश को रत्तीभर भी नुकसान नहीं होगा। शिक्षा पर नए सिरे से विचार हो यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अंत में एक बार पुन: विनोबा। विनोबा कहते हैं कि ‘दिन में एक घंटा, सप्ताह में एक दिन और एक साल में एक महीना अध्ययन, चिंतन, मनन, ध्यान के लिए निकालें।’ हम जो प्रक्रिया शताब्दियों से टालते आ रहे हैं, एक साल उसके लिए कम हैं, पर शुरुआत तो की ही जानी चाहिए।