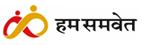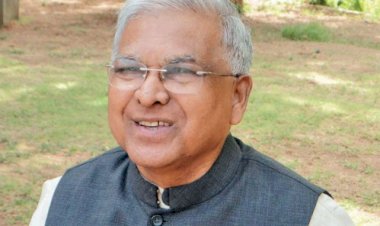कब्र में सिर्फ आदमी ही दफ्न नहीं होता
लोकमान्य तिलक ने एक उदाहरण दिया था कि, ‘‘बंबई से जहाज निकला तो किसी बंदरगाह में ही जाएगा, लेकिन अपने सामने ध्रुवतारा रखकर जाएगा। कहीं निशानी होनी चाहिए, वह है ध्रुवतारा। वह न रहा तो हम भटक जाएंगे।" तो संविधान ही वह ध्रुवतारा है, सबके लिए। न्यायालय, आरोपी, अपराधी, पीड़ित, समाज सभी के लिए।

‘‘ऐसा क्यों है कि लगभग सभी अपराध इतने फूहड़पन से छिपाए जाते हैं और इतनी आसानी से उनका पता चल जाता है और ऐसा क्यों हैं कि लगभग सभी अपराधी अपने पीछे इतने खुले सुराग छोड़ जाते हैं।‘‘
अपराध और दंड (सन् 1866)
फ्योदोर दोस्तो व्यस्की
अतीक-अशरफ अहमद की पुलिस अभिरक्षा (कस्टडी) में तीन युवाओं ने हत्या कर दी। वे तीनों आरोपी निम्न आय वर्ग के थे। उनके पास लाखों रूपये कीमत की पिस्तौल कहां से आई? क्या उनके पीछे राजनीतिज्ञों या बिल्डरों का प्रश्रय था? अतीक अहमद पिछले चार दशकों से अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह था। वह सांसद रहा। वह विधायक रहा। उसके परिवार के कई अन्य सदस्यों का ‘‘एनकाउंटर‘‘ हो चुका है। ऐसा कोई भी अपराध शायद नहीं था, जो उसने न किया हो।
इस सबसे ऊपर यह भी कि जब उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, तब उसने पुलिस वाहन से उतर कर पेशाब भी किया था, जिसे कई भारतीय समाचार चैनलों ने सजीव यानी लाइव दिखाया था। वह अपराधी था, क्या इसलिये उसे ऐसा करते दिखाया जा सकता था? इस अभद्र और अश्लील प्रसारण के लिए एक भी चैनल से सवाल जवाब नहीं हुआ और इस सजीव प्रसारण की अंतिम परिणिति उसकी हत्या के सजीव या लाइव प्रसारण के माध्यम से हुई। जबकि वह कुछ ही दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर कह चुका था कि उसे अंदेशा है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी और ठीक ऐसा ही हुआ। क्या उसे सिर्फ इसलिए जीने का हक नहीं था क्योंकि वह एक अपराधी था? कुछ ही दिन पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी प्रिंस तेवतिया की भी अन्य कैदियों ने हत्या कर दी थी।
यह भी पढ़ें: सुसाइड जैसे गंभीर विषयों का मजाक उड़ाना सही नहीं, PM मोदी के चुटकुले पर राहुल-प्रियंका ने जताई नाराजगी
वस्तुतः अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके द्वारा किए गए अपराधों और राजनीतिक गतिविधियों को ही केन्द्र में रखने की वजह से वह मूल प्रश्न कहीं गुम हो गया कि, ‘‘यदि व्यक्ति पुलिस या न्यायालयीन कस्टडी में भी सुरक्षित नहीं है तो अन्य लोग स्वयं को कैसे सुरक्षित मानें? आरोपी एवं अपराधी दोनों ही वास्तव में न्यायालय के संरक्षण में होते हैं और न्यायालय एक विधायी व प्रशासनिक दंड प्रक्रिया के तहत उसे रिमांड के लिए पुलिस को सौंपता है या अपराध सिद्ध हो जाने पर पुलिस के माध्यम से जेल अधिकारियों को, जहां पर कि वह सजा की अवधि तक निरुद्ध रहता है। यदि कोई अपनी शरण (कस्टडी) में रह रहे व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहा जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो न्यायपालिका से है कि उसकी कस्टडी में (सुरक्षा) कोई आरोपी/ अपराधी बिना मौत की सज़ा पाए मार दिया गया!
इसे कत्ल कर, उसे कत्ल कर
तुझे सात खून मुआफ हैं
तेरी सल्तनत, तेरा दबदबा,
तेरा इक्तिदार है, आजकल।।
क्या सही दस्तूर बन जाएगा? अतीक की हत्या कोई सामान्य घटना नहीं है। यह किसी आतंक का अंत नहीं है, बल्कि एक और वीभत्स आतंक की सुगबुगाहट है। यह लोकतंत्र के और संविधान के अपमान की सुगबुगाहट भर नहीं बल्कि उसके अपमान का जयघोष है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं, ‘‘पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है।‘‘ वहीं गौतम बुद्ध कहते हैं कि ‘‘पहला पत्थर वह मारे जिसने कोई अपराध न किया हो।" वे तमाम लोग जो आज इस हत्या को क्रिया की प्रतिक्रिया कह टाल देना चाहते हैं, भूल जाते हैं कि भारत ने 26 जनवरी 1950 को एक संविधान को स्वीकार ही नहीं, अंगीकार करने का वचन दिया था। जिसकी रक्षा के वचन लेकर संसद और विधानसभाओं में जनप्रतिनिधि अपना दायित्व पूरा करने जाते हैं।
संविधान को पढ़ने से समझ में आता है कि संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के दौरान कानूनों के दुरुपयोग की कितनी गहन विवेचना की है। पूरे संविधान में खासकर मौलिक अधिकारों (भाग-3) में सबसे ज्यादा जोर आरोपी के अधिकारों पर दिया है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण को लेकर विवेचना करता है। इसमें तीन महत्वपूर्ण धाराएं हैं, अनुच्छेद 21 तो साफ व्याख्यायित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद-22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद संभवतः संविधान के सबसे विस्तृत अनुच्छेदों में है।
इसके बाद अनुच्छेद-32 आता है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार Right to Constitutional Ramedies को व्याख्यायित करता है। अनुच्छेद-32 A भी इसी से संबंधित है। तो इस तरह की अभिरक्षा में हुई हत्याएं या एनकाउंटर को किस आधार पर कानूनी या नैतिक स्वीकार्यता प्रदान की जा सकती है? परंतु यह दुखद है कि यह तो कमोवेश समारोहित हो रहा है। प्रशासन द्वारा किया गया प्रत्येक बल प्रयोग शासन-प्रशासन की असफलता ही है।
अतीक अहमद की हत्या और ऐसी तमाम अन्य वारदातों को लेकर न्यायालयों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे प्रोएक्टिव हों। इस तरह के मामलों में सीधी कार्यवाही करें। अंततः उन्होंने ही उसे अभिरक्षा में भेजा है और उन्हें ही उसकी सुरक्षित वापसी/सुपुर्दगी के प्रति वचनबद्ध रहना चाहिए और ऐसा न होने पर स्वमेव ही कार्यवाही की पहल करना चाहिए। अतीक अहमद के मामले में जो न्यायिक आयोग बना उसका गठन राज्य सरकार ने किया। एक विशेष जांच दल उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने गठित किया। दूसरा विशेष जांच दल प्रयागराज के पुलिस आयुक्त ने गठित किया। सवाल किसी की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगाने भर का नहीं है। इस तरह के मामलों की जांच क्या तुरंत केंद्रीय जांच दलों को नहीं हस्तांतरित होना चाहिए था?
यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश की महिलाओं को बेआबरू करने पर उतारू है शिवराज सरकार, कमल नाथ ने महिला आयोग की अध्यक्ष को लिखा पत्र
गौर करिए सर्वोच्च न्यायालय ने हरिचरण एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य (581-2003) के निर्णय (9-3-2011) में कहा था कि ‘‘न्यायालय को इस तथ्य से ध्यान नहीं हटाना चाहिए कि पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु संभवतः सभ्य समाज, जो कि कानून के द्वारा संचालित होता है, में होने वाला संभवतः सबसे निकष्टतम अपराध है और यह एक सामान्य सभ्य समाज के सामने एक बड़ी आशंका खड़ी करता है। अभिरक्षा में दी जाने वाली यातनाएं भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को दिए मूल अधिकारों के तहत प्रदत्त मान्यताओं की अवहेलना करती हैं।
पुलिस को एक सभ्य राष्ट्र में अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए और कई बार ‘‘खाकी‘‘ पहने लोग स्वयं को कानून से ऊंचा मान लेते हैं और कई बार तो वे स्वयं ही कानून बन जाते हैं।‘‘ अतीक अहमद, अशरफ अहमद व तमाम आरोपी जो रिमांड पर हैं या जेलों में बंद हैं, उनके मौलिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते, बल्कि उनके सीधे-सीधे न्यायालय के अंतर्गत हो जाने की वजह से न्यायालयों की जवाबदारी महज सलाहकार भर की या प्रेक्षक (आबजखेर) की नहीं मानी जा सकती। ऐसा भी नहीं है कि न्यायालयों ने इस तरह की वारदातों पर सख्त टिप्पणियां नहीं की। इसके बावजूद उनकी टिप्पणियां असरकारक साबित क्यों नहीं हो पा रहीं हैं? पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता स्व. जसवंत सिंह खारा की पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु पर फैसला (4-11-2011) देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘किसी अभूतपूर्व मामले में से उपजी असाधारण परिस्थितियां मांग करतीं हैं कि उससे निपटने के लिए असाधारण उपचार (उपाय) किये जाएं।
इस हेतु न्यायालय को कानून को अभिनव ढंग से व्याख्यायित करना होगा और ऐसा करते हुए उसका मानस यह होना चाहिए कि एक असाधारण सबूत वाली परिस्थितियां, असाधारण उपायों की दरकार करतीं हैं। (सामान्य अनुवाद) (बी.पी. आचार्य विरुद्ध एस अप्पीरडे)‘‘ तो यह निर्णय स्पष्टतया न्यायालय की सोच के दायरे को न केवल व्यापक बनाने में सहायक है बल्कि न्यायाधीश को नए अभिनव ढंग से सोचने की छूट या अनुमति भी देता है। सवाल फिर घूमकर वहीं आता है, अपराधी व आरोपी की न्यायिक हिरासत में सुरक्षा। अतीक अहमद पर 250 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इनका रहस्य उसी के साथ दफन भी हो गया। यहां पर एक और प्रश्न भी उठता है कि क्या शासन/प्रशासन को अतिरिक्त कठोरता से कार्य करना चाहिए?
हत्या की सुबह ही अतीक अहमद के बेटे को दफनाया गया था। अतीक को कब्रिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी गई और रात 10 बजे उसे अस्पताल ले जाया गया। मुख्य द्वार के बाहर ही उतार कर पैदल ले जाया गया। जबकि वहां एंबुलेंस आदि ठीक पोर्च तक आती हैं। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि आरोपी को लाया जा रहा है। तो फिर मीडिया का झुंड वहां कैसे पहले से मौजूद था? यहीं न्यायालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
हावर्ड झेहट लिखते हैं ‘‘इस पूरी आपराधिक न्याय प्रक्रिया में अपराधी की हैसियत कमोवेश एक तमाशाई जैसी हो जाती है। उसका ध्यान प्राथमिक तौर पर उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर केंद्रित रहता है। वह अनिवार्यतः बहुत सी उलझनों, निर्णयों और स्थितियों से घिरा रहता है। कुल मिलाकर उसके लिए अधिकांश निर्णय दूसरों के द्वारा ही लिये जाते हैं।‘‘ तो जो भी व्यक्ति निर्णय ले रहा है, वही तो उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। इसी दौरान प्रक्रिया में एक आदमी इतना नजदीक आता है कि बंदूक की नोक से उसकी पगड़ी हटाता है और सिर में गोली मार देता है। बाकी के दो लोग भी गोलियां चलाते हैं। उस अपराधी की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी एक भी गोली नहीं चलाते। हत्यारे आत्मसमर्पण कर देते हैं। जिसकी हत्या हुई वह हत्यारा है तो क्या किसी अन्य को उसकी हत्या करने की छूट दी जा सकती है?
कहते हैं, हमारी न्यायिक प्रक्रिया का प्राथमिक लक्ष्य अपराध का निर्धारण करना है और जब यह एक बार तय हो जाता है तो सजा का निर्धारण होता है। पुराने रोमन कानून में न्याय को बजाय निर्णय के, उस प्रक्रिया के द्वारा परिभाषित किया जाता था, जिससे निर्णय पर पहुंचते हैं। यानी प्रक्रिया ही सार या निर्णय पर भारी पड़ती है। यदि सही नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है तो ही न्याय हुआ है। आज की परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। जांच शुरु होते ही राज्य आरोपी के एकदम सामने खड़ा होता है और अक्सर विवेचना की दिशा इसी ओर होती है कि आरोपी को हर हाल में दोषी ठहराया जाए। इस हड़बड़ी में चूक होती है। जांच एकपक्षीय होती है और अंततः अनजाने ही आरोपी कई बार लाभान्वित भी हो जाता है।
मुंशी सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य (फैसला 16-11-2004) के संबंध में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा था, ‘‘पुलिस को लगता है कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तमाम निर्णयों के बावजूद पुलिस के रवैये में कोई अंतर नहीं आ रहा है। पुलिस यंत्रणा या कस्टडी में हुई मृत्यु के मामले में शायद ही कभी कोई सीधा प्रमाण मिलता है। पुलिस वाले आपसी बंधुत्व के चलते गवाह नहीं बनते। पुलिस के मन में कोई डर ही नहीं होता क्योंकि कोई प्रमाण मिल ही नहीं पाता। आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव इससे हिल जाती है।" आपराधिक न्याय प्रक्रिया व प्रणाली की चुनौती है कि उसे आरोपी, अपराधी व पीड़ित तीनों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी होती है। ऐसे में अपराधी/आरोपी एक आसान लक्ष्य होता है।
जनता उसके खिलाफ होती है, उसके प्रति किसी की कोई सहानुभूति नहीं होती और उसके साथ हो रहे अन्याय को ही लोग न्याय मानने लगते हैं। वह एक व्यक्ति से वस्तु में बदल जाता है। एक वस्तु की तरह उसे तोड़ा-मरोड़ या कूड़े के ढेर में फेंका जा सकता है। यह कोई मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बेहद घातक है। तो प्रश्न उठता है कि करा क्या जाए? लोकमान्य तिलक ने एक उदाहरण दिया था कि, ‘‘बंबई से जहाज निकला तो किसी बंदरगाह में ही जाएगा, लेकिन अपने सामने ध्रुवतारा रखकर जाएगा। कहीं निशानी होनी चाहिए, वह है ध्रुवतारा। वह न रहा तो हम भटक जाएंगे।" तो संविधान ही वह ध्रुवतारा है, सबके लिए। न्यायालय, आरोपी, अपराधी, पीड़ित, समाज सभी के लिए।
अतएव न्यायालय हर हालत में उनकी शरण में आए प्रत्येक नागरिक की जवाबदारी अपने ऊपर ले और सीधी कार्यवाही करे। जिसके हाथों गलती हुई है वही उसकी जांच करेगा? तो समाधान तक कैसे पहुंचेगे? वहां तो लीपापोती से ज्यादा कुछ और होगा नहीं। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि आरोपी/अपराधी भी इसी देश का नागरिक है और उसके पास भी संविधान प्रदत्त अधिकार हैं। उसे उससे वंचित करना संविधान और कानून की सीधी अवहेलना ही है। ‘‘चार्टर मैग्नाकार्टा (1215 ई.) का मूल सिद्धांत सिर्फ ‘‘कानून का राज्य" था। राज्य किसी व्यक्ति का नहीं होता। राज्य राजा का नहीं, बल्कि कायदे कानून का होना चाहिए। स्वयं राजा भी परंपरागत कानून से नियमित होता है। वह न मनमाने ढंग से किसी की जायदाद जब्त कर सकता है, न किसी का कत्ल करवा सकता है।" इस चार्टर को जारी हुए एक हजार वर्षों से भी अधिक हो गया।
भारत में आज जो हो रहा है, बुलडोजर या बंदूकों या नए दमनकारी कानूनों के माध्यम से वह हम सब जानते ही है। जबकि भारतीय संविधान में हमारी स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध 32वीं धारा में सीधे सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। ऐसा अधिकार शायद ही किसी दूसरे देश के नागरिकों के पास होगा। इसके बावजूद दमन लगातार बढ़ता जा रहा है। महात्मा गांधी ने समझाया था, ‘‘सच्ची लोकसत्ता या जनता का स्वराज कभी असत्य अथवा हिंसक साधनों से नहीं आ सकता। कारण स्पष्ट और सीधा है, यदि असत्य और हिंसक उपायों का प्रयोग किया जाएगा, तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि सारा विरोध या तो विरोधियों को दबाकर या उनका नाश करके खत्म कर दिया जाएगा।"
आज क्या यह सब वास्तव में घटित नहीं हो रहा है? संविधान और कानून की बात करने वालों को हिकारत से देखा जा रहा है। क्या यही ‘‘न्यू इंडिया‘‘ है? अतीक अहमद दुर्दांत अपराधी होने के बावजूद एक मनुष्य था, भारत का नागरिक था। अतएव शासकों को यह ध्यान में रखना होगा कि वे ‘‘कठोरता‘‘ व निर्दयता और निर्ममता के बीच के अंतर को समझें। लोकतंत्र सिर्फ करुणामय वातावरण में ही पनप सकता है। हिंसा हारे हुए लोगों की अभिव्यक्ति ही है। याद रखिए इन दो हत्यारों की हत्या ने तीन नए हत्यारें पैदा कर दिए हैं। प्रत्येक हत्या के साथ द्विगुणित होते जाएंगे।
अंत में, अभी केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य वाला मुकदमा जिसमें यह स्थापना दी गई थी कि ‘‘संविधान के मूल स्वरुप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।‘‘ के 50 साल हो गये हैं। इस अवसर पर इस पर नई बहस खड़ी हुई है। गौरतलब है, इस फैसले के बाद न्यायमूर्ति ए एन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाने से नाराज तीन न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया था। इस मामले में भारती की पैरवी नानी पालखीवाला ने की थी। कुछ ही दिनों बाद इस मामले को पिछले दरवाजे से पुनर्विचार के लिए लाया गया था। अरविंद पी दातार ने अपने लेख में इसको बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। नई बहस के दौरान हुए इस संवाद पर गौर करें:
न्यायमूर्ति मुर्तजा फजल अली: मान लीजिए केसवानंद भारती निर्णय आपके खिलाफ जाता, तो क्या आपको यहां आने की और पुनर्विचार (रिन्यु) का अधिकार नहीं था। तो आप सरकार द्वारा पुनर्विचार की मांग के खिलाफ क्यों हैं?"
इस पर नानी पालखीवाला के जवाब पर गौर करिए
नानी पालखीवाला:- माय लार्ड, मुझे बिना किसी लागलपेट के यह उत्तर देने दीजिए। यदि केसवानंद भारती निर्णय हमारे खिलाफ जाता, तो आज कोई सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं होता, जिसके सामने मैं पुनर्विचार को आ पाता।" अतएव प्रत्येक भारतीय को यह समझ जाना चाहिए कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन के कितने प्रलयंकारी और आत्मघाती परिणाम सामने आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय भी इसे समझता ही है, तभी तो उसने भी केसवानंद भारती मामले की 50वीं वर्षगांठ को इतना महत्व दिया। अतीक अहमद का उदाहरण सामने रख हमें यह चिंतन करना होगा कि राज्य क्या इस तरह से स्वयं को संचालित कर सकता है और क्या न्यायालय अपनी पट्टी अभी भी नहीं खोलेंगे? वरना अंततः जनता को अपना भविष्य स्वयं ही सुधारना होगा।
कैफ भोपाली ने लिखा भी तो है,
साया है कम खजूर के ऊँचे दरख्त का।
उम्मीद बांधिए न बड़े आदमी के साथ।