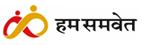फंदे से दूर हुई फांसी
–प्रमोद भार्गव – पंजाब में उग्रवाद का सफाया करने में दो राजनीतिकों का अहम एवं अभिनंदनीय योगदान रहा है। एक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह,जिन्होनें अपने प्राणों की आहुति देकर उग्रवाद को नेस्तनाबूद किया। लेकिन विडंबना देखिए,उनके हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की फांसी अनर्गल तकनीकि कारणों से अटकी हुई है। दूसरे, जुझारू और […]
Publish: Jan 07, 2019, 07:58 PM IST
 फंदे से दूर हुई फांसी
फंदे से दूर हुई फांसी
- strong प्रमोद भार्गव /strong -
p style= text-align: justify strong पं /strong जाब में उग्रवाद का सफाया करने में दो राजनीतिकों का अहम एवं अभिनंदनीय योगदान रहा है। एक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह जिन्होनें अपने प्राणों की आहुति देकर उग्रवाद को नेस्तनाबूद किया। लेकिन विडंबना देखिए उनके हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की फांसी अनर्गल तकनीकि कारणों से अटकी हुई है। दूसरे जुझारू और आतंकवाद के खिलाफ निरंतर आग उगलने वाले युवक कांग्रेस के पूर्व अधयक्ष मनिंदर सिंह बिट्टी हैं जिन्हें कुख्यात खालिस्तान आतंकी देविंदर सिंह पाल भुल्लर ने 1993 में एक बम बिस्पोट करके मारने की कोशिश की थी। इस विस्पोट में 9 लोग मारे गए थे बिट्टा को हमेशा के लिए एक पैर गवांना पड़ा था और 25 अन्य जख्मी हुए थे। इसी भुल्लर को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दीया है। अदालत ने सजा बदलने का आधार राष्टपति द्वारा दया याचिका के निबटारे में लगी 8 साल की लंबी देरी को बनाया है। इस फैसले को तथाकथित मानवधिकारवादी मृत्युदंड के परिप्रेक्ष्य में मानवीय रूख के तमगे से नवाजने का काम कर सकते है? लेकिन एक राष्ट्रघाती और मानवता के हत्यारे की सजा को बहाने ढूढंकर कम करना आखिरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे लोगों की पराजय है। इस फैसले से एक और तो तमाम दुर्दांत आतंकवादियों के बच निकलने का सिलसिला तेज होगा दूसरे आतंकवादियों से संधार्ष कर रहे देशप्रेमी हतोत्साहित होंगे? यहां यह भी सवाल मौजूं है कि आप आखिरकार किस किस्म की राजनीतिक कार्यशैली को श्रेष्ठ और प्रेरणादायी मानेंगे जो प्राणों की परवाह किए बिना आतंकवाद से मुठभेड़ कर रही है उसे या जो आतंकवादियों के समक्ष घुटने टेक रही है उसे ? /p
p style= text-align: justify हत्यारे आतंकवादियों को राजनीतिक सर्मथन मिलना देश की सहिष्णु व शांतिप्रिय अवाम के लिए नितांत दुखद पहलू है। राज्य सरकारें जहां संघीय स्वायत्ता का अनुचित लाभ उठा रही हैं वहीं केंद्र सरकार की ढिलाई और वोट के स्वार्थ ने राष्ट्र्रीय दायित्व बोध को हशिये पर डाल दिया है। अगस्त 1995 में बेअंत सिंह की हत्या हुई थी। हत्यारे बलवंत राजोआना ने खुद अपना जुर्म कबूल लिया था। निचली अदालत में फांसी की सजा मिलने के बाद उसने उपरी अदालत में उपील भी नहीं की थी। बावजूद सिख अस्मिता के प्रभुत्व के चलते माफी की मुहिम को पंजाब में इतना तूल दिया गया कि पूरे पंजाब में एक आतंकी के समर्थन में ताडंव हुआ। सिख और गैर सिखों के बीच सांप्रदायिक वैयमन्स्यता फैलाने की कोशिशें हुईं। यहां तक की पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी राजोआना की फांसी टालने में सरकारी स्तर पर मदद की। यह ऐसा पहला अनूठा मामला था कि फांसी की सजा पाए किसी आतंकी को राजनीतिक समर्थन मिलने की शुरूआत हुई। हालांकि उस वक्त माफी का अभियान चलाने वाली पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बेजा दखल के लिए फटकार लगाते हुए हिदायत दी थी की किसी भी राज्य सरकार का काम अदालत के आदेश पर अमल करना है न कि उसको टालना ? किंतु अदालत की इस नसीहत से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और एक अदने से नौकरशाह जेलर की दलील के चलते राजोआना की फांसी टाल दी गई। जो अभी तक टली हुई है। /p
p style= text-align: justify हालांकि भुल्लर के बच निकलने की राह तो तभी आसान हो गई थी जब शीर्ष न्यायालय ने दया याचिका में देरी के चलते एक के बाद एक फांसी की सजाओं को उम्रकैद में बदलने का सिलसिला शुरू किया था। इस क्रम में अदालत ने चंदन तस्कर वीरप्पन के 15 साथियों की मौत की सजा को आजीवान कारवास में बदला। इसके बाद राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल संथम मुरूगन और पेरारिवलन की फांसी को उम्रकैद में तब्दील किया। इस निर्र्णय के विरूध्द केंद्र सरकार ने फांसी की सजा बहाल रखने के मकसद से समीक्षा याचिका भी दायर की थी लेकिन अदालत ने उसे भी खरिज कर दिया। पुनर्विचार पर अदालत की पुष्टि ने केंद्र का विधायी कार्य देख रहे लोगों की कबलियत पर सवाल खड़े किए हैं। जो सरकार देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को मिली फांसी की सजा पर अमल करने में नाकाम रही वह आम लोगों को न्याय क्या दिला पाएगी ? इस लिहाज से भुल्लर के मामले में अदालत ने जो राहत दी है उसे अनुचित ठहराना मुश्किल है ? लेकिन इन तीन मामलों से इतना जरूर तय है कि राजनीतिक वजहें और राजनेताओं की मंशाएं जो भी रही हों भविष्य में अब मृत्युदंड पर अमल करना आसान नहीं होगा ? विकृत हो रही भारतीय राजनीति की पतनशीलता का यह चरम है। /p
p style= text-align: justify देश के मानवाधिकारवादी इन फैसलों से खुश हो सकते हैं क्योंकि अब इन फैसलों की प्रतिच्छाया में हत्या और बलात्कार जैसे जघन्यतम अपराधों में सजा पाए 90 फीसदी दोषियों के प्रति नरम रूझान का रास्ता खुल गया है। गोया यहां यह सवाल जरूर उठता है कि उन लोगों के मानवाधिकार हितों की कौन परवाह करेगा जिनके परिजन हत्यारों की निर्ममता के शिकार हुए ? कई माताएं विधावा और बच्चे अनाथ हुए ? क्या उनकी कोई ऐसी विलक्षण शारीरिक सरंचना है जिसे मानसिक सतांप नहीं होता ? राजीव गांधी बेअंत सिंह और मनिंदर सिंह बिट्टा पर हुए जानलेवा हमलों के दौरान वे सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे जो अपनेर् कत्तव्य का पालन कर रहे थे। यदि दो दशक से ज्यादा समय तक हत्यारों और उनके परिजनों ने फांसी की सजा पर उहापोह की पीड़ा झेली तो इसी अंतिम निर्णय के असमंजस भरे दौर से वे लोग भी गुजरे हैं जिनके प्रियजनों ने दायित्व बोधा का पालन करते हुए जानलेवा हमले की चपेट में आकर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हत्यारों की सजा कम करने का फैसला क्या बालिदानियों का अवमूल्यन नहीं है ? इस बाबत यदि बिट्टा अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि सजा को कम किया जाना आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे लोगों की पराजय है ? वे राजनीतिक आतंकवाद से परास्त हो गए हैं। तो क्या इस वेदना पर गौर करने की जरूरत नहीं है ? आतंकी हत्यारों के बरक्श किस वेदना को अहम माना जाए यह सवाल भी ऐसी दयाओं के संदर्भ में खड़ा होता है? बहरहाल अदालत की यह दलील भी एक राष्ट्रवादी नागरिक के लिए बैचेन करने वाली है कि दया याचिका के निराकरण में देरी के चलते देशद्रोहियों तक की सजा कम कर दी जाएं ? /p
p style= text-align: justify यह ठीक है कि संविधान में दया याचिकाओं के निपटारे की कोई समय-सीमा निश्चित नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि दया याचिकाएं अनंतकाल तक लटकी रहें ? गौरतलब है कि आठवें दशक तक दया याचिकाओं के निराकरण में इतना समय नहीं लगता था। न्यूनतम दो सप्ताह और अधिकतम एक साल के भीतर फैसला ले लिया जाता था। किंतु नवें दशके के अंत तक आते-आते यह अवधि बढ़कर चार वर्ष हो गई और इक्सवीं सदी में तो इन याचिकाओं को अनिश्चिकाल तक टाला जाने लगा। यही वजहें रहीं कि दया याचिका का निराकरण होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को फैसले का आधार विलंब को बनाना पड़ रहा है ? यहां सवाल यह भी उठता है कि जिन हत्यारों को राहत मिली है वे मानवता के ऐसे दुश्मन रहे हैं जिनकी सजा पर तस्दीक की मोहर शीर्ष न्यायालय भी लगा चुकी है। तब क्या यह विसंगति अदालत की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा नहीं करती ? /p
p style= text-align: justify दया याचिकाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल लेते हैं। ये दोनों पद संवैधनिक हैं। लिहाजा अदालतें इन पर टिप्पणी करने से बचती हैं। यही मर्यादा का तकाजा भी है। लेकिन अब समय आ गया है कि ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिसमें देरी की गुंजाइश ही खत्म हो जाए? यह न तो कोई बड़ा काम है और न ही इसके लिए किसी बजट प्रावधान की जरूरत है ? बावजूद राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा में निर्णय लेने को बाधय करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत तो पड़ेगी ही? इस हेतु संविधान में संशोधान की जरूरत भी पड़ सकती है ? लेकिन इसमें कोई बाधा उत्पन्न होगी ऐसा नहीं लगता ? लिहाजा आम चुनाव के बाद नई सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वह दया याचिका के निर्णय को समय में बांधाने की दृष्टि से अग्रणी भूमिका का निर्वहन करे ? /p