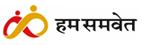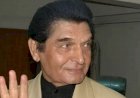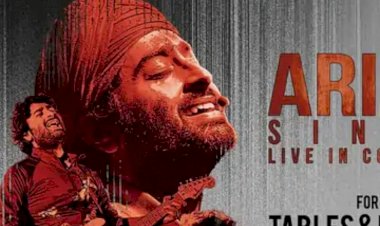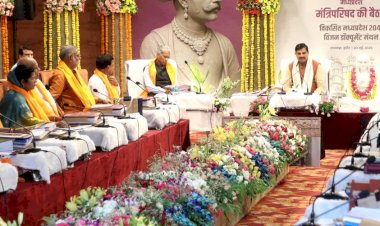मध्य प्रदेश के जंगलों में दंगल
हरित हृदय के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन पारंपरिक से आधुनिक दौर तक विकसित हुआ है। लेकिन अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व विस्तार के नाम पर हजारों आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। वन विभाग व समुदायों के बीच टकराव बढ़ा है। जबकि स्थायी संरक्षण स्थानीय भागीदारी से ही संभव है।

मध्य प्रदेश भारत का “हरित हृदय” कहलाता है क्योंकि यह देश के सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में से एक है। यहां के वनों ने न केवल प्रदेश की पारिस्थितिकी को संतुलित रखा है, बल्कि जनजीवन, जलस्रोतों और वन्यजीवों के संरक्षण में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। वन व्यवस्थापन का विकास यहां कई चरणों में हुआ है, परंपरागत, औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के दौर में।
प्राचीन एवं परंपरागत काल
मध्य प्रदेश के प्राचीन जनजातीय समाज (भील, गोंड, बैगा आदि) का जीवन वन से गहराई से जुड़ा था। इन समुदायों में “साझा वन प्रबंधन” की परंपरा थी, जैसे ग्राम वन, देववन या सरना स्थल। वन का उपयोग आजीविका, औषधि, पशुओं के चारे और धार्मिक उपयोगों तक सीमित था, इसलिए वनों का संतुलन बना रहा। गोंड राजाओं (जैसे गढ़ा-मंडला या गोंडवाना के शासक) के शासन में वनों की सुरक्षा के लिए कुछ स्थानीय नियम भी बने हुए थे।
औपनिवेशिक काल (ब्रिटिश शासन के दौरान)
19वीं सदी में ब्रिटिश शासन ने वनों को राजस्व और संसाधन के रूप में देखना शुरू किया। 1865 का भारतीय वन अधिनियम और बाद में 1878 का अधिनियम लागू हुआ, जिसके अंतर्गत “आरक्षित वन” और “संरक्षित वन” घोषित किए गए। इससे स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकार सीमित हो गए और राज्य का नियंत्रण बढ़ा। ब्रिटिश काल में मध्यप्रदेश (तब का मध्य भारत और छत्तीसगढ़ क्षेत्र) में लकड़ी (विशेषकर सागौन और साल) की कटाई रेलवे स्लीपरों और निर्माण कार्यों के लिए की जाती थी। इस काल में वन विभाग का औपचारिक गठन हुआ और वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ हुआ।
स्वतंत्रता के बाद का काल
1947 के बाद भारत सरकार ने वनों को राष्ट्रीय संपत्ति माना और संरक्षण की दिशा में नीतियाँ अपनाईं।1956 में मध्यप्रदेश के पुनर्गठन के बाद राज्य में वन विभाग की पुनर्संरचना की गई।1952 की राष्ट्रीय वन नीति ने वन क्षेत्र को देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% तक बनाए रखने का लक्ष्य रखा। मध्यप्रदेश के जबलपुर में वन अनुसंधान संस्थान और सागौन उत्पादन के लिए टिंबर कॉरपोरेशन जैसी संस्थाएं बनीं। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, जिसके अंतर्गत कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा आदि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित किए गए। 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम ने वनों की भूमि को गैर-वन उपयोग के लिए स्थानांतरित करने पर नियंत्रण लगाया।
जन भागीदारी और संयुक्त वन प्रबंधन (1990 के बाद)
1990 के दशक में संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में ग्राम समितियों को वन संरक्षण, पुनर्वनीकरण और उत्पादों के साझा उपयोग में भागीदार बनाया गया। बहुत सारी कमीयों के बाबजूद मध्यप्रदेश इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में रहा। वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने आदिवासी और अन्य परंपरागत वनवासियों को उनके पारंपरिक अधिकारों की कानूनी मान्यता दी।
वर्तमान स्थिति और नई पहल
आज राज्य का लगभग 30% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। वन प्रबंधन में जैव विविधता संरक्षण, इको-टूरिज़्म, वन्यजीव प्रबंधन और कार्बन-क्रेडिट जैसी आधुनिक अवधारणाएं जुड़ रही हैं।“हरित मध्यप्रदेश” और “क्लाइमेट एक्शन प्लान” जैसी योजनाएँ राज्य की नई पर्यावरण नीति का हिस्सा हैं।
वन भूमि से स्थानीय आदिवासी समुदायों की बेदखली
अपने राजस्व एवं तथाकथित विकास के नाम पर सरकार ने आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों (जंगल, जमीन एवं पानी) का असीमित दोहन किया है। आजादी के बाद आदिवासियों को भी नयी उम्मीद जगी थी कि अब प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और अपनी मातृभूमि पर इनका अपना अधिकार एवं नियंत्रण मिल जाएगा। लेकिन आजाद भारत ने अपने विकास के लिए पूंजीवादी रास्ता अपना कर देश में विभिन्न विकास परियोजनाओं और अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व के नाम पर दो करोड़ आदिवासियों को बेघर कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश में 11 नये अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। पहले 6 टाईगर रिजर्व था जो अब उसे विस्तार देते हुए 9 कर दिया गया है। कान्हा नेशनल पार्क के विस्तार के नाम पर बालाघाट जिले के जनपद पंचायत बिरसा, बैहर, परसवाड़ा और लांजी क्षेत्र के 55 वन खंडों के लगभग 120 से अधिक गांव जिनका निस्तार जंगल से होता है। इन वन भूमि पर पीढ़ियों से आदिवासी खेती कर रहे हैं और मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, जिसमें 25 से अधिक वन ग्राम है। 55 वनखंडों के वन भूमि का रकबा 36833 हेक्टेयर है। जिसे वन विभाग द्वारा आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।
इसे लेकर विगत 8 अक्टूबर को बालाघाट मुख्यालय पर हजारों महिला एवं पुरूषों ने मोर्चा निकाल कर विरोध किया था।दो दिन तक घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यालय में डटे रहे। मध्यप्रदेश सरकार विभिन्न अभ्यारण्य और टाईगर रिजर्व के नाम पर लगभग 500 गांव को हटाने की योजना बनाई है।जिसका आदिवासी संगठनों ने तीखा विरोध किया है। मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में वन अधिकारियों द्वारा जंगल वासियों के फसलों को नष्ट करने और उनके झोंपड़ी को तोङने, जलाने तथा मारपीट की घटनाएं बङे पैमाने पर हुआ है।
वन विभाग और स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच का संघर्ष” भारत के पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे में एक गहरी जड़ें रखने वाली समस्या है। ब्रिटिश शासनकाल में जब वन कानून बनाए गए, तब से ही वन विभाग को वनों का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण दे दिया गया था। जबकि पारंपरिक रूप से जो आदिवासी और वनवासी समुदाय पीढ़ियों से वनों में रहते आए थे और जंगल से अपनी आजीविका प्राप्त करते थे, उन्हें “अतिक्रमणकारी” या “अवैध निवासी” घोषित कर दिया गया। इस तरह वन विभाग का नियंत्रण बढ़ता गया और स्थानीय समुदायों का अधिकार घटता गया। वन अधिकार कानून 2006 के प्रस्तावना में कहा गया है कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है एवं आदिवासी समाज पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, फिर भी वन भूमि से बेदखल किया है। यह कानून वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों द्वारा पीढ़ियों से सभी प्रकार के वन भूमि का उपभोग करते आ रहे हैं, वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश करता है।
निष्कर्ष
मध्यप्रदेश में वन व्यवस्थापन का ढांचा अब भी मुख्यतः राज्य-केंद्रित है, जबकि वन-आश्रित समुदायों के निस्तार हकों को वास्तविक अर्थों में मान्यता और संरक्षण की आवश्यकता है।
वनों का सतत संरक्षण तभी संभव है जब स्थानीय लोगों को “संरक्षक” नहीं, “सह-स्वामी” के रूप में स्वीकार किया जाए।
(लेखक राज कुमार सिन्हा बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ से जुड़े हुए हैं)