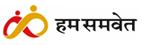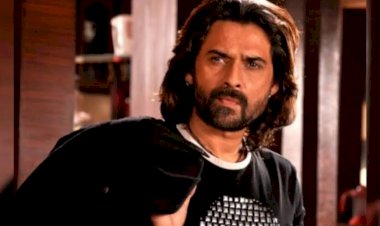छवियों में कैद समाज और नैतिकता की खुली हवा
राजनीति में नैतिकता बहाल करनी है तो अन्याय के विरुद्ध लड़ना होगा, न सिर्फ अपने बराबर वाले से, बल्कि ज्यादा ताकतवर से भी

उत्तर प्रदेश के हाथरस, बलरामपुर और दूसरी जगहों पर स्त्री संबंधी अपराध की जो घटनाएं हुईं उस पर विरोध का स्वर देश के कई हिस्सों से उठते हुए संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। लेकिन विडंबना देखिए कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन उसे एक साजिश की थ्योरी में बांध कर भटकाने में लगी है वहीं अगर पार्टी और गठबंधन के कुछ नेताओं को आपत्तियां हुई हैं तो इसलिए कि इससे पार्टी की छवि खराब होगी और भावी चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्हें किसी कमजोर की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वे करुणा की बजाय राजनीतिक हित से संचालित होते हैं। न ही उनके भीतर से आगे आकर कोई यह कह रहा है कि यह समाज जाति और लैंगिक असमानता में जकड़ा हुआ है। उसे मुक्त किए बिना इन घटनाओं से मुक्ति नहीं है।
दरअसल अच्छी छवि की यह चिंता उस पूंजी की तरह है जिसे पार्टियां चुनावों में खर्च करके भारी लाभ कमाती हैं। इन छवियों का सच्चाई से लेना देना हो यह जरूरी नहीं। न ही इसका किसी सामाजिक आदर्श और नैतिकता से वास्ता होता है। राजनीतिक दल और नेता उन छवियों के बूते ही लोकतंत्र में अपनी शक्ति अर्जित करते हैं। भले ही वे संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन वे जानते हैं कि शपथ लेने के बाद न तो वे संविधान के पन्ने पलटते हैं और न ही जनता उस शपथ पर ध्यान देती है। अगर आजादी के समय कांग्रेस पार्टी से जुड़े और उससे बाहर काम करने वाले नेताओं ने त्यागी, तपस्वी और साहसी होने को एक अच्छी छवि के रूप में प्रस्तुत किया था तो आज एक कठोर और ठोक देने वाले प्रशासक के रूप में अच्छी छवि निर्मित कर दी गई है। भले ही इस कठोरता में संविधान और कानून के राज की ऐसी की तैसी हो जाए और सारे मौलिक अधिकारों को तिलांजलि दे दी जाए। अगर आजादी के समय किसी राजनीतिक दल का आदर्श स्वरूप वह होता था जहां तमाम नेता अपने विचारों को खुले तौर पर रख सकें और सर्वोच्च नेता से मतभेद प्रकट कर सकें। तब अंतररात्मा की आवाज का बड़ा महत्व होता था। लेकिन आज राजनीतिक संगठन वह अच्छा माना जाता है जिसके नेता के सामने किसी अन्य नेता की बोलने की हिम्मत न हो और पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और किसी अन्य की अंतररात्मा से कोई स्वर न उठे।
आज अगर किसी नेता की कार्यशैली पर सवाल उठाया जाता है तो छूटते ही जवाब दिया जाता है कि कुछ भी हो वह ईमानदार तो है। जो ईमानदार नहीं होता उसके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रवादी तो है। और इससे आगे बढ़कर कहा जाता है कि हिंदुओं की रक्षा तो करता है। ऐसे ही राजनीतिक दलों के बारे मे कभी सर्वोदयी नेता दादा धर्माधिकारी ने कहा था कि राजनीतिक दल एक गिरोह हो गए हैं जहां पर न तो खुली बहसें होती हैं और न ही प्रश्न उठाए जाते हैं। लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए संगठित हैं और चुनाव के बाद उसी तरह पद बंटते हैं जैसे लूट और चोरी का माल बंटता है। निश्चित तौर पर यह सब काम धीरे धीरे हुआ इसलिए यह कैसे हुआ इससे ज्यादातर लोग अनजान नहीं हैं। लेकिन यह सब क्यों हुआ इसकी पड़ताल कम ही की गई है। दरअसल स्वाधीनता संग्राम में भारत में जो नैतिकता विकसित हो रही थी उसे सत्ता और धन के लालच ने तेजहीन कर दिया। स्वाधीनता संग्राम और उसके साथ साथ चल रहे समाज सुधार के आंदोलनों के कारण नेताओं के साथ मध्यवर्ग भी जातिविरोध, स्त्री सम्मान और सांप्रदायिक सद्भाव का दिखावा तो करता ही था। लोग उसे एक तरह से पाखंड कहते थे लेकिन इसी पाखंड के झीने परदे के साथ आदर्श जीवित रहता है।
आज ऊपर से नीचे तक वह पाखंड भी समाप्त हो गया है। समाज में जातिगत भेदभाव का विरोध करते हुए जो आंदोलन खड़े हुए उसके नेताओं ने पद प्राप्त करने की शर्त पर सिद्धांत और अंतररात्मा की आवाज को मार दिया। इसी के साथ वे भ्रष्ट हुए और किसी मुद्दे पर बोलने की उनकी नैतिक शक्ति भी समाप्त हो गईं। हालांकि इसके पीछे शासक वर्ग और छवि निर्माण करने वालों की अपनी परिभाषा और प्रयास भी शामिल हैं। यह कोई छोटी घटना नहीं है कि जिस देश का राष्ट्रपति दलित हो वहां एक दलित लड़की से बलात्कार और हत्या को लेकर हुए इतने बड़े विवाद के बाद देश का मुखिया खामोश हो। वह भी तब जब देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया और उसका प्रशासन उस कमजोर व्यक्ति की पीड़ा को खारिज करने और उससे ध्यान बंटाने में अपना सारा संसाधन झोंकने को तैयार हो। कल्पना कीजिए आज अगर बाबा साहेब आंबेडकर या कांशीराम इस देश के राष्ट्रपति होते तो उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर क्या करते। कम से कम मौन तो नहीं रहते।
अगर डॉ राम मनोहर लोहिया लोकसभा में तीन आने बनाम पंद्रह आने की बहस उठा सके या पंडित जवाहर लाल नेहरू के रहन सहन पर प्रतिदिन 25,000 रुपये व्यय का आरोप लगा सके तो उसके पीछे उनकी नैतिक शक्ति थी। उसी के साथ सत्तापक्ष की भी लोकतांत्रिक भावना थी जो हर तरह के आरोपों को सुनते और सहते हुए उसका जवाब देता था न कि राजद्रोह का मुकदमा लगाता था। पंडित नेहरू से हर तरह का टकराव लेने वाले डॉ लोहिया बात कहते थे कि इस समय पंडित जी भारत में हिमालय जैसे कद के नेता हैं। मैं जानता हूं कि उनसे टकराना हिमालय से टकराना है और इससे मेरा सिर फूट सकता है लेकिन मैं टकराऊंगा क्योंकि उसके बिना विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बीमार होने पर आप कहां जाना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास परिवार तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं नेहरू के यहां जाना चाहूंगा जहां मेरी सबसे अच्छी सेवा होगी। डॉ लोहिया ने केरल की सोशलिस्ट पार्टी की पत्तुम थानै पिल्लई की अपनी सरकार को इसलिए गिरवा दिया था कि उसने छात्रों पर लाठी चलवाई थी। उनका कहना था कि लोकतंत्र में अपने लोगों पर लाठी चार्ज का कोई औचित्य नहीं है। यहां यह जानना भी रोचक होगा कि समाजवादियों से मैत्री रखते हुए और आजीवन राजनीतिक विरोध झेलने के बावजूद अपने आखिरी दिनों में पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को भेजकर जयप्रकाश नारायण को यह कह कर बुलवाया था कि आप मेरे उत्तराधिकारी हैं और देश के प्रधानमंत्री का पद संभालिए। यह पंडित जी का बड़प्पन था।
यहां यह जानना रोचक होगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय दक्षिणपंथी विचारों और ब्राह्मण संस्कारों के नेता थे, लेकिन वे जब भी बंबई जाते थे बाबा साहेब आंबेडकर से जरूर मिलते थे। लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जब आंबेडकर ने कहा कि भारत में मेरा कोई सम्मान नहीं है, तो मालवीय जी ने भावुक होकर कहा कि आप ऐसा न कहें इससे हमें बहुत दुख होता है और भारत में आपका सम्मान करने वाले बहुत लोग हैं। मालवीय जी बाबा साहेब से प्रेम करने के साथ उनकी लाइब्रेरी पर निगाह लगाए हुए थे और वे उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ले जाना चाहते थे। लेकिन बाबा साहेब उसके लिए तैयार नहीं हुए।
राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर में ब्राह्मणों का पैर धोया तो उस पर नेहरू जी ने आपत्ति की और डॉ लोहिया ने कड़ा प्रतिवाद किया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरकारी खर्च से कराए जाने का भी विरोध किया था।
इसे कहते हैं राजनीतिक नैतिकता जो हमारे पुरखों ने हमें दी थी और जिसे बहुत तेजी के साथ नष्ट किया जा रहा है। लेकिन इस नैतिकता को नष्ट करने का काम सिर्फ राजनेताओं के बदले चरित्र ने ही नहीं किया है, उसे नष्ट करने का काम हमारे जातिवादी और सांप्रदायिक समाज ने भी किया है। भारतीय समाज को लोकतांत्रिक बनाने और संवैधानिक नैतिकता कायम करने के लिए जिस नवजनवादी क्रांति की जरूरत थी वह हो नहीं पाई और वैश्वीकरण के साथ मूल्यविहीन मध्यवर्ग का उदय हो गया। इस मध्यवर्ग के भीतर न तो जातिविहीन और वर्गविहीन समतामूलक समाज बनाने का सपना है और न ही विभाजन के दौरान पैदा हुई सांप्रदायिकता से लड़ने का जज्बा। उसके दो ही उद्देश्य हैं एक तो किसी तरह से अच्छी नौकरी और पद की प्राप्ति हो और उससे मिलने वाले धन से सुख प्राप्त किया जाए। इस दौरान जो नैतिक शून्यता पैदा हुई उसकी जगह धार्मिक कट्टरता ने भर दी। उस कट्टरता को प्रदान करने का काम धार्मिक संगठनों ने और एक हद तक राजनीतिक संगठनों ने किया। धार्मिक संगठनों ने तमाम रूढ़ियों और प्रथाओं को पुनर्जीवित किया और राजनीतिक संगठनों ने उन्हें सांप्रदायिक जामा पहनाया। जो मध्यवर्ग पढ़ लिखकर इन तमाम जकड़बंदियों से मुक्त हो रहा था उसे अस्मिता और अंधविश्वास की राजनीति में उलझा दिया गया। यही कारण है कि हाथरस में पीड़ित परिवार को धमकाने और उनकी घेराबंदी के साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठी चलवाने वाले कई अधिकारी अनुसूचित जनजाति और जनजाति के हैं। उन्हें न तो आरक्षण के उस उद्देश्य की चिंता है जो उन्हें देकर उस पद तक पहुंचाया गया है और न ही उन्हें सिविल सेवा के दौरान ली गई संविधान की शपथ की चिंता है। लगता है कि वे मौलिक अधिकारों और मानवीय मूल्यों की अवहेलना करने के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। तभी तो देश के कई पूर्व अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में चेताया है।
पंडित जवाहर लाल नेहरू जिस समाज को अपनी लोकतांत्रिक समाजवादी सोच से परिवर्तित कर रहे थे उसे डॉ. भीमराव आंबेडकर और डॉ. लोहिया आक्रामक जातिविरोधी आंदोलनों से बदल रहे थे। आंबेडकर से मिलकर लोहिया अलग पार्टी इसलिए बनाना चाहते थे ताकि इस देश से जातिव्यवस्था का खत्म किया जा सके। उन्हें लगता था कि अगर वे दोनों मिल गए तो यह काम हो सकता है। लोहिया ने जाति के कारणों को ढूंढ कर उन पर प्रहार किया। उसी के साथ वे स्त्री पराधीनता को भी अपना लक्ष्य बनाते थे। इसीलिए उन्हें रामचरित मानस की वे पंक्तियां बहुत प्रिय थीं जिनमें कहा गया है, “कत विधि सृजी नारि जग माहीं, पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं।“ उन्होंने जाति और यौनि के कटघरे तोड़ने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। डॉ. लोहिया को अगर द्रौपदी का चरित्र बहुत प्रिय था तो इसीलिए क्योंकि वे अत्याचारी पुरुष प्रधान समाज से प्रश्न करती हैं।
डॉ. आंबेडकर ने भी ‘जातिभेद का बीजनाश’ और ‘हिंदू स्त्री का उत्थान और पतन’ नाम पुस्तिकाओं में इन्हीं बातों को उठाया है। वे जाति व्यवस्था और स्त्री शोषण के लिए व्यक्तियों की बजाय धर्मग्रंथों को दोष देते हैं और समाज को उस पर सवाल खड़ा करने और उससे मुक्त होने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें मालूम था कि इन धर्मग्रंथों की मान्यता के रहते हुए न तो जाति व्यवस्था का समूल नाश हो सकता है और न ही स्त्रियों को स्वतंत्रता मिल सकती है।
उन्हीं के समांतर लेकिन उनसे थोड़ा अलग डॉ. लोहिया कहते थे कि नैतिकता मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंधों का नियमन करती है। लेकिन जाति ने परिवर्तन का बुनियादी काम बंद कर दिया है। जाति व्यवस्था आध्यात्मिकता की विरोधी बन गई है। ऐसी नैतिकता चाहिए जो आध्यात्मिकता के अनुरूप हो। डॉ. लोहिया कहते थे हम अपने बराबर या ताकतवर से लड़ना भूल गए हैं। भारत में सच्चा लोकतंत्र तभी आएगा जब लोग स्वेच्छा से मरने और अन्याय के विरुद्ध लड़ने को तैयार हों। इसीलिए वे श्रेय और प्रेय के बीच सेतु बनाने की बात करते थे। प्रेय वह चीज है जो थोड़े समय के लिए थोड़े से जीवों को प्रिय लगती है। जिससे वासना प्रफुल्लित होती है। इससे मायाजनित सांसारिक सुख मिलता है। लेकिन श्रेय वह चीज है जो सबका कल्याण करती है। जो सबको प्रिय होती है और सर्वकालिक होती है।
पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने नैतिकता के इन्हीं गुणों का प्रदर्शन किया है। अगर हमें राजनीति में नैतिकता की बहाली करनी है तो छवि की चिंता छोड़कर अन्याय के विरुद्ध लड़ने की तैयारी करने होगी और न सिर्फ अपने बराबर वाले से लड़ना होगा बल्कि इसी नैतिक शक्ति से अपने से ज्यादा ताकतवर से भी लड़ना होगा। आज भारतीय समाज की समस्या यह है कि वह बेईमान और दब्बू होता गया है। उसी के साथ उसे पक्षपाती बनाने का भी अभियान तेजी से चल रहा है। वह अल्पसंख्यकों से लड़ना चाहता है, वह स्त्रियों का दमन करना चाहता है, वह विपक्ष की आवाज दबाना चाहता है और वह अपने भीतर मौलिक परिवर्तन नहीं लाना चाहता है। उसे ऐसा बनाने में बड़ी पूंजी ने योगदान दिया है। कॉरपोरेट हित, जातिवाद और सांप्रदायिकता के इस गठजोड़ ने हमारी राजनीति और समाज को छवि के दायरे में कैद कर दिया है। जिसे कॉरपोरेट मीडिया अपने हितों के अनुरूप बनाता रहता है। वहां समता स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्य गौण हैं। वहां जो जीता वही सिकंदर है। समाज को छवियों की कैद से बाहर निकालकर सत्य और नैतिकता के मुक्त आकाश में अगर ले जाना है तो समाज को ही आगे आना होगा।