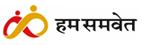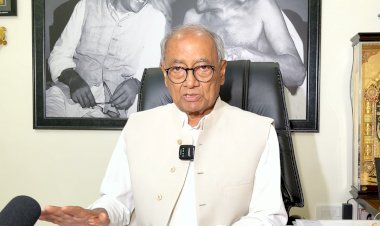व्यवस्था से करुणा की बेदखली
आदेश! उसने नफरत से कहा, जबकि ज़रूरत आदेशों की नहीं कल्पना की है। अल्बेयर कामू के प्लेग नामक उपन्यास से - 1947 ......................... हम हर रोज अपने आसपास लोगों को असमय जाता देख रहे हैं। हम लोग रोज और अधिक अधूरे होते जा रहे हैं। इसके बावजूद कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। अपनी गर्दन झुकाए पंक्ति में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या यह जीवंत समाज की निशानी है ? शासक निश्चिन्त हैं, कि चुनाव तक सब भूल जाएंगे। क्या लाखों लोगों के असमय, अकारण मृत्यु के बाद भी उनका इतना आत्मविश्वास से भरे होना हमें विचलित नहीं कर रहा ? क्या हम अभी भी आजादी से पहले पड़े बंगाल अकाल के समय की प्रजा ही हैं ? हममें कोई परिवर्तन नहीं आया ?

कोरोना महामारी के दूसरे दौर से हम सबको समझ जाना चाहिए कि मानव सभ्यता से करुणा प्रस्थान करती नजर आने लगी है। भारत के संदर्भ में कहें तो पहले दौर में हुई चूक को संदेह का लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि तब यह वायरस हमारे लिए अनजाना था। परंतु सालभर बाद इसके पुनः आक्रमण के दौरान हमारी शासन व्यवस्था का हतप्रभ रह जाना समझा रहा है कि इस देश के राजनीतिज्ञों और प्रशासकों में कल्पनाशक्ति का नितांत अभाव है और वर्तमान परिस्थितियों के लिए यही जिम्मेदार भी है। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में दवाईयों व अन्य संसाधनों की कमी हो सकती है। परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। यहां जो हुआ और जो हो रहा है, वह एक वर्ष पूर्व जो हुआ था उसकी पुनरावृत्ति ही है। पिछली बार यूरोप व अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ने के 2 से 3 माह में भारत में मामलों में वृद्धि हुई थी। इस बार भी वही घटा, परंतु हमारी तैयारी न तब थी न अब है। आग लगने पर कुँआ खोदने जैसा मुहावरे की सार्थकता भारतीय शासन व्यवस्था ने सिद्ध कर दी है।
प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन एक तरह से उस हताशा व आसन्न पराजय को दिखला रहा था, जिसके लक्षण हमें दिखाई दे रहे है। याद रखिए कोई भी महामारी पूरी मनुष्य प्रजाति को नष्ट नहीं करती। उसके एक हिस्से को प्रभावित करती है। एक समय के बाद यह स्वमेव समाप्त भी हो जाती है। ऐसा ही इस बार भी होगा। कोरोना के पिछले दौर में भी यही महसूस हो रहा था। परंतु यह पलटवार भी कतई अनपेक्षित नहीं था। कोरोना का वायरस एक अजेय योद्धा की तरह अपनी तलवार भांजता आगे बढ़ता साफ नजर आ रहा था। वह कोई गुरिल्ला युद्ध नहीं लड़ रहा है। परंतु हमने उसे रोकने की बजाय उसकी तरफ से आँखे बंदकर लीं जैसे कि कबूतर बिल्ली को देखकर करता है और शिकार हो जाता है।
हम कोरोना से आँख फेरकर बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम और केरल की ओर चल दिए। हमारे नेता खासकर सत्ताधारी डॉनक्गिज़ोट काम्पलेक्स से ग्रसित हो गये जिसमें कि तथ्य और कल्पना या गल्प एक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने चुनाव की कमान ऐसे समय पर भी नहीं छोड़ी जबकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। प्रधानमंत्री के बिना क्या कोई नीतिगत निर्णय संभव है? साथ ही जिस व्यक्ति या पद यानी गृहमंत्री पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के क्रियान्वयन का दारोमदार हो, वह राष्ट्रीय राजधानी से बाहर कैसे रह सकता है ?
पर यही हुआ और इसे लेकर उन्हें किसी तरह पछतावा तो दूर संकोच तक नहीं है। साधु होने के लिए साधु दिखना कतई जरुरी नहीं है। जिस तरह से केंद्र व अधिकांश राज्य सरकारों ने कोरोना के इस नए दौर में व्यवहार किया है वह ब्रिटिश काल में पड़े अकाल के दौरान मचे हाहाकार जैसा प्रतीत हो रहा है। यदि सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों में करुणा का अभाव है तो फिर हम व्यावसायिक अस्पतालों, दवाई निर्माताओं, वितरकों, आक्सीजन निर्माताओं, प्रशासनिक तबके से लेकर कोरोना से मृत व्यक्ति की लाश को अपनी गाड़ी से श्मशान या कब्रिस्तान ले जाने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह करुणा व मानवता से लबरेज होगा? चुनावी सभाओं में लाखों का मजमा इकट्ठा करने के बाद किस मुँह से जनता से कहेंगे कि ज्यादा लोग इकट्ठा न हों एवं सार्वजनिक स्थानों पर यथोचित दूरी बनाए रखें। परन्तु पूरी बेदर्दी के साथ यह किया गया।
एक बार महात्मा गांधी के पास एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ आई और बोली, ‘‘बापू यह लड़का बहुत गुड़ खाता है। यह इसके लिए हानिकारक है। यदि आप इसे गुड़ खाने को मना कर देंगे तो यह खाना छोड़ देगा। बापू ने कहा एक सप्ताह बाद आना। एक हफ्ते बाद वह महिला पुनः आश्रम पहुंची। बापू ने उस बच्चे से गुड़ छोड़ने को कह दिया। महिला के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें एक सप्ताह बाद इसलिए बुलाया कि मैं स्वयं गुड़ खाना छोड़ सकूं। यह मुझे भी बहुत प्रिय है।’’ परंतु हमारे शासक दो तरह के जीवन में विश्वास रखते हैं। इसी का परिणाम है कोरोना का दूसरा विस्फोट।
पुलिस घूमने वालों को डंडे मार रही है। कहीं तो दुकान समय पर बंद न करने का आरोप लगाकर पिता-पुत्र दोनों को ही मार डाला। प्रशासन एयरकंडीशन दफ्तरों और कारों में लदा रोज नए आदेश पारित कर रहा है। परंतु कोई मान नहीं रहा। वजह? वजह यह कि जब आदेश देनेवाले पालन नहीं कर रहे तो, बाकी क्यों करें? पिछले दौर में बनी सुविधाओं में से कइयों का इस बार प्रयोग न कर नई सुविधाएं तैयार की जा रहीं हैं क्यों? क्या यह भी बताने की जरुरत है? याद रखिए यदि मस्तिष्क को लगातार एक मिनट तक आक्सीजन न मिले तो कोशिकाएं (सेल) मरने लगती हैं | 3 मिनट के पश्चात कोशिकाओं को स्थायी नुक्सान पहुंचना शुरु हो जाता है। काफी सारी कोशिकाएं इस दौरान मर भी जाती हैं। दस मिनट बाद इतनी कोशिकाएं मर जाती हैं कि जीवन कठिन हो जाता है और लगातार पंद्रह मिनट तक आक्सीजन न मिले तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसके बावजूद आक्सीजन की देशव्यापी किल्लत और तमाम लोगों की आक्सीजन के अभाव में हो रही मृत्यु हमें समझा रही है कि तंत्र की कार्यशैली में करुणा की कोई जगह नहीं बची है।
निजी खासकर कारपोरेट अस्पतालों की मनमानी भी किसी से छुपी नहीं है। विपदा में पड़े व्यक्ति से अतिरिक्त लाभ की आकांशा ही अमानवीयता का चरम है। कामू प्लेग में लिखते हैं, ‘‘भयानक महामारी का असर यह हुआ कि हमारे शहर के लोग इस तरह से आचरण करने को मजबूर हो गए, जैसे उनमें व्यक्तिगत भावनाएं थी ही नहीं।’’ आज पुनः वही दोहराया जा रहा है। यह व्यवस्था व्यक्ति को और अधिक स्वार्थी होने को विवश कर रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति की वजह से ही कोरोना महामारी में हमें यह सबको भोगना पड़ रहा है। पूरे देश में सरकार ने शायद ही किसी बड़े निजी अस्पताल पर कोई कार्यवाही की हो। यदि कोई प्रश्न उठता भी है तो प्रशासनिक जवाब आता है हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। जैसे बिना नामजद शिकायत के कभी कोई कार्यवाही हो ही नहीं सकती।
यहां पर हमें अपनी मीडिया की भूमिका की पड़ताल भी करनी ही होगी। इसका भी बराबरी का दोष है। अखबारों में अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि वे प्रशासनिक अमले से कठिन सवाल पूछ सकें। जिला प्रमुख को आईना दिखा सकें। इस महामारी के तांडव के बीच भी सबकुछ सामान्य बनाने का खेल चल रहा है। कुछ अपवाद जरुर हैं। अतएवं कोरोना के फैलाव की भयावहता का अंदाजा ही नहीं लग पाया। हम हर रोज अपने आसपास लोगों को असमय जाता देख रहे हैं। हम लोग रोज और अधिक अधूरे होते जा रहे हैं। इसके बावजूद कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। अपनी गर्दन झुकाए पंक्ति में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या यह जीवंत समाज की निशानी है ? शासक निश्चिन्त हैं, कि चुनाव तक सब भूल जाएंगे। क्या लाखों लोगों के असमय, अकारण मृत्यु के बाद भी उनका इतना आत्मविश्वास से भरे होना हमें विचलित नहीं कर रहा? क्या हम अभी भी आजादी से पहले पड़े बंगाल अकाल के समय की प्रजा ही हैं? हममें कोई परिवर्तन नहीं आया ?
विनोबा ने इस स्थिति पर तंज करते हुए एक प्रवचन में कहा था, ‘‘एक था गांव। वहां कसाई लोग रहते थे। वे बकरे को ‘‘शेफील्ड’’ की छुरी से काटते थे। फिर स्वराज्य आ गया। तो तय हुआ कि अब ‘‘शेफील्ड’’ की नहीं, अलीगढ़ की छुरी से बकरे काटे जाएंगे। फिर भी बकरे चिल्लाते रहे। कसाई कहने लगा ‘‘मूर्ख अब क्यों चिल्लाता है? अब तो शेफील्ड की नहीं अलीगढ़ की छुरी से काटा जा रहा है।’’ क्या यह सुनकर बकरा खुश होगा ? सारांश, स्वराज्य दिल्ली में आ जानेभर से कुछ नहीं बनता।’’
अब हमें सोचना होगा कि हम बकरा बना रहना चाहते हैं या स्वराज्य को अपने भी यहां लाना चाहते हैं।