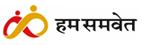हुंकार नहीं यह पीड़ा है
पूंजी की बढ़ती हिस्सेदारी ने नई किस्म की हताशा को जन्म दिया है। भारत सरकार कहती है कि आम जनता को यह जानने का अधिकार ही नहीं है कि राजनीतिक दलों को कौन-कौन चंदा दे रहा है। किसी लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा बेचारगी और क्या हो सकती है?

“भारत में अंग्रेजी शासन ने युवाओं के आत्मसम्मान को आहात किया था और इसी से राष्ट्रीय मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ। स्वाभाविक था कि अंग्रेजी शासन द्वारा स्थापित मूल्यों के विकल्प में वैसे सम्मानजनक मूल्यों की तलाश है, जिनके आधार पर राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सके I” -सच्चिदानंद सिन्हा
राहुल गांधी की नवीनतम पत्रकार वार्ता इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि इसमें वे लगातार भारत सरकार और प्रधानमंत्री की लाचारगी बताते रहे। उनकी बेचारगी अभिव्यक्त करते हुए उनके चेहरे पर न तो हंसी थी न व्यंग बल्कि एक गहन पीड़ा साफ़ झलक रही थी। यह पीड़ा इस सच को अभिव्यक्त कर रही थी कि देश जिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है, वे बेहद डरावनी होती चली जा रही हैं। आज़ादी के बाद पहली बार यह महसूस हुआ कि पूंजी का कुछ ही लोगों के हाथों में एकत्र हो जाना अंततः लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। “अडानी युग” हमें ऐसा सबक सिखा रहा है, जो आज से कुछ वर्ष पूर्व तक अकल्पनीय था। राहुल गांधी की बेचैनी साफ़ नज़र आती है जब वह कहते हैं कि सत्ता बदल जाने के बाद भी अडानी युग आसानी से विदा नहीं होगा। इसके लिए नई योजनाएं बनाना और उसका क्रियान्वयन करवाना कोई आसन कार्य नहीं है। हम एक अंधकूप में उतर चुके हैं, जिसकी गहराई इतनी है कि रोशनी पहुँच पाना बेहद कठिन है।
एप्पल की सूचना कि विपक्षी नेताओं की जासूसी हो रही है, अब उतना नहीं चौंकाती, जितना कुछ बरस पहले चौंकाती थी। राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि राफेल, पेगासस, अडानी कोयला कांड या वर्तमान जासूसी कांड, यदि पिछली सरकारों में घटे होते तो निश्चित तौर पर सरकारों को इस्तीफा देने को बाध्य होना होता। 2-जी स्पेक्ट्रम में कथित भ्रष्टाचार को लेकर यू.पी.ए. की चुनावी हार शायद लोकतंत्र में चमकी आखरी लौ थी। यह विवाद का विषय हो सकता है कि शायद वह एक झूठ था, परन्तु तब तक भारतीय लोकतंत्र में मुद्दे मायने रखते थे I सन् 2019 का आम चुनाव एक मुद्दाविहीन चुनाव था। जिसमें अंततः जनता तो पराजित हुई ही नजर आती है। आज की परिस्थिति बहुत अलग नहीं है, परंतु मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम विधानसभाओं के चुनाव, शायद मुद्दों को पुनर्जन्म दे पाए।
हालांकि मिज़ोरम में प्रधानमंत्री का अपनी सभा रद्द करना, छोटे पैमाने पर ही सही, यह तो सिद्ध कर रहा है कि लगातार अनदेखी अंततः असंतोष को जन्म देती है और करीब 6 माह बीत जाने के बावजूद, मणिपुर में शांति और सदभाव की बहाली संभव नहीं हो पाई है। भारतीय मीडिया इजरायल बनाम हमास को जैसे भारत का आंतरिक मामला मानकर रिपोर्टिंग कर रहा है, यह भी ध्यान बंटाने का एक तरीका ही तो है। तो किया क्या जाए?
प्रसिद्ध गांधीवादी लवणम समझाते हैं, “गांधी के विचारों को हम “सत्य से सत्य की यात्रा” कहते हैं। गांधी किसी दर्शन को लेकर नहीं आए थे, न ही उन्होंने कोई दर्शन दिया। मार्क्स ने समाज निर्माण का दर्शन दिया। गांधी ने कहा कि समाज निर्माण करते हुए दर्शन खुद बनाओ, हम तुम्हें अपने दर्शन में मुक्त करते हैं। गांधीजी को एक समय जो सत्य जैसा लगा आपका अध्ययन किया, आचरण के दौरान दूसरा सत्य पाया तो पुराना सत्य छोड़ दिया। गांधी ने केवल चिंतन से ही सत्य नहीं खोजा बल्कि उस पर प्रयोग भी किए।” राहुल गांधी भी सत्य को ही अपना अभीष्ठ बताते हैं और उसी के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष की बात करते हैं।
गौरतलब है गांधी सन 1915 में भारत लौटे और अब हम सन 2023 में हैं, यानी करीब 108 वर्षों का सफर भारत तय कर चुका है, और उसमें 75 वर्ष आजाद भारत के हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिका, आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक परिस्थितियों में भी आमूलचूल परिवर्तन सामने आए हैं और लगातार सामने आ भी रहे हैं। आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि देश में कोई एक सर्वमान्य नेता हो, जैसा कि तब सबने महात्मा गांधी को माना था। विरोध और असहमति उसमे भी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिन्दू महासभा, उसी की पौध है। परंतु इसके बावजूद उनकी व्यापक स्वीकृति थी। भारत तब लोकतंत्र भी नहीं था, चुनावी राजनीति मूलभूत अनिवार्यता भी नहीं थी।
परंतु आज जिन भिन्न परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, उनके “सर्वमान्य” तो दूर की बात है किसी को “मान्य” मानने का साहस अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ताओं में नहीं बचा है। ऐसे में “सत्य” को आधार बनाकर रणनीति तैयार करने की सोचना भी अपने आप में किसी “चमत्कार” से कम नहीं है। राहुल गांधी इसमें सफल होते हैं या असफल, यह कि प्रश्न औचित्यहीन ही। सवाल पृष्ठभूमि तैयार करने का है। भारत की आजादी का अंग्रेजों से सीधा संघर्ष करीब 190 वर्ष चला था। खैर! गांधी इस परिस्थिति को बहुत पहले ही समझ चुके थे। तभी तो उन्होंने चेताते हुए कहा था कि आजादी के बाद के हमारे संघर्ष और भी कठिन होंगे, क्योंकि तब हमारा संघर्ष अपनी चुनी हुई सरकार के होगा। आज उनका यह कथन एकदम सटीक बैठ रहा है। पेगासस साफ्टवेयर से लेकर एप्पल की चेतावनी, चुनी हुई सरकारों के उद्देश्य से भटक जाने का सजीव चित्रण कर रही है।
राजनीति के नीति विमुख हो जाने और चुनावी राजनीति को राजनीति का पर्याय बन जाने की वैश्विक परिघटना ने सारी मानवीय संवदनाओं को कमोवेश भस्मिभूत कर दिया है। इस परिस्थिति में एकाएक किसी परिवर्तन की आशा करना स्वयं को धोखा देने जैसा होगा। पिछले दिनों पाँचों विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य सरकारों ने अख़बारों में कई कई पृष्ठों के विज्ञापन कई कई सप्ताहों तक दिए, मगर शायद इसमें किसी कोने में कहीं “सांप्रदायिक सौहाद्र” का जिक्र आया हो। जबकि महात्मा गांधी का मानना था कि बिना “सांप्रदायिक सौहाद्र” के भारत का अस्तित्व बच ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश की एक चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ने जरूर धर्म की राजनीति को नकारने की बात की थी। अतः सत्य के मार्ग पर चलने की अनिवार्य शर्तों को तो हमें पूरा करना ही होगा।
राहुल गांधी की इस नई यात्रा, नई पहचान को देखकर जान एलिया की ये पंक्तियां याद आती हैं-
“एक ही तो वह मुहिम थी, जिसे सर करना (पूरा करना) था,
मुझे हासिल न किसी की हुई इम्दाद (सह्दयता) इसमें।”
राजनीतिक दलों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के अपने बहुत अलग से हो गये हैं। पूंजी की बढ़ती हिस्सेदारी ने नई किस्म की हताशा को जन्म दिया है। भारत सरकार कहती है कि आम जनता को यह जानने का अधिकार ही नहीं है कि राजनीतिक दलों को कौन-कौन चंदा दे रहा है। किसी लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा बेचारगी और क्या हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला दे, लेकिन सरकार और सत्तारूढ़ दल को नजरिया हमारे सामने है और पिछले पाँच वर्षों में सत्ताधारी दल को मिला चंदा इस बात का प्रमाण है कि, पूरी व्यवस्था को कैसे सत्ता के अनुकूल किया जा सकता है। चुनाव के नाम पर हासिल किए चंदे से राजनीतिक दल क्या- क्या कर रहे हैं, यह किसी से छुपा भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश राजनीतिज्ञ व बुद्धिजीवी अमूर्त में बात करते हैं। स्पष्ठाता और खुलकर बात करना अब दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता एक ठंडी बयार की तरह सब पर उतरी है। बिया तल्खी के इतनी साफगोई से सब कहना, वास्तव में हिम्मत का काम है।
युवाओं को अगर उनके अंधकारमय भविष्य के बारे में किसी और को बताना पड़े, तो इससे समझ में आता है कि वर्तमान तकनीकि युग ने उनसे राजनीतिक चेतना छीन ली है। असाधारण बेरोजगारी के बीच अगर वे चैन की बंसी बजा रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति सप्ताह में 70 घंटे काम करने की सीख देते हुए भूल जाते हैं कि अधिकतम कार्य घंटे क्यों तय किए गए थे, और यदि एक व्यक्ति अकेला इतना कार्य करेगा तो कितने युवाओं को रोजगार छिन जाएगा या मिलेगा ही नहीं। परंतु युवाओं की प्रतिक्रियाओं का इंतजार बना ही रहता है वे सामान्यतया आती ही नहीं। इस परिस्थिति से आखरी बार जयप्रकाश नारायण टकराए थे, और परिवर्तन सामने आया था।
बदली परिस्थितियों में यदि परिवर्तन की संगठनात्मक ताकत को उभारना है तो आजादी के पहले की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संरचना और कार्य की प्रक्रिया का नए सिरे से अध्ययन और रूपांतरण ज़रूरी है। गांधी के इस सिद्धांत को स्वीकार कारन होगा कि “जो बात व्यक्तियों के लिए सच है, वही राष्ट्रों के लिए भी सच है। कल्पनाशीलता की कोई सीमा नहीं हो सकती। कमजोर आदमी कभी भी क्षमा नहीं करते। क्षमा तो बलवानों का गुण है।” इसी को आधार बनाकर भविष्य की परिकल्पना करनी होगी।
राहुल गांधी की पत्रकारवार्ता से जो बात उभरकर सामने आती है, वह यह है कि सच को बिना किसी मुलम्मे के सीधा सपाट तौर पर ही कहना होगा। प्रश्न उठाने होंगे /उत्तर खोजने की प्रवृत्ति को उभारना होगा। भवानी प्रसाद मिश्र की लंबी कविता की कुछ पंक्तियाँ बहुत कुछ समझा रहीं हैं-
“प्रश्न चारों ओर में आओ, उठो बेचैन मेरे प्रश्न,
चारों ओर से गाओ कि यह क्या हो रहा है?
उठो जैसे कि कोई चाँद उठता है गगन में...............
कविता के अंत में कहते हैं-
“उठो हे उठकर पुकारो जोर से,
क्या हो रहा है
कौन है जो सो रहा है नींद सुख की,
आग जब घर में लगी है
कौन है जो बुझाने बढ़ता नहीं है,
कौन है जो और भड़काना जरूरी समझता है आग को
कौन है जो एक सुविधा समझता है जल रहे इस बाग को”
उस कौन को शायद अब पहचान गए हैं।