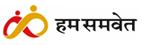खुद को बाजी पर लगाने का दौर
हमें अपने आसपास जो कुछ घट रहा है, उसकी ठीक-ठीक विवेचना और विश्लेषण करना होगा। तब हमारी समझ में आएगा कि पिछले दस वर्षों में सांप्रदायिकता की आड़ लेकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता को बेहद निष्ठुरता के साथ नष्ट करने की कोशिश की गई है। सुखद यह है कि दस वर्षों के पश्चात् “असहमति” ने फिर अपने लिए थोड़ी, जगह बनाई है और जमीन तैयार की है। अब जरुरी है सर्वधर्म समभाव की फसल को पुष्पित करने की।

“मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया है, वह करेगी या मरेगी। अबकी जो लड़ाई छिड़ेगी, वह तो सामूहिक लड़ाई होगी। हमारी योजना में गुप्त कुछ भी नहीं है, हमारी तो खुली लड़ाई है। कांग्रेस को कुचल डालना सरकारी अफसरों के लिए नामुमकिन है। हम एक सल्तनत का मुकाबला करने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई बिल्कुल सीधी लड़ाई होगी। इस बारे में आप किसी भ्रम में न रहें। दिल में कोई उलझन न रखें। लुक-छिपकर कोई काम न करें। जो लुक-छिप कर कोई काम करते हैं, उन्हें पछताना पड़ता है।”
महात्मा गांधी (8-8-1942)
उपरोक्त कथन के करीब 82 वर्ष पश्चात्, भारत पुनः एकबार गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वर्तमान लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था वाले आजाद भारत में एक ऐसी चुनी हुई सरकार से संघर्षरत हैं, जिसके पिछले दो कार्यकाल सल्तनत की याद दिलाते रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस संघर्ष से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सन 2024 के आमचुनाव ने कांग्रेस की भूमिका को काफी हद तक व्याख्यायित तो कर दिया है, लेकिन इस सैद्धांतिक व्याख्या की व्यावहारिक परिणिति कब और कैसे संभव हो पाएगी?
महात्मा गांधी इस परिस्थिति को आजादी के पहले ही भांप चुके थे, तभी तो उन्होंने कहा था कि, आजादी के बाद के हमारे संघर्ष और भी कठिन होंगे क्योंकि तब हमें अपनी चुनी हुई सरकार से संघर्ष करना होगा। इस परिस्थिति को हम आज साक्षात देख रहे हैं। किसान आन्दोलन से लेकर नीट परीक्षा घोटाले तक किए गये सामाजिक व् राजनीतिक आंदोलन अंतत: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पाश्र्व में चले गये हैं। यह एक बेहद गंभीर परिस्थिति है। प्रत्येक राजनीतिक विवाद के हल का माध्यम या मार्ग न्यायालय को बना लेना अंततः हमारी संवैधानिक संसदीय प्रणाली के महत्व को कम कर रहा है।
तकरीबन प्रत्येक विवादास्पद मसले पर सरकार एवं संबंधित या प्रभावित पक्षों के बीच किसी भी तरह का कोई संवाद ही नहीं होता। क्या आजादी के पहले कांग्रेस भारत की आजादी के प्रश्न को लेकर कभी न्यायालय में गई थी? निश्चित ही नहीं! नीट जैसी प्रशासकीय नाकामी का मामला भी सीधे उच्चतम न्यायालय गया। नीट परीक्षा संचालित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन टी ए) के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही ही नहीं हुई। सीबीआई ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यमार्ग अपना कर, सरकार कांग्रेस और प्रतिपक्ष पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने का मौका उपलब्ध करा दिया और चौबीस लाख प्रतिभागी छात्र अवाक रह गये।
यह एक नवीनतम उदाहरण है, इसलिए हमारा ध्यान इस ओर जा रहा है। अन्यथा बांधों एवं विकास योजनाओं की वजह से विस्थापित हुए करोड़ों आदिवासी और ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के दशकों तक चलें आंदोलन अंततः राजनीतिक मसले से न्यायिक मसलों में बदल गये और उनका हल बजाए एक सामाजिक एवं राजनीतिक विमर्श, बहस या बहुपक्षीय वार्ताओं से निकलने के प्रचलित कानून के कानूनी नजरिये से निकाला गया न कि न्याय के दृष्टिकोण से। सारे राजनीतिक दलों को इस विषय पर बेहद तार्किकता और दार्शनिक वैचारिकता के दृष्टिकोण से विचार करना होगा।
अंग्रेज शासक मानते थे कि उन्हें भारत पर कब्ज़ा करने में ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ा। उनके अनुसार, “हमने यह देश कब और कैसे जीत लिया, यह भी हमें पता नहीं चला। (We seemed to have conqured india in a fit of absentmindedness)।”
महात्मा गांधी भी कहते थे, “हिंदुस्तान को अंगेजों ने नहीं लिया; यह हमने उन्हें दिया। हिंदुस्तान में वे स्वयं के बल पर नहीं टिके; हमने उन्हें यहां रख लिया।” उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की सरकारें कांवड़ यात्रा मार्ग पर पट्टिका लगाकर कमोवेश सांप्रदायिक आधार पर यात्रा पथ को “सुशोभित” करना चाह रही थीं। जबकि यह एक पूर्णतः सामाजिक और राजनीतिक मसला है और समाज और राजनीतिक दलों को इसे निपटाना चाहिए था। परंतु राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में राजनीतिक दल कमोवेश वक्तव्य जारी करने और विरोध दर्ज कराने तक सीमित होकर रह गये। कोई भी सीधे टकराव में नहीं आया।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रशासनिक निर्णय पर अस्थायी रोक लगाई लेकिन उत्तरप्रदेश सरकार ने जो नवीनतम शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें कमोवेश अपने पूर्व निर्णय को औचित्यपूर्ण ही निरुपित किया है। वहां अब एक पक्ष देवताओं के चित्र लगाने का आह्वान कर रहा है और दूसरा पक्ष जो उत्तरप्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है संविधान की उद्देशिका को खाने की दुकानों और ठेलों पर लगाने को तत्पर हो रहा है। जबकि यह एक साधारण मसला नहीं बल्कि व्यापक प्रभाव डालने वाला मसला है, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे।
दुष्यन्त कुमार लिखते हैं,
“ये रोशनी है हकीकत में एक छल, लोगों,
कि जैसे जल में झलकता हुआ महल, लोगों।
दररुत हैं तो परिंदे नजर नहीं आते,
जो मुस्तहक हैं वही हक़ से बेदखल लोगों।”
पुनः नीट परीक्षा पर लौटते हैं। अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट – (2015 ) में भी धांधली हुई थी और तब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था यदि किसी एक छात्र को भी गैरकानूनी लाभ मिला है तो वह परीक्षा अमान्य या रद्द मानी जायेगी। दोबारा परीक्षा ली जायेगी। वहीं नौ वर्ष पश्चात् वही न्यायालय कहता है कि प्रस्तुत सामग्री दर्शाती है कि नीट-यूजी परीक्षा का परिणाम पूरी तरह से विकृत नहीं हुआ था। अतएव पुनः परीक्षा नहीं होगी। मात्र एक दशक में न्यायालयीन निर्णय यदि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जायेंगे तो क्या इसे लेकर किसी भी तरह की राजनीतिक पहल नहीं की जाएगी?
क्या नवीनतम निर्णय राहुल गांधी या आखिलेश यादव जैसे राजनीतिज्ञों के राजनीतिक हस्तक्षेप को “गलत” ठहरा रहा है? अतएव नीट परीक्षा या शिक्षा संबंधी गलत नीतियों के विरोध में निरंतरता बनाये रखना एक किस्म की अनिवार्यता ही है। भारत के राजनीतिज्ञों के सामने यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसका तत्काल कोई समाधान निकाला जाना जरुरी है। वस्तुतः न्यायालयीन व्यवस्था और निर्णयों को लेकर किसी तरह का आग्रह या पूर्वाग्रह नहीं है। बल्कि वस्तुतः मूल प्रश्न यही है कि यदि सभी निर्णय अंततः न्यायालयीन प्रक्रिया से ही हल किए जायेंगे तो राजनीतिक विचारों को परिपक्वता कैसे मिल पायेगी?
गौर करिए सन 2005 से 2014 के दस वर्षीय यू पी ए शासन में खाद्यसुरक्षा कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, मनरेगा कानून, सूचना का अधिकार कानून, वन अधिकार कानून, नया भूमि अधिग्रहण कानून जैसे जनहितकारी कानून सामाजिक संगठनों और तत्कालीन राजनीतिक इच्छाशक्ति के माध्यम से पारित और लागू किए गये। क्या अब इन्हें केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही देखा, परखा और इस्तेमाल किया जाएगा?
अतएव आवश्यकता इस बात की है कि उपरोक्त मुद्दों पर राजनीतिक सक्रियता लगातार बनाई रखी जाए क्योंकि महज कानून बन जाने से संतुष्ट होकर बैठ जाना अंततः घातक सिद्ध हो रहा है। यह अनिवार्य है कि सामाजिक विषमताओं को समाज और राजनीति के माध्यम से लगातार हल करने के प्रयास करते रहना चाहिए। आज तमाम राज्यों को मनरेगा के अंतर्गत ठीक तरह से धन आबंटन और वितरण नहीं हो रहा है, तो क्या अब सिर्फ चिट्टी-पत्री और बयानों पर ही बात अटकी रहेगी या विरोध को जमीनी स्तर पर दोबारा जिन्दा किया जाएगा?
अंग्रेजों भारत छोड़ो या करेंगे या मरेंगे जैसे नारे अपने जन्म के आठ दशक बाद भी अर्थहीन नहीं हुए हैं। अंग्रेजों की जगह अगर सांप्रदायिकता लिख दिया जाए तो यह नारा “सांप्रदायिकता भारत छोड़ो” में बदल जाता है। और यह आज की सबसे बड़ी जरुरत भी है। अंग्रेज सिर्फ अंग्रेजों भारत छोड़ो कहने से देश नहीं छोड़ गए थे और न आज सांप्रदायिकता ही ऐसे स्वमेव चली जाने वाली है। अतएव भारत छोड़ो आंदोलन के दूसरे नारे “करेंगे या मरेंगे” को अपनाना होगा और गांधी के उस अमर वाक्य कि प्रत्येक स्वतंत्रता संग्रामी स्वयं अपना सेनापति है, को भी आत्मसात करना होगा।
हमें अपने आसपास जो कुछ घट रहा है, उसकी ठीक-ठीक विवेचना और विश्लेषण करना होगा। तब हमारी समझ में आएगा कि पिछले दस वर्षों में सांप्रदायिकता की आड़ लेकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता को बेहद निष्ठुरता के साथ नष्ट करने की कोशिश की गई है। आजाद भारत में वर्तमान में विद्यमान कई कानून औपनिवेशिक कानूनों से भी ज्यादा दमनकारी सिद्ध हो रहे हैं। सुखद यह है कि दस वर्षों पश्चात् “असहमति” ने फिर अपने लिए थोड़ी, जगह बनाई है और जमीन तैयार की है। अब जरुरी है सर्वधर्म समभाव की फसल को पुष्पित करने की।
महात्मा गांधी ने कौमी एकता या सर्वधर्म समभाव को अपने रचनात्मक कार्यों में पहला स्थान दिया था। वे मानते थे एकता का मतलब सिर्फ राजनीतिक एकता भर नहीं होता। राजनीतिक एकता तो जोर जबरदस्ती से भी लादी जा सकती है। और हम ऐसा होता देख भी रहे हैं। उनका कहना था एकता के सच्चे मानी है वह दिली दोस्ती जो किसी के तोड़े न टूटे। इस हेतु उनकी कांग्रेस जनों से अपेक्षा थी कि वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी वगैरह सभी धर्मों का नुमाइंदा समझें।
अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए वे समझाते हैं, “हिन्दुस्तान के करोड़ों बाशिंदों में से हर एक के साथ वे अपनेपन का, आत्मीयता का अनुभव करें: यानी वे “उनके” सुख दुःख में अपने को उनका साथी समझें। इस तरह की आत्मीयता को सिद्ध करने के लिए हर एक कांग्रेसी को चाहिए कि वह अपने धर्म से भिन्न धर्म का पालन करने वाले लोगों के साथ निजी दोस्ती कायम करें, और अपने धर्म के लिए उनके मन में जैसा प्रेम हो ठीक वैसा ही प्रेम वह दूसरे धर्म से भी करें।”
वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में यह बात सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं सभी राजनीतिक दलों पर एक सी लागू होती है। यह तय है कि कांगेस को इस कार्य की अगुवाई करना होगी। परंतु यह सफ़र एक के पीछे एक जैसी स्थिति में कारगर सिद्ध नहीं होगा। सभी राजनीतिक दलों को एक पंक्ति में खड़े होकर एक साथ- आजादी पूर्व के सांप्रदायिक सौहार्द की वापसी सुनिश्चित करानी होगी। सत्ता राजनीति का सह उत्पाद या बाय प्रोडक्ट है। वस्तुतः सत्ता नहीं राजनीति ही दिशा परिवर्तन का माध्यम बन सकती है और भारत की जनता ने सन 2024 के आम चुनाव में अपनी राजनीतिक समझ की परिपक्वता काफी हद तक सिद्ध कर दी है।
अब राजनीतिक दलों पर यह जिम्मेदारी है कि वे राजनीतिक नैतिकता को पुर्नस्थापित करने कि दिशा में कदम बढ़ाएं।
दुष्यंत कुमार बड़ी उम्मीद जगाते हुए कहते हैं
“इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है,
नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है।
एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों,
इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।”