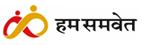अकर्मण्यता चित्त शुद्धि का साधन नहीं
जब मनुष्य की भोग लिप्सा अत्यधिक बढ़ जाती है, जब उसका ईश्वर और धर्म पर विश्वास शिथिल हो जाता है तब वह अकार्य करने लग जाता है

मनुष्य चाहे कितनी ही समृद्धि प्राप्त कर लें, भौतिक सुख साधनों को एकत्र कर लें, बिना मन की निर्मलता के उसे शान्ति नहीं मिल सकती। अध्यात्म शास्त्रों में कहा गया है-
यच्च काम सुखं लोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम्।
तृष्णा क्षयसुखस्यैते, कलां नार्हन्ति षोडशीम्।।
अर्थात् लोक में जो काम सुख है और जो स्वर्गादि लोकों में दिव्य महत्सुख है, इन सबको मिलाकर भी यदि तृष्णा क्षय से होने वाले सुख के साथ तुलना करके देखा जाए तो यह सब उसके सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं ठहरते।
भगवान आद्य शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में कहा है-
तृष्णा क्षय: स्वर्ग पदं किमस्ति?
अर्थात् स्वर्ग पद क्या है?इसका उत्तर है तृष्णा क्षय।
आधुनिक समालोचकों ने हमारे भारतीय शास्त्रों और महापुरूषों के इन विचारों को निराशाजनक बतलाकर इसे देश की लौकिक अवनति का कारण मानकर कामना और तृष्णा की अभिवृद्धि को पुरुषार्थ का मूल कहा है,पर यदि विचार करके देखा जाए तो पता चलता है कि अत्यधिक तृष्णा और लोभ जितना सामान्य मनुष्य को अकर्मण्य बनाते हैं उतने इस प्रकार के दार्शनिक विचार नहीं बनाते। क्यूंकि गीता कार ने यह स्पष्ट बताया है कि अकर्मण्यता चित्त शुद्धि का साधन नहीं है।
उन्होंने कहा कि तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। तू न तो फल-कामना से कर्म करके अपने बंधन का कारण बन, और न ही अकर्मण्य बनकर पाप का भागी ही बन।
दूसरी ओर देखा जाए तो जब मनुष्य की भोग लिप्सा अत्यधिक बढ़ जाती है और उसका ईश्वर और धर्म पर विश्वास शिथिल हो जाता है तो वह अकार्य करने लग जाता है। ईर्ष्या द्वेष से आक्रान्त होकर न्याय, नीति,श्रम और पुरुषार्थ को छोड़कर सुख की ओर दौड़ने लगता है। परिणाम स्वरुप व्यक्ति और समाज का नैतिक पतन हो जाता है। जिससे अनाचार, दुराचार, की वृद्धि होती है। मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थों के पीछे कुछ भी करने में संकोच का अनुभव नहीं करता।
अतः हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारा कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। हमें प्रतिक्षण धर्म पालन करते हुए नैतिक मूल्यों की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए।