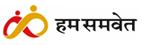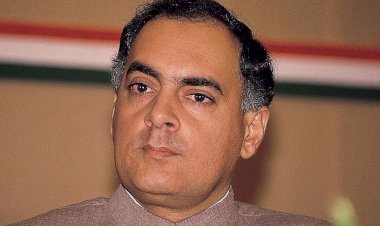आजादी: आफताब का आभास
हमारे दिमाग में यह लगातार भरा गया है कि महात्मा गांधी संसदीय प्रणाली के प्रशंसक नहीं थे। परंतु ऐसा नहीं है। सन् 1931 में उन्होंने कहा था, स्वराज्य से मेरा अभिप्राय है, लोक सम्मति के अनुसार होने वाला भारत वर्ष का शासन। लोक सम्मति का निश्चय देश के बालिग लोगों की बड़ी संख्या के मत द्वारा होगा, फिर वे स्त्रियां हो या पुरुष, इसी देश के हों या इस देश में आकर बस गए हैं। इसके आगे वे एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि, वे लोग ऐसे होना चाहिए, जिन्होंने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की कुछ सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम लिखवा लिया हो। परंतु शारीरिक या मानसिक श्रम तो छोड़ ही दीजिए राजनीति तो बाजुओं के बल और हिंसा में उलझ गई। सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय इसकी गवाही देता है।

आजादी के 75वें वर्ष में भारतीय संसद को सत्तारुढ़ दलों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद व सदन के पीठासीन अधिकारियों ने जिस तरह से संचालित किया है, वह वास्तव में बेहद डरावना है। उम्मीद तो यह थी कि आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश को विशेष अधिवेशन के माध्यम से समारोहित किया जाएगा, परंतु हुआ ठीक इसके उलट। 15 अगस्त के तीन दिन पहले संसद का सत्रावसान कर दिया गया। विपक्ष की एक भी मांग नहीं मानी गई और दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने दर्जनभर विधेयक बिना व्यवस्थित चर्चा के पारित करा लिए गए। क्या आजाद भारत के संविधान द्वारा संसदीय प्रणाली का चुनाव करने के पीछे यही उद्देश्य या भावना थी ?
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रही है। हमें और सारी दुनिया को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसकी संवैधानिक संस्थाएं लगातार कमजोर होती जा रहीं हैं। दुनिया की 20 प्रतिशत आबादी को समेटने वाले देश का लोकतांत्रिक ढांचा यदि कमजोर होता है, जो कि हो भी रहा है, तो यह वैश्विक लोकतंत्र पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा है। दक्षिण एशिया पर थोड़ी नजर दौडाएं चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और एक हद तक बांग्लादेश में लोकतंत्र कमोवेश लुप्त प्राय होता जा रहा है | ऐसे में भारतीय लोकतंत्र का अधिकनायकवाद की ओर अग्रसर होना विध्वंस की पूर्व चेतावनी से भी ज्यादा है।
वर्तमान केंद्र सरकार से तो किसी लोकतांत्रिक पहल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कांग्रेस व अन्य विपक्ष दलों द्वारा शासित राज्यों यथा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, को तो इस 75 वीं वर्षगांठ पर अपनी विधानसभाओं के विशेष सत्र आहूत करने थे और इसमें उन सब विषयों पर चर्चा करते जिन पर चर्चा करवाने से केंद्र सरकार लगातार बच रही है। परंतु ऐसा नहीं हुआ। कारण तो ऐसा न करने वाले ही बता पाएंगे। हमारे दिमाग में यह लगातार भरा गया है कि महात्मा गांधी संसदीय प्रणाली के प्रशंसक नहीं थे। परंतु ऐसा नहीं है। सन् 1931 में उन्होंने कहा था, ‘‘स्वराज्य से मेरा अभिप्राय है, लोक - सम्मति के अनुसार होने वाला भारत वर्ष का शासन। लोक सम्मति का निश्चय देश के बालिग लोगों की बड़ी संख्या के मत द्वारा होगा, फिर वे स्त्रियां हो या पुरुष, इसी देश के हों या इस देश में आकर बस गए हैं।’’ इसके आगे वे एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि, ‘‘वे लोग ऐसे होना चाहिए, जिन्होंने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की कुछ सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम लिखवा लिया हो।’’ परंतु शारीरिक या मानसिक श्रम तो छोड़ ही दीजिए राजनीति तो बाजुओं के बल और हिंसा में उलझ गई। सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय इसकी गवाही देता है।
उपरोक्त कथन के करीब 10 बरस पश्चात् 1939 में गांधी जी कहते हैं, ‘‘फिलहाल मेरे स्वराज्य का अर्थ होगा, भारत की आधुनिक व्याख्या वाली संसदीय व्यवस्था।’’ तो आजादी के बाद संसदीय व्यवस्था तो आ गई लेकिन उसमें आधुनिकता, नवाचार व नये प्रयोगों का लगातार अभाव बढ़ता गया और पिछले कुछ वर्षों से तो इसके कदम पीछे की ओर जा रहे हैं। आसंदी के प्रति बढ़ता असंतोष व रोष इसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शा भी रहा है। वैसे गांधी यह भी मानते थे शुरुआत में हमारी संसद संभवतः बहुत परिपक्व न हो। उनके अनुसार ‘‘जब हमारी संसद हो जाएगी तब हमें महान भूलें करने और उन्हें सुधारने का अधिकार होगा। प्रारंभिक अवस्था में बड़ी-बड़ी भूलें हमसे होंगी। ब्रिटेन की लोकसभा का इतिहास बड़ी-बड़ी भूलों का अवतार है।’’ परंतु विरोधाभास यह है कि ब्रिटिश संसद लगातार स्वयं में सुधार करती रही लेकिन भारतीय संसद की कार्यवाही देखें तो पता चलता है कि हम सदन के भीतर भी संभवतः अब उतने लोकतांत्रिक नहीं हैं, जितने 10 बरस पहले हुआ करते थे।
ब्रिटिश संसद के सुधार और अधिक परिपक्व लोकतांत्रिक संस्थान में बदलने की प्रक्रिया को उनके इस आचरण से समझा जा सकता है। गौर करिए, ब्रिटिश संसद वर्ष में करीब 100 दिन बैठक करती है। इसमें से 20 दिन विपक्षी दलों के हिस्से में आते हैं और वे ही इन दिवसों की कार्यसूची (एजेंडा) तय करते हैं। इसमें से 17 दिन सबसे बड़े विपक्षी दल को और 3 दिन दूसरे सबसे बड़े विपक्षी दल को आबंटित किए जाते हैं। इन सत्रों के दौरान पारित प्रस्ताव सामान्यतया सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते। परंतु इस प्रक्रिया की वजह से विपक्षी दलों को राष्ट्रीय (विधानसभा में राज्य संबंधी) महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखने का मौका मिलता है और सारा राष्ट्र उनके विचारों को जान जाता है। क्या भारत की राजनीतिक जमात इस प्रक्रिया पर गौर करेगी। क्या विपक्षी दल अपने द्वारा शासित राज्यों में इसे प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ कर पाने की इच्छाशक्ति दर्शा पाएंगे। यह कदम भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए प्राणवायु का काम कर सकता है।
मजाज़ लखनवी अपनी नज्म ‘‘पहला जश्ने आजादी’’ के अंत में लिखते हैं,
ये इनकलाब का मुजदा (शुभ संकेत) है इनकलाब नहीं,
ये आफताब (सूरज) का परतौ (आभास) है, आफताब नहीं,
वो जिसकी ताबो - तवानाई (चमकदमक और ऊर्जा) का जवाब नहीं,
अभी वो सई-ए-जुनुरवेज (जुनून भरी कोशिश) कामयाब नहीं,
ये इंतिहा नहीं आगाजे-कोर-मरदां (काम का आरंभ) है।
उनको ये बात कहे 75 बरस होने को आए, लेकिन लगता है जैसे हम वहीं कदमताल कर रहे हैं। ये तय है कि हमने तमाम किस्म कि भौतिक तरक्की की है। हम सेटेलाइट तक बनाने और छोड़ने लगे हैं। परंतु हमें याद रखना होगा कि आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा और शायद एकमात्र मकसद एक लोकतांत्रिक समतामूलक समाज और उसके माध्यम से देश विकसित करना था। आर्थिक तरक्की से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य थे सामाजिक व आर्थिक असामनता को दूर करना और हम 75 बरस बाद भी उसमें सफल नहीं हो पाए हैं | निकट भविष्य में ऐसी सफलता की गुंजाईश भी बहुत कम नजर आ रही है। बढ़ती सांप्रदायिकता और आर्थिक असमानता की खाई का एक गहरी घाटी में बदल जाना हमारी बड़ी असफलताएं हैं। हमारी संसद और विधानसभाएं यदि आजादी के 75वें साल से ही इन विषयों पर ईमानदारी से बहस प्रारंभ करें तो यह बेहद सकारात्मक कदम होगा।
गौरतलब है आजादी के 75वें वर्ष में देश की 80 प्रतिशत जनता आज सरकार द्वारा मुफ्त दिए जा रहे अन्न पर निर्भर है। हमारे पास अन्न का इतना भंडार होना गौरव की बात है लेकिन किसान तो सालभर से सड़कों पर हैं। कोरोना महामारी के दौरान जो कुछ हो रहा है, उसे देख सुन कर मंटो की यह बात याद आ रही है कि, ‘‘एक आदमी का मरना मौत है....। एक लाख आदमियों का मरना तमाशा।’’ हमें तमाशा देखना छोड़ना होगा। हमें आदिवासियों की सांस्कृतिक सोच जैसा दृष्टीकोण अपनाना होगा, जिसमें कि सभी नाचते हैं, भागीदारी करते है, कोई भी दर्शक नहीं होता। वहीँ राजनेताओं की कुर्सी से चिपके रहने की प्रवृति अब हास्यास्पद रूप लेती जा रही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की छोटी सी कविता है,
कभी राम ने सीता छोड़ी। इक धोबी के कहने से।
अबके राम गधा न छोड़ें। लाख दुलत्ती सहने से।।
सबके बावजूद हमें अपनी आजादी पर गर्व है। हार्दिक शुभकामनाएं!
(यह लेखक के स्वतंत्र विचार हैं)