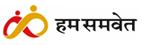जनता को नागरिक बनाने की अनिवार्यता
यदि गांधी को यह विश्वास हो जाता कि चुनाव आयोग ने ईवीएम धांधली की ओर से आँख मूंचकर नतीजे घोषित किए हैं तो यकीन मानिये कि वे जो विधायक चुनकर आए हैं, उनसे भी तुरंत इस्तीफ़ा दिलवा देते या अधिकतम यह “दया” करते कि विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलवा कर उनसे पहले ही सत्र में सामुहिक इस्तीफ़ा दिलवा देते।

“जीवन को नियमित करने के लिये मापदण्ड के होने और न होने में यही अंतर है। आदमी का स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी कि किसी स्तर का अभाव होना।”
धर्मचक्र प्रवर्तन-गौतम बुद्ध
हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय लोकतंत्र के सामने तमाम नए तरह के प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मात्र 0.06 प्रतिशत मत कम मिलने से कांग्रेस को 30 प्रतिशत कम स्थान प्राप्त हुए जबकि पिछले विधानसभा चुनाव की बनिस्बत उसे 11 प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुए हैं। चुनावी जीत-हार या सत्ता पर स्थापित हो जाने भर से क्या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो पाती है?
हरियाणा के चुनाव परिणाम हमारे सामने दो मुख्य प्रश्न उठाते हैं, पहला यह कि कांग्रेस की हार उसकी गलत रणनीति और व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता का परिणाम है या ईवीएम मशीन में कथित कमियों या फेरबदल से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए! परंतु वास्तविकता यह है कि भारत में भाजपा इस वक्त एकमात्र ऐसा दल है, जिसका प्रमुखतम कार्य चुनाव लड़ना और उसे जीतना है।
यह दल चौबीसों घंटे, सातों दिन, बारहों महीने यानी पूरे 365 दिन चुनावी मोड में रहता है और उसके राजनीतिक निहितार्थ कमोवेश वहीं तक सिमट गये हैं। केन्द्र में पिछले दस वर्षों से जिस एकमात्र निरंतरता का आभास मिलता है, वह है “कदमताल।” इस दल के उच्च नेताओं के भाषणों की विषयवस्तु में तो कोई बदलाव नहीं आया है बल्कि भाषा भी कमोवेश वही है।
लगातार दोहराव के चलते भारतीय जनमानस राजनीति को विकल्पहीन मानने की चूक करने को अभिशप्त हो गया है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस सतत चलते प्रोपेगंडे का जवाब क्या चुनाव की घोषणा और आदर्श (?) आचारसंहिता के लागू होने बाद के चंद दिनों में दिया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि मौखिक प्रतिक्रिया मात्र से भी जवाब नहीं दिया जा सकता।
सीधी सी बात यह है कांग्रेस की किसानों में पैठ किसान आंदोलन का समर्थन कर देने या सहानुभूति प्रकट कर देने मात्र से नहीं हो पाएगी। कांग्रेस को कृषि और कृषक की समस्याओं को राजनीतिक व् आर्थिक परिप्रेक्ष्य से समझना और किसानों और देश को समझाना होगा। अगर भारत की 60 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है तो कोई भी राजनीतिक दल उसकी समस्याओं के लिए किसी अन्य समूह के विश्लेषण पर निर्भर नहीं रह सकता।
यदि कांग्रेस या अन्य कोई राजनीतिक दल यह विश्वास कर ले कि ग्रामीण समस्याओं को लेकर गैरदलीय राजनीति को ही अंगीकार करना श्रेयस्कर हैं, तो वह कमोवेश परजीवी होता चला जाएगा। यह तय है कि किसान नेताओं का अपना प्रभाव व प्रभामंडल है और उनके समर्थकों का अपना विराट संसार है, लेकिन जब स्थानीय या राज्य या केन्द्र की सत्ता के लिए चुनाव होगें तो वे अधिकांश किसान एक किसान नेता के हिसाब से चुनावी हस्तक्षेप करेंगे। यही हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उभरकर आया है। यह मान लेना कि आम मानस महज धार्मिक कट्टरवाद को ही वैचारिक तौर पर केन्द्र में रखता है, काफी हद तक “अंधविश्वास” ही है।
कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों को यह अब मान लेना होगा कि चुनावी राजनीति वस्तुतः व्यापक राजनीति का बहुत छोटा सा हिस्सा, सह उत्पाद या बायप्रोडक्ट भर है। वैसे भाजपा की राजनीति वस्तुतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की स्थापना की छोटी सी कड़ी भर है। पिछले करीब 32 वर्षो (6 दिसंबर 1992) से देशभर में जो धर्म को राजनीति के ऊपर बैठाने का प्रयास चल रहा है, उससे पार पाने के लिये महज सत्ता पर नियंत्रण ही काफी साबित नहीं होगा।
अतएव कांग्रेस को आजादी के पहले के अपने स्वरूप व कार्यशैली का नये सिरे से अध्ययन करना होगा और उसकी नई व्याख्या भी करना होगी। वैसे नई व्याख्या उसने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर की भी है। गौरतलब है सन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में एक ओर लोकमान्य तिलक और अन्य कुछ नेता और दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथ के कुछ अन्य नेताओं द्वारा भारतीय संविधान में मुस्लिमों को कुछ विशेषाधिकार देने के बारे में समझौता हुआ था।
उस समय कांग्रेस के संविधान में एक से अधिक राजनीतिक संगठन में शामिल होने की छूट थी। इसलिये जिन्ना जैसे कुछ नेता कांग्रेस तथा लीग दोनों के सदस्य थे और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोग कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों के सदस्य थे। परंतु सन 1916 के सम्मेलन के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मतभेद हुए और सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठन हुआ। आज करीब 100 वर्षों पश्चात् भारत राष्ट्र नई तरह की दुविधा में घिर गया है। यह तय है भारतीय संविधान के कारगर रहते भारत का विघटन असंभव है। लेकिन आंतरिक परिस्थितियां जिसमें बढ़ती सांप्रदायिकता और पुनः सिर उठाता जातिवाद नए तरह के सीधे टकराव को सामने ला रहे हैं।
संत चोखा मेला (सन 1300 से 1400 ईस्वी) महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत और कवि थे। उन्हें दलित महार जाति का पहला महान कवि माना जाता है। उनके अभंगों ने सामाजिक आंदोलनों को नई दिशा दी है। उनके इस अभंग पर गौर करिए, “गन्ना टेढ़ा-मेढ़ा है लेकिन उसका रस नहीं/बाहरी दिखावे पर क्यों जायें?/धनुष मुड़ा है लेकिन उसका तीर नहीं/बाहरी दिखावे पर क्यों जायें? / नदी में घुमाव है लेकिन पानी में नहीं / बाहरी दिखावे पर क्यों जायें? / चोखा (मेला) भद्दा और अनगढ़ हो सकता है / लेकिन उसकी भक्ति नहीं/बाहरी दिखावे पर क्यों जायें?”
ठीक इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिये आवश्यक है कि, वह स्वयं को महज चुनावी राजनीति तक सीमित न रखे। वास्तविकता यही है कि सामाजिक आंदोलन ही अंततः राजनीति की दिशा तय करते हैं। इसीलिये भारतीय संविधान क्रमशः सामाजिक न्याय सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात करता है। सबसे ज्यादा जरुरी है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की लड़ाई अंततः राजनीति में सत्ता का माध्यम बनती है।
आजादी के बाद मा. काशीराम इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। गौरतलब है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण” से संबंधित जो फैसला दिया गया उस पर कांग्रेस आलाकमान की त्वरित व तीखी टिप्पणी ने दल के हाथ आया एक बड़ा मौका गंवा दिया। राजनीतिक दलों से यह उम्मीद की जा रही थी कि वे इसे पहले अपनी केन्द्रीय व राज्य इकाईयों में उठाएंगे और फिर इसे सार्वजनिक रूप से सामजिक न्याय के मुद्दे के रूप में उभारेंगे और इसके बाद प्रस्ताव पारित करेगा परंतु सारा मामला प्रतिक्रियाओं वो भी उच्चतम स्तर लोगों द्वारा शांत कर दिया गया। गौरतलब है कांग्रेस पूर्व में बी टी बैगंन के मामले में देशव्यापी व्यापक बहस के माध्यम से अपना मत सिद्ध करवा भी चुकी है।
कांग्रेस को यदि संघ के विचारों की धार को बोथरा करना है तो महज निंदा या प्रतिक्रिया से बात नहीं बनेगी। विचार को विचार से जूझना पड़ेगा और कांग्रेस के पास ऐसे विचार और प्रतिबद्धता मौजूद हैं, जो कि सांप्रदायिक और इसी तरह के तमाम विघटनकारी परिस्थितियों के अलावा आर्थिक नीतियों पर भी कारगर हैं। बदली परिस्थितियों में राज्य स्तरीय संगठनों का मौन बेहद नुकसानदेह सिद्ध हो रहा है। यदि मध्यप्रदेश का ही उदाहरण लें, तो समझ में आता है कि पिछले 15-17 वर्षों में ऐसा एक भी बड़ा आंदोलन या विरोध नहीं हुआ जो जनमानस की स्मृतियों में बना रहा हो।
हमें यह समझना होगा कि राजनीति अल्पकालीन या पार्टटाइम कार्य नहीं है और बिना विषयों को गहराई से समझे तथा बिना समाधान भी ध्यान में रखे, राजनीतिक संघर्ष कभी भी यथोचित परिणाम नहीं दे पाता है। कांग्रेस के लिए आवश्यक जान पड़ता है कि वह महात्मा गांधी द्वारा किस तरह आंदोलन को खड़ा किया जाता था, उसका गहन अध्ययन करे।
गांधी कहते हैं, “मैं यह सिद्ध कर दिखने की आशा रखता हूँ कि सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों के द्वारा सत्ता प्राप्त करने से नहीं बल्कि सब लोगों द्वारा सत्ता के दुरूपयोग का प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करने से हासिल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, स्वराज्य जनता में इस बात का ज्ञान पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर नियंत्रण और नियमन करने की क्षमता उसमें है।” यही एक शाश्वत प्रक्रिया है, जिससे लोकतंत्र को बचाया व् समृद्ध किया जा सकता है।
जबकि वर्तमान में जो शासन व्यवस्था हमारे ऊपर शासन कर रही है, उसने भारतीय जनमानस के दिमाग में यह स्थापित कर दिया है कि एक कठोर और न्यूनतम लोकतांत्रिक शासन ही हमें यानी नागरिकों को सुरक्षित रख सकता है। लगातार कठोर से कठोरतम कानून बनाये जा रहे हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को श्रीहीन किया जा रहा है और वैसे एक हद तक कर भी दिया है। इस परिस्थिति या व्यापक डर से भारतीय समाज को बाहर निकाल पाना अब दिनोदिन कठिन होता जा रहा है। परंतु इससे आम नागरिकों को बाहर निकाले बगैर परिवर्तन संभव भी नजर नहीं आ रहा है।
भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, “कोई रंगीन तस्वीर नहीं है अनुभव / वह तो कोई / एक जगह है जहाँ / होते हैं हम किसी क्षण / और रंग / पकड़ने लगती है जब / वह जगह / तो जमीन खिसक जाती है / पांवों के नीचे से / वैसे ही जैसे दृश्य सामने के / आखे मींचे से।” यहां गांधी द्वारा कही गई और तमाम बार दोहराई गई बात कि; आजादी के बाद के हमारे संघर्ष और भी कठिन होंगे, क्योंकि तब हमें अपने द्वारा चुनी सरकार से संघर्ष करना होगा। बेहद सामयिक जान पड़ता है। वैसे अब महाभारत जैसी परिस्थिति भी नहीं है और लोकतंत्र का “सपना” हमारे पास है साथ ही साथ सत्य और अहिंसा का ताबीज भी।
परंतु यह ताबीज असाधारण तेज ऊर्जा वाला है, जिसे धारण करना आसान नहीं है। हरियाणा चुनाव परिणामों की ही बात करें और उस संदर्भ में कल्पना करें कि महात्मा गांधी इस परिस्थिति में क्या कदम उठाते तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो सकती हैं।
यदि गांधी को यह विश्वास हो जाता कि चुनाव आयोग ने ईवीएम धांधली की ओर से आँख मूंचकर नतीजे घोषित किए हैं तो यकीन मानिये कि वे जो विधायक चुनकर आए हैं, उनसे भी तुरंत इस्तीफ़ा दिलवा देते या अधिकतम यह “दया” करते कि विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलवा कर उनसे पहले ही सत्र में सामुहिक इस्तीफ़ा दिलवा देते।
वे समझते थे कि कोई संस्था एक स्थान पर ईमानदार और दूसरे स्थान पर बेईमान एक साथ नहीं हो सकती। साथ ही एक गैरजिम्मेदार संस्था के अभिमत को पूरी तरह से नकार दिया जाना चाहिए जिससे कि उसमे ग्लानिभाव पैदा हो सके। आज यह कथन शायद अतिशयोक्ति सा प्रतीत हो रहा है। परंतु अंतिम समाधान ऐसे ही किसी निर्णय के आस-पास ही टिका है।
बहरहाल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के चुनाव सन्निकट हैं। कांग्रेस और समर्थक दलों के सामने चुनौतियां लगातार गहरी होती जा रहीं हैं। वहीं, बिना कटुता और व्यक्तिगत आलोचना पर ज्यादा केन्द्रित हुए, आवश्यक है कि अपनी बात कही जाए।
इसी के समानांतर जनता को नागरिक बनाने की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाना जरुरी है। लोकसभा चुनावों में विपक्ष की वापसी, जम्मू कश्मीर में इंडिया समूह की सरकार बनना और हरियाणा में मतों में 11 प्रतिशत की वृद्धि बता रही है कि राह तो ठीक पकड़ी है बस थोड़ी और स्पष्टता जरुरी है।
राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा है।
जा के ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से।
फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से।।